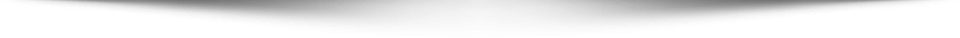लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार’- यह लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया – लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं। लोकनियोजन, लोकनीति, लोकस्वामित्व, लोकअभिव्यक्ति और लोक उम्मीदवारी – ये लोकतंत्र के प्रमुख प्रभावी पांच लक्षण है। लोक के साथ तंत्र का सतत् संवाद, सहमति, सहयोग, सहभाग, सहकार और सदाचार लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालन के छह सूत्र हैं। यदि लोकतंत्र के उक्त तीन जोड़, चार स्तंभ, पांच लक्ष्ण और छह सूत्र सक्रिय व सुविचारित रूप से मौजूद हों, तो समझना चाहिए कि व्यवस्था सुचारु और लोकतांत्रिक है। यदि ऐसा न हो तो लोक घाोषणापत्र, लोक निगरानी और लोक-अंकेक्षण, लोक को नियंत्रित करने के तीन औजार हो सकते हैं और लोकउम्मीदवारी तंत्र में लोक के कब्जे का एक सर्वोदयी विचार।
सोचिए!
क्या हमारी पंचायत और ग्रामसभा के बीच, निगम और मोहल्ला समितियों के बीच सतत् और बराबर का संवाद है?
क्या हमारे जनप्रतिनिधियों ने जनता से अलग एक ऐसा रुआब नहीं बना लिया है, मानो वे किसी और लोक के प्राणी हों?
क्या गांव से लेकर राष्ट्र तक किसी भी स्तर तक नीति, विधान, योजना व कार्यक्रम व्यापक सहमति से बनाये व चलाये जाते हैं?
क्या हम और हमारी सरकारें दोनों एक-दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़ा रहने को लालायित रहते हैं?
क्या हमारा सरकार के निर्णयों-कार्यक्रमों में बराबर का सहभाग और सहकार रहता है?
क्या प्राकृतिक संसाधनों पर लोक का स्वामित्व है?
क्या लोक सही मायने में योजनाओं के क्रियान्वयन व संसाधनों के प्रबंधन व निगरानी में अपनी भूमिका निभा रहा है?
क्या तंत्र के संचालन के लिए लोक सर्वश्रेष्ठ व लोकहितैषी लोगों को चुनकर भेज रहा है?
हकीकत यह है कि हम भारत को भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहकर गौरवान्वित हो लें, लेकिन वस्तुस्थिति गौरवान्वित होने की नहीं है। तंत्र में लोक को आगे लाने के अतुलनीय नेतृत्व के कारण जिस जे पी को हमने कभी लोकनायक की पदवी से नवाजा था, आज उन्हीं के नाम पर रौशन जे पी पार्क (निकट आई टी ओ, दिल्ली) में लगी मूर्तिमान लोकनायक की छड़ी कहीं खो गई है। मंहगाई की मार बताकर गांधी के चरखे के तार तोड़ दिए गये हैं। जो टोपी कभी गांधी ने पहनी ही नहीं, उस गांधी टोपी को पहनकर आज लोग गांधीवादी होने का दावा ठोक रहे हैं। विनोबा के भूदान के भाव को भू-माफिया ने उलट दिया है। लोहिया, अंबेडकर और विवेकानंद का चेहरा पूजने वालों ने उनके विचार को अपनाना बंद कर दिया है। नस्ली घृणा ने राष्ट्रवाद का नारा देने वालों को ही असल राष्ट्रीय भावना से दूर कर दिया है। नेताजी, भगतसिंह, बिस्मिल, आजाद, अजीजन और झांसी ने अपने तो क्या, पड़ोसी के घर में भी पैदा होना बंद कर दिया है।
लोक के पास प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार नहीं है। पैसा कुछ हाथों में सिमटकर रह गया है। एक ओर अमीर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर गरीब। एक ओर जीडीपी की उड़ान पर हमने अपनी पीठ ठोंकी, दूसरी ओर दुनिया के देशों ने दासता व गरीबी का सूचकांक दिखाकर हमारी हेकड़ी निकाल दी है। एक ओर अंतर्जातीय व अंतर्धर्म विवाह बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर वर्ग और वर्ग के बीच में विभेद बढ़ता जा रहा है।
एक ओर लोक प्रतिनिधियों को नकारा व स्वार्थी कहने से हम चूक नहीं रहे, दूसरी ओर तंत्र के संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ व लोकहितैषी उम्मीदवार चुनने की बजाय जाति, धर्म, धन, लालच, दबाव व क्षेत्रवाद आदि के अनैतिक आधार पर उम्मीदवार चुन रहे हैं।
उत्तर पूर्व में कभी जातीय अस्मिता, तो कभी परंपरा के नाम पर समाज में फांस डालने और हिंसा को आगे बढ़ाने का काम सुनियोजित तरीके से जारी है। नक्सलवाद की नकेल देश की नाक में है ही। जम्मू और कश्मीर के बीच बढ़ते विभेद को कम करने की बजाय हम बढ़ाते जा रहे हैं। देश ऐसे कई विरोधाभासी विभेदों में फंस गया है। पार्टियों व सरकारों की नीतियां भी ऐसे ही विरोधाभासी व अनैतिक आधारों पर गुनी व बुनी जा रही हैं।
सही मायने में देश में दो राष्ट्रीय दल हैं। कायदे से दोनों को पूरी तरह सशक्त व लोकतांत्रिक होना चाहिए। दुर्भाग्य से दोनों ही राष्ट्र के न होकर संप्रदाय के हो जाने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। लोकप्रतिनिधि पेश करने वाली पार्टियां ही नहीं, शासन भी अनैतिक आड़ में वोट व लोकसमुदाय दोनों के शिकार का माध्यम बन रहे हैं।
दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितना हम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, विविधता में एकता का गौरवगान गाने वाले भारत राष्ट्र का यह विरोधाभासी हश्र उतना ही अधिक गहराता रहा है। 21वीं सदी में महाशक्ति बनने के सपने, सूचना तंत्र के क्षेत्र में अधिकतम तीव्र प्रसार वाला देश होने के तमगे और पश्चिमीकरण की खुली सोच के पूरब में प्रवेश का आरोप लगने के बावजूद यह सब कैसे और क्यों है?
इस प्रश्न का उत्तर तलाशना जरूरी है।
जवाब कुछ भी हो, लेकिन यह सब इसलिए तो कतई नहीं है कि लोकनीति की जगह राजनीति ने ले ली है। क्योंकि यह बदलाव कारण नहीं, परिणाम है। फिर भी सत्य यही है कि लोकप्रतिनिधि स्वयं को राजा समझने लगे हैं। लोकप्रतिनिधि सभायें सत्तासीनों की सभा में तब्दील हो गई हैं। लोक की आवाज लोकसभा तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो गई है। लोक तंत्र को नहीं, तंत्र लोक को संचालित कर रहा है। लोक भी लोकतंत्र निर्माण में व्यापक सहभागिता के दायित्व निर्वाह की पूर्ति के लिए अभी तक पूरी तरह तैयार दिखाई नहीं देता। आधे लोग वोट नहीं देते, शेष आधे पांच साल के लिए सो जाते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के अपरिपक्व होने के लक्षण हैं।
लोकतांत्रिक पिरामिड को इसके आधार पर वापस लाने को बेताब ताकतें चार मार्ग सुझा रही हैं। एक वर्ग जोर-शोर से प्रचारित कर रहा है कि पार्टी बदलने से सब कुछ बदल जायेगा। दूसरा मानता है कि पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा। राजनीति में अच्छे लोगों को आगे आने व लाने की जरूरत है। अच्छे लोगों के आने से व्यवस्था खुद-ब-खुद सुधर जायेगी। तीसरा वर्ग अंकुश लगाकर तंत्र को नियंत्रित करने से सुधार की संभावना का भरोसा जताता है। चौथा वर्ग मानता है कि व्यवस्था में बदलाव अवश्यसंभावी है। व्यवस्थामूलक खामियों को सुधारकर ही बीमारी का इलाज किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं।
इतिहास गवाह है कि पार्टी बदलने से बेहतरी के परिणाम तात्कालिक होते हैं। इससे दूरगामी व स्थाई निदान की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। इस बीच लोकतंत्र के चारों खंभों को अनुशासित करने की उठी आवाजों के कारण ‘पेड न्यूज’ पर संसदीय समिति की रिपोर्ट, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान, दागियों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जजों की नियुक्ति संबंधी जैसे संसदीय कदम उठे ही हैं। किंतु क्या यह सच नहीं है कि सूचना के अधिकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुद दलों ने मिलकर अंकुश नहीं लगा दिया है? क्या दागियों के मामले में ‘स्पष्ट निर्देश नहीं’ का आड़ लेकर वे फिर से निरंकुश होने की फिराक में नहीं है?
याद करने की बात है कि ‘सम्पूर्ण क्रांति’ के मूल में व्यवस्था परिवर्तन से ज्यादा व्यवस्था को नियंत्रित करने का नारा था। किंतु दुर्भाग्य से वह अभियान भी सत्ता में पार्टी परिवर्तन का सबब बनकर रह गया। सम्पूर्ण क्रांति का नेतृत्व व अनुयायी दोनों ही सत्ता परिवर्तन से संतुष्ट होकर रह गये। वे यह गारंटी देने में भी असफल रहे कि परिवर्तित सत्ता लोक द्वारा नियंत्रित होती रहेगी। यही वजह है कि संपूर्ण क्रांति अभियान ने जहां अच्छे समाजसेवी, राजनीतिज्ञ व प्रोफेसर, लेखक व पत्रकारों की एक भरी-पूरी जमात को जन्म दिया, वहीं चारा खाने वाले की एक भरी-पूरी जमात भी उसी अभियान से जन्मी।
यह बात यह सिद्ध करती है कि व्यवस्था में बदलाव या व्यवस्था को जबरन नियंत्रित करने की लड़ाई कुछ समय के लिए चल चाहे जो जाये, हो सकता है कि इसकी बदौलत कभी हमें बेहतर शासन भी देखने को मिल जाये, लेकिन जैसे ही लगाम लगाने वाला लगाम ढीली छोड़ देगा, व्यवस्था पुन: बेलगाम हो जायेगी। किंतु इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम व्यवस्था को अनुशासित करने का काम करना बंद कर दें।
इतिहास में सत्ता को अनुशासित करने के भारतीय उद्धरण कई हैं। धर्मपथ से च्युत होने पर इन्द्र जैसे देवप्रमुखों को भी अपने पद से अलग होना पड़ा। लोकलज्जा के कारण सीता ने अग्नि परीक्षा दी। राम ने सीता का परित्याग किया। लंबे समय तक धर्मगुरुओं ने राजसत्ता को अनुशासित करने का काम किया। अलग-अलग काल में महात्मा विदुर-चाणक्य जैसे बुद्धिजीवियों ने भी। हां! इसका मतलब यह जरूर है कि यदि इस तंत्र में लोक ही सब कुछ है, तो दोषी सिर्फ तंत्र को कैसे ठहराया जा सकता है?
यहां विवेकानंद और तिलक के बीच घटित उस प्रसंग को भी याद करना जरूरी है, जिसमें तिलक ने गुलामी को राजनैतिक समस्या माना था और विवेकानंद ने चारित्रिक। गांधी जी ने भी आजादी के बाद यही माना था कि अब कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक संघ का गठन हो, जो लोकसेवा, बुनियादी शिक्षा, स्वावलंबन व चरित्र निर्माण का काम करे। हालांकि इस पर यह प्रश्न करना भी जायज है कि चरित्र निर्माण के काम में तो कई दशक लग जायेंगे, तब तक तो भ्रष्टाचार व अनाचार की इंतेहां हो जायेगी, लुटेेरे देश लूटकर चले जायेंगे, क्या इसका इंतजार करें? सवाल का जवाब एक ही है, संकट चौतरफा है, तो प्रयास भी चौतरफा ही होने चाहिए। किंतु प्रयास करने वाले तो हम ही हैं। अत: पहले हम बेहतर हों।
भारत का अतीत भय के प्रतीक यमराज से प्रश्न करने वाले नन्हे नचिकेता का है, सवाल का जवाब न देने पर धर्म के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर के बलिष्ठ भाइयों को दण्डित करने वाले यक्ष का है। अत: पहले समाज के अगुवा अपने भीतर नचिकेता सी निडरता व यक्ष सी दृढ़ता व नैतिकता तो लायें, एक दिन तंत्र भी अनुशासित हो जायेगा और शेष लोक भी।
तंत्र नियंत्रण के लोक औजार लोक घोषणापत्र-लोकनिगरानी-लोक अंकेक्षण
लोक घोषणापत्र
पार्टियां ही उम्मीदवार तय करती हैं। पांच साल वे क्या करेंगी; इसका घोषणापत्र भी पार्टियां ही तय करती हैं। फिर पांच साल लोकप्रतिनिधि के तौर पर चुने गये उम्मीदवार जो करते हैं, उसमें भी लोक की कोई भूमिका नहीं होती। मतदान न करने वाले मतदाताओं का यह रोना अभी आम है।
याद कीजिए कि इस पर गौर करते हुए इस बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर क्षेत्रवार घोषणापत्र जारी करने की घोषणा की थी। भाजपा भी कह रही थी। कि वह लोगों की राय से अपने घोषणापत्र को अंतिम रूप देगी। उसने कहा कि वह इस प्रक्रिया के तहत अपने प्रतिनिधियों से राय लेगी। जनता-जर्नादन की राय के लिए उसकी वेबसाइट खुली रहेगी। किंतु उसने यह भी कहा था कि राय कुछ भी हो, राममंदिर जैसे अपने एजेंडे से वह पीछे नहीं हटेगी। यह कदम दिखावटी हो, तो भी लोक की सुनने के लिए आगे बढ़ा था, अत: सराहनीय था। इसकी अंतिम परिणति लोक घोषणापत्र ही होती। कई संगठनों ने नागरिक घोषणापत्र, पर्यावरण घोषणापत्र के नाम से यह प्रयास पहले भी किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में न आम आदमी पार्टी ने पार्टी घोषणापत्र बनाने के लिए रायशुमारी का क्रम जारी रखा और न ही भाजपा ने।
लोक घोषणापत्र का मतलब है- लोगों की नीतिगत तथा कार्य संबंधी जरूरत व सपने की पूर्ति के लिए स्वयं लोगों द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज। प्रत्येक ग्रामसभा/मोहल्ला समितियोंं को मौजूद संसाधन, सरकारी-गैरसरकारी सहयोग, आवंटित राशि तथा जनजरूरत के मुताबिक अपने इलाके के लिए अगले पांच साल के सपने का नियोजन करना चाहिए। उसे हर साल परिमार्जित करने का विकल्प खोलकर रखना चाहिए। इस लोक एजेंडे या लोक नियोजन दस्तावेज को लोकघोषणापत्र का नाम दिया जा सकता है। इस लोक घोषणापत्र को किसी बैनर या फ्लेक्स पर छपवाकर अथवा सार्वजनिक मीटिंग स्थलों की दीवार पर लिखकर चुनाव प्रचार के लिए आने वाले चुनावी उम्मीदवारों के समक्ष पेश किया जा सकता है। उनसे उसकी पूर्ति के लिए संकल्प लिया जा सकता है। इससे उम्मीदवार के चयन में भी सुविधा होगी और पालन करने के लिए उम्मीदवार के सामने अगले पांच साल एक दिशा-निर्देश होगा।
लोक अंकेक्षण
लोकप्रतिनिधियों के बजट से क्रियान्वित होने वाले कार्यों में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए फंड का लोक अंकेक्षण यानी ‘पब्लिक ऑडिट’ अनिवार्य हो। ऑडिट सिर्फ वित्तीय नहीं, कैग के नए विविध सूचकांकों के आधार पर होना चाहिए। इसका तरीका बहुत साधारण है। हमारे पास ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, मोहल्ला समिति, वार्ड समिति, जैसे संगठन पहले से ही मौजूद हैं। भिन्न-भिन्न स्तर पर उनसे नीचे के स्तर की प्रतिनिधि सभाओं द्वारा नामांकित सदस्यों की सदस्यता वाली लोक-अंकेक्षण समितियों का गठन किया जा सकता है। यह समितियां अपने लोकप्रतिनिधि को बाध्य कर सकती हैं कि लोक घोषणापत्र व लोकमांग के अनुरुप बजट का आवंटन करे। वह लोकप्रतिनिधि को कह सकती हैं कि वह प्रति तिमाही अपने खाते के बजट व कार्य का लेखाजोखा लोक-अंकेक्षण समूह के समक्ष प्रस्तुत करे। लोक अंकेक्षण समिति के किसी भी सदस्य द्वारा मांगे जाने पर लोकप्रतिनिधि लेखा व कार्य विवरण की रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को सदैव बाध्य हो।
पांच साल पूरे होने पर लोक अंकेक्षण समूह की रिपोर्ट खुद-ब-खुद इस बात का आइना होगी कि निवर्तमान प्रत्याशी उसमें अपना चेहरा देख सके; जान सके कि वह अगली बार चुनाव लडऩे लायक है या नहीं। पर्टियां भी इस आधार पर अपना उम्मीदवार तय कर सकती हैं और लोग भी कि उस प्रतिनिधि को अगली बार चुना जाये या दरकिनार कर दिया जाये। पंचवर्षीय लेखा जोखा अगले पांच वर्षीय कार्यों का नियोजन व तद्नुसार लोक घोषणापत्र निर्माण में भी बराबर का मददगार सिद्ध होगा। यदि जनता यह जवाबदारी निभा सकी, तो तंत्र पर लोक की हकदारी स्वत: आ जायेगी। कभी यह प्रयोग करके देखना चाहिए।
लोक निगरानी
हालांकि केन्द्र द्वारा भेजे एक सैकड़ा पैसे के नीचे तक पहुंचते-पहुंचते तीन दहाई रह जाने संबंधी राजीव गांधी के बयान की चर्चा आज भी खूब होती है, किंतु योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की कोई गंभीर कोशिश आज तक नहीं हुई। दिल्ली सरकार की ‘जनभागीदारी’ भी इस मामले में आंशिक भूमिका ही निभा पा रही है। लोकनिगरानी इस सपने को सच करने का भी एक कारगर औजार हो सकती है और तंत्र पर नकेल कसने का भी।
योजना को ठीक से जानना-पहचाना, उसके हर पहलू पर नजर रखना, लाभार्थियों को पहले से अवगत कराना, योजना में कमी है तो टोकना, उन्हें दूर करने के लिए मजबूर करना, योजना ठीक से लागू हो; इसमें अपनी भूमिका की तलाश कर उसका निर्वाह करना, योजना के दुश्मनों को दूर करना और कर्मनिष्ठ सहायकों को मदद देना व सम्मानित करना, समय-समय पर योजना की हकीकत को उजागर करना। ये काम अत्यंत जिम्मेदारी, सावधानी, कौशल व सातत्य की मांग करते हैं। इसके लिए लोकनिगरानी समूहों के गठन, प्रशिक्षण, कौशल विकास, संवैधानिक मान्यता व हकदारी की निर्णायक पहल समाज को स्वयं करनी चाहिए। निगरानी समूहों की आवाज सरकार में सुनी जायेगी, यह भरोसा सरकार, स्वयंसेवी जगत, पत्रकार, अदालत सभी को मिलकर देना चाहिए।
मैं मानता हूं कि लोक निगरानी तंत्र जैसे-जैसे विकसित होंगे लोकतंत्र भी विकसित होगा। अभी तंत्र आगे है, लोक पीछे। तब लोक आगे होगा व तंत्र सहायक की भूमिका में। शासन-प्रशासन जनता की सुनने को मजबूर होंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम स्वत: लग जायेगी। लोकसहभागिता स्वत: सुनिश्चित होने लगेगी। यह आदर्श स्थिति होगी। इसकी अभी हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। हां! बीज बो सकते हैं। उसे खाद-पानी, निराई-गुडाई कर सकते हैं। बगैर चिंता किए कि क्या होगा…. शुरूआत तो करें। निश्चित जानिए कि नतीजा तो निकलेगा ही। कभी देखा यह सपना भी एक दिन सच हो ही जायेगा।
स्वानुशासन, तभी सुशासन
व्यवस्था अपने आप में कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं होती। वह जो कुछ भी होती है, उसे बनाने व संचालित करने वालों की नीति, नीयत और क्षमता होती है या यूं कहें कि व्यवस्था शासित या शासक के बीच का अंतर्संबंध और चालक होती है। अत: सुव्यवस्था के लिए जरूरत व्यवस्था में बदलाव की नहीं, शासित व शासक के अंतर्संबंधों में अनुशासन व एक-दूसरे के सम्मान, पोषण व रक्षण-संरक्षण की है। इस तैयारी के साथ चलने वाली कोई भी व्यवस्था सुव्यवस्था हो सकती है; फिर वह भले ही राजतांत्रिक व्यवस्था ही क्यों न हो। लोकतंत्र भी एक व्यवस्था का ही नाम है। यदि लोक की नीति, नीयत और क्षमता में दोष होगा, तो तंत्र स्वत: दोषपूर्ण हो जायेगा। यह निर्विवाद सत्य है। भारतीय लोकतंत्र में भी अब यह सत्य स्वीकारने का वक्त आ गया है। जाहिर है कि जरूरत व्यवस्था को गाली देने की नहीं, स्वयं के सामने आइना रखकर अपने गुण-दोष निहारने की है।
लोक समुदाय की मूल भारतीय संकल्पना पर निगाह डालें, तो हम पायेंगे कि यह संकल्पना भारतीय संस्कृति के दो महत्पवूर्ण पहलुओं की बुनियाद पर बुनी गई थी- ‘सहजीवन’ और ‘सहअस्तित्व’। ये सांस्कृतिक पहलू जीवन विकास संबंधी डार्विन के उस वैज्ञानिक सिद्धांत को भी पुष्ट करते हैं, जो परिस्थिति के प्रतिकूल रहने पर मिट जाने और अनुकूल तथा सक्रिय रहने पर विकसित होने की बात कहता है। लॉर्ड मेटकाफ की नजरों में समुदाय होकर ही भारत का गांव समाज सदियों तक ऐसी परिस्थितियों में भी टिका रहा, जिन परिस्थितियों में दूसरी हर वस्तु। व्यवस्था का अस्तित्व मिट जाता है। स्पष्ट है कि यदि तंत्र व लोक को भी एक-दूसरे का अस्तित्व मिटाये बगैर एक साथ बने रहना है तो एक-दूसरे को चुनौती देने की बजाय एक दूसरे के साथ सहजीवन व सहअस्तित्व का भाव बनाना होगा। ऐसा तभी संभव है, जबकि तंत्र व उसे सर्जित व संचालित करने वाला लोकसमुदाय दोनों स्वानुशासित हों। भारत का इतिहास इस बात को और पुख्ता तरीके से प्रमाणित करता है।
वैदिक काल में विश: ऐसी समिति थी, जो राजा तक का चुनाव करती थी। इसी समिति के माध्यम से प्रत्येक गांव में एक नेता चुना जाता था। उसे ‘ग्रामणी’ कहा जाता था। प्रत्येक गांव एक छोटा सा स्वायत्त राज्य था। स्वायत्त होने के बावजूद यह व्यवस्था अराजक नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजा व गांव एक-दूसरे की सत्ता को चुनौती देने की बजाय एक-दूसरे के पोषक और रक्षक की भूमिका में थे। एक मां तो दूसरा संतान। जहां राजा का पद वंशानुगत होता था; वहां भी राजा को आर्य नियमों के विरुद्ध जाने नहीं दिया जाता था। वाल्मीकि रामायण में गणराज्यों और उनके मेल से बने संघों का वर्णन है। रामायण कालीन राज्य सभा में सर्वाधिक शक्तिशाली अंग ‘पौर जनपद’ था। पौर जनपद में राजधानी के नैगम और गण्वल्लभ तथा ग्रामप्रांत के ग्रामघोष, महत्तर और समविष्ट होते थे। जनाक्षेप के आधार पर राजा राम द्वारा सीता के परित्याग का कथानक प्रमाण हैं कि गांव समितियों का हस्तक्षेप तब राज्यसभा तक था। किंतु इसके उलट राजा ने कभी ग्रामीण संस्थाओं के कार्य में अपनी ओर से हस्तक्षेप नहीं किया। बावजूद इसके लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करते थे। मौर्यकालीन व्यवस्था इसका अनुपम उदाहरण है।
कालांतर में जब कभी संतान अपने कर्तव्य से च्युत हुई तो उन्हें अनुशासित करने के लिए मां ने डांट भी पिलाई। लेकिन यह तंत्र व लोक के बीच का असल व आदर्श रिश्ता मां और संतान का है; यह तथ्य निर्विवाद रहा। आज भी है।
व्यवस्था परिवर्तन का लोकमार्ग लोक उम्मीदवार
लोकप्रतिनिधि सभाओं को दलों की दलदल से उबारने के लोकमार्ग के रूप में लोकउम्मीदवारी को काफी अरसे से एक विकल्प के रूप में पेश किया जाता रहा है। जो तंत्र पर लोक के काबिज होने को ही बेहतरी व बदलाव का एकमेव मार्ग मानते हैं, वे भी लोकउम्मीदवारी के विचार को उभारने के पक्षधर हैं। पार्टी उम्मीदवार, निर्दलीय व लोक उम्मीदवार में बुनियादी फर्क कई हैं। पार्टी उम्मीदवार पार्टी द्वारा तय किया जाता है। निर्दलीय उम्मीदवारी स्वेच्छा से अपनी उम्मीदवारी पेश करता है। लोक उम्मीदवार की उम्मीदवारी उस जनता के बहुमत द्वारा तय की जाती है, जिनका उसे प्रतिनिधित्व करना है। ऐसी उम्मीदवारी के मामले में पहले से अनुबंध होता है कि लोक व उम्मीदवार दोनों एक-दूसरे के प्रति जवाबदेह होंगे। लोक उम्मीदवार लोकप्रतिनिधि के रूप में लोक के एजेंडे को अपना एजेंडा बनायेगा। लोक के लिए किए गये कार्य की योजना, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में लोक को शामिल करेगा। लोक की उम्मीदों पर खरा न उतरने की स्थिति में लोक को हक होगा कि वह अपने द्वारा ही नामांकित-चयनित लोकप्रतिनिधि को वापस बुला सकें। दलगत व निर्दलीय उम्मीदवार उक्त चार में से एक भी शर्त को मानने को अभी बाध्य नहीं हैं। नि:संदेह लोक उम्मीदवार एक सपना है। ग्राम से लोकसभा तक इसे सच करने के रास्ते विनोबा ने भी सुझाये थे। अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रपति चुनने के तौर-तरीके को भी कोई-कोई लोक उम्मीदवार का दर्जा दे देते हैं।
आज दलों के दलदल और निर्दलीय की भी लोक के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित न होने से आजिज आ चुके मतदाताओं के एक बड़े वर्ग द्वारा मतदान न किए जाने की स्थिति में लोकउम्मीदवार का महत्व और बढ़ जाता है।
अरूण तिवारी