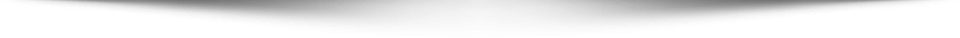2019 का लोकसभा चुनाव मोदी के राष्ट्रवाद पर आकर टिक गया है। एक ओर मोदी की मजबूत राष्ट्रवाद की परिकल्पना है तो दूसरी तरफ कमजोर विपक्ष है। एक तरफ मोदी के द्वारा पांच साल में कराये गए कार्यों की रूपरेखा है तो दूसरी तरफ इस दौरान पूरी तरह बिखर चुका विपक्ष है। एक तरफ अबकी बार 400 पार का नारा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के जरिये स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्ष करता विपक्ष है। इन सबके बीच ‘मैं भी चौकीदार’ का नारा लगाते भाजपाई सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम को जपते दिख रहे हैं। चाय से चौकीदार का यह खेल खेलने में मोदी की टीम सफल होती दिख रही है। 2014 में अपने शपथ ग्रहण के दौरान मोदी ने सार्क देशों के सभी प्रतिनिधियों को बुलाकर एक नयी तरह की मोदी कूटनीति की शुरुआत की थी। अभिनंदन की समय से वापसी उसी कूटनीति का एक परिणाम थी। इस समय सभी इस्लामिक देश भारत के साथ दिखाई दे रहे हैं। समय के साथ साथ मोदी सरकार के प्रारम्भिक दिनों में असहिष्णुता का नारा बुलंद करने वाले विपक्षियों के मुंह पर ताला लग चुका है। इसके साथ ही दुनिया के इस्लामिक देश भी अब यह बात मानने लगे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं। मोदी का राष्ट्रवाद दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। राष्ट्रवाद की अन्तर्राष्ट्रीय हवा अब मोदी के अनुसार चल रही है। इस राष्ट्रवाद की भावना को बल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के द्वारा मिलता साफ दिखता है। मोदी का ध्यान अपनी कूटनीति में पहले दुनिया के देशों को अपने साथ लाना और उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रभाव जमाना था। जिसमें वह पूरी तरह से कामयाब भी दिखते हैं। चूंकि, मोदी को निर्णय लेना आता है इसलिए वह आगे बढ़कर नेतृत्व करना जानते हैं। उनकी यह अदा ही उन्हें अन्य नेताओं से अलग एवं जनता में लोकप्रिय बनाती है। मोदी खतरे लेना जानते हैं। पहले उन्होंने दलित वोटों में सेंध लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलटने का जोखिम लिया, इसके बाद जब तीन राज्यों में हार हुयी तो आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके उस जोखिम की भरपाई भी कर ली। इस तरह से उन्होंने अपने सभी पत्ते फेंट कर 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार भी किया। इसके बाद जब पुलवामा में हमला हुआ तब उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की। अब मोदी के सामने लक्ष्य आतंकवाद के खिलाफ शुरू की गयी इस लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचाने का है। चूंकि वर्तमान में मोदी के सामने विपक्ष नदारद है इसलिए उनकी अपनी ही पार्टी में एक विपक्ष उनके खिलाफ तैयार हो रहा है। आडवाणी और जोशी के टिकट काटकर वह पुराने भाजपाइयों के निशाने पर और ज़्यादा आ गये हैं। इसके साथ ही कई केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों के टिकट काटने के कारण मोदी का विपक्ष उनके अपने ही लोग बनने लगे हैं। अब मोदी की जिजीविषा और राष्ट्रवाद की अग्निपरीक्षा जनता की कसौटी पर खरी उतरने का समय आ गया है।
द्य अमित त्यागी
भारत के लोकसभा चुनाव एक राष्ट्रीय विमर्श पर आधारित होते रहे हैं। उनमें एक वोटिंग पैटर्न पाया जाता है। इसे कुछ ऐसे समझिए। 1952 का पहला लोकसभा चुनाव स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का पहला चुनाव होने के कारण स्वतन्त्रता संग्राम के विमर्श एवं भारत के निर्माण पर आधारित था। आज़ादी दिलवाने में कांग्रेस के योगदान के कारण कांग्रेस के प्रति लोगों में सहानुभूति थी। राष्ट्रीय विमर्श देशभक्ति था और कांग्रेस देश के सामने एक मात्र विकल्प बनकर उभरी थी। देश ने दोनों हाथों से जवाहरलाल नेहरू को बहुमत दिया। इसके बाद देश का अगला चुनाव 1957 में हुआ। इस चुनाव में भी स्वतन्त्रता आंदोलन की खुमारी हावी रही और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। 1962 तक तीसरे लोकसभा चुनाव आते आते देश में स्वतन्त्रता संग्राम की खुमारी उतरने लगी थी। हालांकि, राष्ट्रीय विमर्श का विषय तब भी देशभक्ति ही रहा। नेहरू दौर तब तक अपने उतराव की ओर बढ़ रहा था। 1962 के चुनावों में सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी के द्वारा नेहरू को अच्छा खासा झटका भी दे दिया। हालांकि वह ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब नहीं रहे किन्तु मानसिक रूप से यह सत्ताधारी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। पुराने जमाने के राजाओं, जमीदारों और पूंजीपतियों के विरोध का यह आरंभकाल था। प्रजातन्त्र में विपक्ष और परिवर्तन जरूरी है का नारा भी उनके द्वारा दिया गया था। 1962 का वह दौर राष्ट्रीय विमर्श के शिफ्ट होने का दौर था। देशभक्ति की भावना के राष्ट्रीय विमर्श धीरे धीरे गरीब और अमीर के राष्ट्रीय विमर्श में बदलने की शुरुआत इसी काल के दौरान हुयी।
1967 आते आते स्वतंत्र पार्टी और आगे बढ़ी और कुछ सीटों पर विजय भी प्राप्त की। नेहरू के न रहने के बाद इन्दिरा गांधी के लिए यह पहला चुनाव था। इस बार इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जीत तो गयी किन्तु लडख़ड़ाते हुये। इन्दिरा गांधी ने इससे उबरने का रास्ता निकाला। देश का राष्ट्रीय विमर्श जो गरीब और अमीरों के बीच की दूरी बन रहा था उस पर काम किया। राजाओं और महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म कर दिये गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी राशि देने पर रोक लगा दी गयी। इस तरह राष्ट्रीय विमर्श के अनुकूल चलकर इन्दिरा गांधी ने 1971 में एक प्रचंड जीत हासिल की। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विमर्श को चुनावी वोटबैंक में बदलने का हुनर बखूबी जानती थी। नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में उनसे दो कदम आगे नजऱ आते हैं। वह देश का राष्ट्रीय विमर्श स्वयं अपने हिसाब से निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं। वह और उनकी भाजपा की टीम को अपने अनुकूल राष्ट्रीय विमर्श निर्धारित करना आता है।
जैसे पहले भाजपा को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था। तब पहले भाजपा ने पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और अनुसूचित जाति से आने वाले रामनाथ कोविन्द को राष्ट्रपति बनाकर यह धारणा तोड़ दी। इसके बाद अनुसूचित जाति विधेयक पर जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया तब उसको पलट कर भाजपा ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने का बड़ा जोखिम लिया। इसके बाद जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण चुनाव हुये तब भाजपा को अपनी इस नीति से नुकसान उठाना पड़ा। इसकी भरपाई के लिए भाजपा ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का एक मास्टर स्ट्रोक चला। एक झटके में सवर्णों की नाराजगी दूर हो गयी। इसके साथ ही देश में एक राष्ट्रीय विमर्श राम मंदिर के रूप में चल रहा था। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढऩे के क्रम में भाजपा की छवि एक हिंदुवादी दल की बन सकती थी इसलिए भाजपा ने इस राष्ट्रीय विमर्श को चुनावी विमर्श नहीं बनने दिया। इसी बीच पुलवामा में घटना हो गयी। यहां नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पूरे देश में राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति एक राष्ट्रीय विमर्श बन गया। चूंकि इस समय देश में चुनावी मौसम आ चुका था इसलिए इस राष्ट्रीय विमर्श को चुनावी विमर्श बनाने में मोदी की टीम ने कोई देर नहीं की। मोदी के विरोधियों ने इस देश की जनता के बीच चलने वाले इस विमर्श की नब्ज़ को सही से नहीं पकड़ा। वह सर्जिकल स्ट्राइक में कितने मरे या नहीं मरे, इस बात में उलझ गए। जनता के बीच विपक्ष के लिए इसके द्वारा एक नकारात्मक संदेश गया। सेना की कार्यवाही पर संदेह करना भारत की जनता को रास नहीं आता है।
ऐसी धारणा बनी कि विपक्षी दल जमीनी हक़ीक़त को समझें बिना सिर्फ मोदी को घेरने के लिए सवाल कर रहे हैं। विपक्ष के सवाल तो इतने अजीब हैं कि वह पाकिस्तान के लिए अपने पक्ष में भुनाने का माध्यम बन रहे हैं। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि विषय यह नहीं है कि बालाकोट में कितने आतंकी मारे गए। विषय इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विषय यह है कि 50 सालों के इतिहास में पहली बार भारत की वायु सेना ने पाकिस्तान में भीतर जाकर प्रहार किया। जिस पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से पुरानी सरकारें डर जाया करती थी उस गीदड़ भभकी में शेर दिल मोदी नहीं आए और सेना को छूट दे दी। 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तब देश में राष्ट्रीय विमर्श राष्ट्रवाद बना था। तब भी सरकार से जनता की अपेक्षा थी कि वह पाकिस्तान के भीतर जाकर प्रहार करे। तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार इसमें चूक गयी थी। मोदी ने राष्ट्रीय विमर्श के इस विषय को भुना लिया। शायद मोदी के निर्णय लेने की यह क्षमता ही उन्हें बेहतर स्टेट्समैन बनाती है। देश में एक बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा है जो किसी दल का मतदाता नहीं होता है। उसे फ्लोटिंग वॉटर कहा जाता है। मोदी के इस निर्णय के बाद वह मतदाता देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद की छत्र छाया में भाजपा के पक्ष में मतदान करता दिख रहा है।
राष्ट्रवाद की पुरानी धारणाएं तोड़ते मोदी
भारत पर पहली बार कोई आतंकवादी हमला हुआ हो ऐसा नहीं है। पुलवामा में हुआ हमला दशकों से हो रहे हमलों की एक अगली कड़ी मात्र था। इसके पहले जब संसद पर हमला किया गया था तब अटल बिहारी ने सेना को सीमा पर भेज दिया था। दो महीने तक सेना सीमा पर दिल्ली से आदेश आने का इंतज़ार करती रही किन्तु कोई आदेश नहीं आया। इसके बाद सेना वापस लौट आई। इसके बाद जब 2008 में मुंबई में हमला हुआ तब भी मनमोहन सिंह ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि वह सेना को इजाजत दे पाते। वायुसेना के पायलट काकपिट में बैठे आदेश का इंतज़ार कर रहे थे किन्तु दिल्ली तब भी आदेश देने से चूक गयी थी। अब जब 2019 में मोदी सरकार के दौरान पुलवामा में हमला हुआ तब भी भारत सरकार की ओर से रटा रटाया जवाब आया कि हम पाकिस्तान को कड़ा जवाब देंगे। भारत की जनता को लगा कि हर बार की तरह इस बार भी कोई कार्यवाही नहीं होगी। जब मोदी ने कहा कि हमने सेना के हाथ खोल दिये हैं तब उनकी इस बात का मज़ाक बनाया गया कि क्या अब तक हाथ बांधे हुये थे? किन्तु इस बार कहानी शायद दूसरी थी। उरी का बदला दस दिनों में और पुलवामा का बदला बारह दिनों में ले लिया गया। मोदी ने इस मिथक को तोड़ दिया कि परमाणु हथियार होने के कारण पाकिस्तान पर हमला नहीं किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी पैठ बना चुके मोदी को दुनिया के देशों को यह समझाने में कतई देर नहीं लगी कि भारत के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर किया गया वार आत्मरक्षा के लिए था न कि युद्ध के लिए उकसाने का प्रयास।
मोदी के इस निर्णय की तारीफ करने में विपक्षी लगातार कंजूसी करते रहे। उनको पाकिस्तान हमले से तो सुखद अनुभूति हुयी किन्तु मोदी को श्रेय देना उनके लिए टेढ़ी खीर रहा। वह इसके लिए लगातार सेना को श्रेय देते रहे। अब ऐसे लोगों को यह बात भी समझ नहीं आती है कि यह वही सेना थी जिसे अटल जी और मनमोहन सिंह ने छूट नहीं दी थी। दोनों ही समय सेना को पराक्रम दिखाने का अवसर दिल्ली के राजनीतिक नेतृत्व ने नहीं दिया। मोदी के कार्यकाल में सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो कार्यवाही की है उसके पीछे सिर्फ दो चार दिन की मेहनत नहीं है बल्कि पिछले पांच साल की ज़बरदस्त कूटनीति भी है। मोदी ने मुस्लिम राष्ट्रों में ज़बरदस्त पैठ बना ली है। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रों में अलग थलग पड़ गया है। दुनिया के सभी मुस्लिम देश यह मानते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है। गुजरात के दंगों के बाद मोदी की छवि को बिगाडऩे का जो अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा गया था उसको मोदी ने नेस्तनाबूद कर दिया है। अब सिर्फ चीन और सऊदी अरब को छोड़कर बाकी सभी देश पाकिस्तान में चल रहे आतंकी अड्डों को खत्म करने की भारत की कार्यवाही का स्वागत एवं समर्थन करते हैं। इसी कारण भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर स्थित खैबर पख्तूनख्वा में हमला करके जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद अभिनंदन की सकुशल रिहाई एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। फैसले लेने की क्षमता, सफल कूटनीति और देशहित में जोखिम लेने की काबलियत रखने वाला यह राष्ट्रवाद अब चुनावों में कितना प्रभाव दिखा पाएगा, इसकी परख अभी बाकी है।
अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की धुरी बनते मोदी
2008 में जब विश्व में मंदी का दौर आया तब सम्पूर्ण विश्व में स्वदेशी और राष्ट्रवाद की भावना बलवती होनी शुरू हो गयी। देश प्रथम के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार निर्धारित होने लगा। चूंकि, मंदी के बाद विकसित देशों के लोग भी माल कल्चर और केंद्रीयकृत व्यवसाय के विरोध में दिखने लगे तो लगभग सभी देशों में अपने देश को आगे बढ़ाने का भाव घर करने लगा। मोदी जब 2014 में आए तब तक यह भाव अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपना प्रभाव जमा चुका था। इसके बाद इसी भाव के ऊपर अमेरिका में ट्रम्प की सरकार बनी। ट्रम्प और मोदी दोनों में एक समानता यह है कि दोनों राष्ट्रवाद और राष्ट्रप्रथम की अवधारणा पर काम करते हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं उसी राष्ट्रवाद का व्यापारिक स्वरूप हैं। दोनों के बीच अच्छा आपसी समंजस्य भी दिखता है। दोनों के बीच बेहतर व्यापारिक रिश्ते हैं। अमेरिका चीन को संतुलित करने के लिए भारत के साथ जुड़ा है तो पाकिस्तान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था के कारण अमेरिका और चीन के आगे हाथ फैलाये खड़ा रहता है। इस कारण भारत जाने अंजाने अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ा बाज़ार होने के कारण महत्वपूर्ण धुरी बन जाता है।
अब जब अगर कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मजबूत स्थिति में होता है तो उसके राष्ट्राध्यक्ष के पास सिर्फ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। पूरा विश्व समुदाय उसके साथ आ जाता है। किन्तु विपक्ष के द्वारा अगर विरोध नहीं किया जाएगा तो उनकी राजनीति कैसे पुष्पित और पल्लवित होगी। इसलिए सच्चाई को जानते हुये भी विपक्ष मोदी का विरोध करता रहता है। सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करना स्वस्थ लोकतन्त्र की निशानी नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम बड़े घातक होते हैं। इसे समझने के लिए अगर 2004 में वापस लौंटे तो वाम दलों ने उस समय कांग्रेस को समर्थन सिर्फ इसलिए दिया था कि भाजपा को सत्ता में आने से रोक सके। वामदलों ने कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद होने के बावजूद एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया। यह कार्यक्रम सिर्फ कागजों तक सीमित रहा और ज़मीन पर लागू नहीं हो पाया। 2008 में जब कांग्रेस ने अमेरिका से परमाणु करार किया तो वाम दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी वामपंथियों के इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तब सोमनाथ ने वाम दलों को आत्मविश्लेषण करने की सलाह देते हुये कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है। सोमनाथ चटर्जी की भविष्यवाणी थी कि अगले चुनावों में वामदलों को इस विरोध का नुकसान होगा। उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुयी और 2009 के चुनावों में वाम दल की सीटें काफी घट गईं।
कम्यूनिस्टों का तो स्वभाव मूलत: विरोध करना होता है। पर अब कांग्रेस भी उसी विचारधारा पर चल निकली है। उसके नेता बिना सोचे समझे सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते रहते हैं। महात्मा गांधी ने 1947 में वामपंथियों के लिए कहा था कि ”ये लोग समझते हैं कि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ी सेवा मनमुटाव पैदा करना, असंतोष को जन्म देना है। वह यह नहीं सोचते हैं कि यह असंतोष, ये हड़तालें अंत में किसे हानि पहुचाएंगी। ये लोग अब एकता को खंडित करने वाली उस आग को हवा दे रहे हैं जिसे अंग्रेज़ लगा गए थे।’’ गांधी जी का यह कथन आज की कांग्रेस के विरोध पर भी सटीक बैठता है। वह सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। अब राफेल के विषय को ही देखें तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी राहुल गांधी अपना राग अलापते रहे। एक तरफ वामपंथी माक्र्स के आधार भारत को समझने की भूल के कारण निष्प्रभावी हो गए तो दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ मोदी को तानाशाह और जुमलेबाज साबित करने के कारण निष्प्रभावी होने की कगार पर है।
चुनावी राजनीति और रणनीति में काफी आगे भाजपा
अब चूंकि चुनाव के चरण प्रारम्भ हो चुके हैं तो भाजपा की चुनाव की रणनीति की चर्चा भी आवश्यक है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए पांच बिन्दु महत्वपूर्ण होते हैं। उम्मीदवार, सांगठनिक ढांचा, कैंपेन का तरीका, राजनीतिक दल के बारे में जनता की धारणा एवं विरोधियों में उस दल के प्रति चिंता। 2014 में मोदी की लहर थी तो भाजपा के टिकट पर जो भी उम्मीदवार खड़ा हो गया वह जीत गया। लोगों ने उम्मीदवारों को नहीं मोदी को वोट दिया। जीतने के बाद वही हुआ जिसकी आशंका थी। अक्षम उम्मीदवार अपने लोकसभा क्षेत्रों में बेहतर काम नहीं करा पाये और उसका दोष मोदी के सिर पड़ा। भाजपा और मोदी प्रत्याशियों को बदलने का काम काफी समय से करते रहे हैं। यही उनकी विजय का फॉर्मूला होता है। पूर्व में दिल्ली एमसीडी चुनावों में भाजपा ने सभी प्रत्याशियों के टिकट काट दिये और भारी विरोध के बावजूद विजय प्राप्त की। इस बार छत्तीसगढ़ में सभी सांसदों के टिकट काट दिये गए हैं। इसके साथ ही लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिया गया है। केन्द्रीय कृषि कल्याण राज्यमंत्री कृष्णाराज एवं पूर्व मानव संसाधन राज्यमंत्री रामशंकर कथेरिया के भी टिकट कटे हैं। इस तरह से भाजपा अब नए उम्मीदवारों के साथ मैदान में है।
अगर संगठनिक ढांचे की बात करें तो 2014 की जीत के बाद से संघ और भाजपा लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं। दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के कारण जातिगत समीकरण भी भाजपा के अनुकूल होते चले जा रहे हैं। अब भाजपा हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता से जुड़ी है जो उसके लिए जीत का आधार बन सकता है। इसके साथ ही भाजपा का आईटी सेल और मीडिया उसकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मीडिया में सिर्फ और सिर्फ भाजपा दिखाई दे रही है। भाजपा के मुद्दे, भाजपा की विचारधारा और तो और भाजपा के प्रचार वाले विज्ञापन ही ज़्यादा दिखते हैं। जनता के बीच में भाजपा के लिए यह धारणा है कि यह एक हिंदुवादी पार्टी है। इसके द्वारा भाजपा को हिन्दू वोट मिलते हैं। चूंकि 2014 में पहली बार हिन्दू वोट बैंक एकजुट हुआ था इसलिए भाजपा उसे खोना नहीं चाहती है। इसके साथ ही अगर जातिगत आधार पर कहीं वोटबैंक कटता है तो इसके लिए तीन तलाक के विषय द्वारा मुस्लिम महिलाओं के वोटों पर भाजपा की नजऱ है। इसके लिए भाजपा ने अपनी छवि हिंदुवादी के स्थान पर राष्ट्रवादी की कर ली है। पाकिस्तान पर कार्यवाही के बाद अब भाजपा का राष्ट्रवाद धर्म से ऊपर चला गया दिखता है। जिस तरह से भाजपा ने उज्जवला, किसानों को धन, आवास एवं अन्य योजनाएं ज़मीन तक पहुंचाई हैं उसके बाद विपक्षियों में भाजपा से डर भी दिखाई देता है। शहरी और सवर्णों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा अब गांव, पिछड़ों, दलितों के साथ ही मुस्लिमों तक अपनी पैठ बना चुकी है।
मोदी बनाम कौन एवं अपूर्ण बहुमत की स्थिति
हालांकि तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद कमजोर विपक्ष एवं विकल्प हीनता की स्थिति के कारण मोदी की वापसी लगभग तय लग रही है। मोदी के सामने विपक्ष में कौन है यह स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष तो अवश्य हैं किन्तु वह एवं उनकी पार्टी सत्ता में आती नहीं दिख रही है। प्रियंका के आने से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित होती दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जितनी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है उसका उतना फायदा भाजपा को हो रहा है। गठबंधन के दोनों दल सपा-बसपा प्रियंका गांधी के कारण मतों के नुकसान में आ रहे हैं। अब प्रियंका गांधी नर्म हिन्दुत्व की राह पर चल पड़ी हैं। वह काशी विश्वनाथ सहित मंदिरों में दर्शन कर रही हैं। इसके द्वारा जो हिन्दू वर्ग भाजपा से नाराज़ है और केवल विकल्प हीनता के कारण मजबूरी में भाजपा को वोट देने वाला था वह कांग्रेस की तरफ जा सकता है। किन्तु ऐसे वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आज का मतदाता जागरूक है। वह इस बात को जानता है कि उसके वोट से स्थायी सरकार बन रही है या अस्थायी। उत्तर प्रदेश में 2007 के बाद से एक ट्रेंड रहा है। यहां मतदाता उस दल को प्रचंड बहुमत देता है जो जीतते दिख रही होती है। 2007 विधानसभा में बसपा, 2012 में सपा और 2017 में भाजपा को प्रचंड बहुमत उसी पैटर्न के आधार पर था। 2014 में भी जनता ने मोदी को प्रचंड बहुमत दिया था।
पर भाजपा के साथ एक समस्या भी है। भाजपा में भक्त ज़्यादा हो गए हैं। मैनेजर ज़्यादा हो गए हैं। लीडर की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके लिए मोदी की टीम भी जिम्मेदार है। मोदी की टीम ने जनाधार वाले नेताओं को बिलकुल किनारे कर दिया है। उनको लगता है कि राष्ट्रवाद और मोदी के नाम पर वह इतने वोट पा सकते हैं कि उन्हे जनाधार वाले नेताओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
लीडर कम होने से भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि उसके नेता विपक्ष के छोटे से छोटे कमेंट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। वह उपलब्धियों का बखान नहीं कर पाते हैं। जनता के बीच जुड़ नहीं पाते हैं। जैसे अगर देखा जाये तो भाजपा की सरकार के दौरान आतंकी घटनाएं और दंगे न के बराबर हुये किन्तु भाजपा इस विषय को जनता के बीच ले जाने में नाकामयाब रही। 24 घंटे बिजली का विषय भी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है। इसकी वजह है कि भाजपा में संघ से आने वाले बौद्धिक कम हो गए हैं। अब अन्य दलों से आए लोग ज़्यादा हावी हैं। इन सबके बीच मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती नौकरशाही है। नौकरशाही नहीं चाहती है कि भाजपा सरकार की वापसी हो। ऐसे में अगर भाजपा या एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राजनाथ सिंह एक ऐसा नाम हैं जो प्रधानमंत्री के बड़े उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। राजनाथ सिंह अन्य दलों के नेताओं को भी स्वीकार्य माने जाते हैं। एक अन्य विकल्प नितिन गडकरी का है जो संघ की विचारधारा से आते हैं। पर परिस्थितियों को देखते हुये और कमजोर विपक्ष के कारण मोदी सरकार की वापसी तय लग रही है।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
राजनीतिक धारणा बनवाता लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ
देश का प्रत्येक जागरूक नागरिक जानता है कि अब भारत की राजनीति देश सेवा का माध्यम नहीं रह गई है यह अब मात्र एक विशाल व्यापार बन गई है। तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां व्यापारिक कंपनियां बन चुकी हैं और आज की मीडिया इनकी मार्केटिंग मैनेजर, जिसको यह पार्टियां अपने अपने प्रचार के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भरपूर प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण है राजनीति का व्यापार भारत का सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। इस व्यापार में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से अरबों खरबों कमाए जा रहे हैं। या मेरी भाषा में कहें तो लूटे जा रहे हैं। इस लूट पर पर्दा पड़ा रहे इसके लिये मीडिया का प्रयोग बखूबी किया जा रहा है। मीडिया के मालिक, उनके पत्रकार, एंकर करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं। पार्टियों के चुनाव के एजेंडे अब जनता में मीडिया सेट कर रहा है। कुल मिलाकर देश की जनता मूल मुद्दों से कैसे भटके इसके लिये नेताओं और पार्टियों द्वारा मीडिया को खूब मैनेज किया जा रहा है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारी मीडिया ऐसी है या सभी पत्रकार पार्टियों के मार्केटिंग मैनेजर हो गये हैं। कुछ ईमानदार भी हैं जिनको शायद सत्ता की ताकत के साथ समझौता न करने यानी ईमानदारी का फल भी मिलता है। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बड़े पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी के साथ कुछ ऐसा ही होता प्रतीत हुआ जब एक बड़े संस्थान के कार्यक्रम मास्टर स्ट्रोक में सरकार की कमियों और भ्रष्टाचार को तथ्यों सहित बताते नजर आने पर चैनल के मालिक ने सरकार के दबाव में उन्हें चैनल से बाहर कर दिया। इसके पहले कई अन्य चैनल से भी वह बाहर होते रहे हैं। अभी एक नामचीन बिस्किट कंपनी के चैनल से भी बाजपेई जी दबाव से बाहर कर दिये गये। पुण्य प्रसून के लिए कुछ लोग कहते हैं कि वह सरकार को आईना दिखाते हैं तो कुछ लोग यह मानते हैं कि इसकी आड़ में वह अपना एजेंडा चलाते हैं। कुछ भी हो पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब लगता है पार्टियों और सरकारों के राजनीतिक परसेप्शन सेट करने का एक मजबूत स्तंभ बन गया है। निश्चित इसके लिये बड़ी कीमत भी मिलती होगी और चुनावी माहौल में तो मीडिया चैनलों के वारे न्यारे हो जाते हैं।
पर इसका एक दूसरा संवेदनात्मक पहलू है जो प्रत्येक भारतीय को समझना चाहिए। जो अपने को राष्ट्र के प्रति एवं राष्ट्र के लोगों के प्रति संवेदनशील मानते हैं उनको समझना चाहिये कि यह जो राजनीति के व्यापारियों का एवं उनके मीडिया मैनेजरों का व्यापार है वह निश्चित रूप से देश हित में नहीं है। अब आप करोड़ों अरबों रुपये के इस खेल को समझिये। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में एक सांसद के चुनाव में एक प्रत्याशी को कम से कम पांच से दस करोड़ खर्च करने पड़ते ही हैं और कहीं कहीं यह आंकड़ा पचास करोड़ तक पहुंचता है। अब यह समझना बहुत साधारण है कि जो व्यक्ति सांसदी के लिए करोड़ों लगायेगा वह जीतने के बाद अरबों कमायेगा ही। या यूं कहे कि वह इस व्यापार में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर ही अरबों कमाने के लिये कर रहा है। तो फिर प्रश्न है इस व्यापार में मुनाफा कहां से आएगा? यह अरबों कहां से कमाए जाएंगे? सीधा सा उत्तर है देश की जनता के हक की गाढ़ी कमाई और देश के संसाधनों की लूट होगी। अब यदि चुनाव में ईमानदारी से मुद्दा यह बने कि चुनाव में लडऩे वाले करोड़ो रूपये कहां से लाते हैं? कौन इनकी फंडिंग कर रहा है? और इन नेताओं का चाल चरित्र नियति कैसी है? क्या यह देश की सेवा के लिये चुनाव में आ रहे हैं या फिर उस देश के संवैधानिक डकैत बनने?
अब समझिये! मीडिया, सत्ता और पार्टियों के गठजोड़ में न नेता, न पार्टियों और न ही मीडिया के लिये शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, भुखमरी, पानी, बिजली, सुरक्षा आदि कोई बड़े मुद्दे हैं। यदि मुद्दे हैं तो सिर्फ जाति, धर्म, मंदिर मस्जिद और छदम राष्ट्रवाद का प्रोपेगंडा मात्र। अपने अपने वोटबैंक के हिसाब से पार्टियां अपने एजेण्डे को मीडिया मार्केटिंग द्वारा भावनात्मक रूप से खूब सजाती है जिससे इस सजावटी छद्मता से शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, रोजगार जैसे ज्वलंत एवं मूल मुद्दों की विद्रुपता को छुपाया जा सके। 2019 का लोकसभा चुनाव भी सभी पार्टियों और नेताओं के लिये बड़ा व्यापारिक अवसर है जहां लाखों करोड़ों का बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा जो शायद भारत की लचर शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था सुधारने के लिये पर्याप्त होता यदि इसका सुधारने में इस्तेमाल होता। इस लूट से बचने का केवल एक ही समाधान है कि जनता खुद जागे और समझे कि देश का नेता और सरकार कैसी होनी चाहिये एवं किन मुद्दों पर चुनी जानी चाहिये और इस बात को भी समझे कि वो मालिक है और नेता एवं ब्यूरक्रेट्स नौकर। इस बात को आज मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कुछ ईमानदार पत्रकारों और पत्रकारिता की वजह से सत्य बाहर आ ही जाता है। इसमें प्रमुख ‘डायलॉग इण्डिया’ जैसी पत्रिका है और उसका मंच जिसमें चाहे पक्ष हो या विपक्ष दोनों के ही सत्यों को बिना भेदभाव के कम से कम उजागर तो किया जाता है। राज्य के लोगों और और राजा अर्थात शासन करने वाले को सुख कब प्राप्त होता है या उसका सुख किसमें निहित है यह कौटिल्य के इस श्लोक में विदित है।
प्रजासुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां च हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम् ।।
प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, अर्थात् जब प्रजा सुखी अनुभव करे तभी राजा को संतोष करना चाहिए । प्रजा का हित ही राजा का वास्तविक हित है। वैयक्तिक स्तर पर राजा को जो अच्छा लगे उसमें उसे अपना हित नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रजा को जो ठीक लगे, यानी जिसके हितकर होने का प्रजा अनुमोदन करे, उसे ही राजा अपना हित समझे। (लेखक राष्ट्रवादी विचारक हैं। )
-अशित पाठक
(लेखक राष्ट्रवादी विचारक हैं)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
चुनाव में काले धन की आवक अब भी एक बड़ा विषय
चुनावों की घोषणा होते ही कालाधन आना शुरू हो जाता है। धन और बल के माध्यम से चुनावों को जीतने का इतिहास पुराना रहा है। बल पर नियंत्रण करने में तो चुनाव आयोग कामयाब रहा है किंतु धन पर नियंत्रण के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। वास्तव में चुनाव सुधार एवं कालाधन एक दूसरे के पूरक मुद्दे हैं। कालेधन को नियंत्रित किये बगैर चुनाव सुधार संभव नहीं है। चुनावी खर्च की जो सीमा चुनाव आयोग ने तय की है उसका व्यवहारिकता में पालन नहीं हो पाता है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण वजह है कि कालाधन पिछले रास्ते से आता रहता है। बड़े कार्पोरेट घराने पार्टियों को फंडिग करते हैं। जो संवैधानिक तो है पर अलग किस्म के कालेधन का एक स्रोत है। राजनैतिक दलों ने अब स्वयं के धन को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर कर लिया है। पार्टी फंडिग पर रोक लगाकर यह धन चुनाव आयोग को मिलना चाहिए एवं इसका आवंटन चुनाव आयोग द्वारा पार्टियों को होना चाहिए। जब ऐसा होने लगेगा तब चुनाव आयोग का दबाव राजनैतिक दलों पर होगा। चुनाव में कालेधन की आवक रुकेगी।
कालाधन एवं चुनाव सुधार के लिए लोग प्रतिक्षा में हैं। चुनाव सुधार के लिए अब संवैधानिक प्रावधानों को समझते हैं। संविधान का अनु. 324 चुनावों के दौरान आचार संहिता के माध्यम से चुनाव आयोग को स्थितियों को ‘नियंत्रित एवं निर्देशित’ करने का अधिकार देता है। स्थितियों को ‘परिवर्तित’ करने का अधिकार उसके पास नहीं है। चुनाव सुधार या चुनाव संबंधी उपबंधों में परिवर्तन का अधिकार अनु. 327 में संसद एवं अनु. 328 में राज्य सरकारों की विधायिका के पास होता है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो चुनाव आयुक्त होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1995 के वाद में मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकारों का विकेंद्रिकरण करते हुये अन्य दो चुनाव आयुक्तों को भी लगभग समान अधिकार देने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग यदि कभी मनमानी करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नियंत्रित भी कर देता है। ए.सी. जोस बनाम सिवम पिल्लई, 1984 के वाद में चुनाव आयोग ने मतदान में मनमानी की थी। 34 बूथों पर पारंपरिक तरीके से एवं 50 बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गिनती करवायी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक मानते हुये आयोग को निर्देशित किया था कि एक ही मतदान में दो तरह के मापदंड असंवैधानिक हैं। चुनाव आयोग को अनु. 327 के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। अनु. 324 को संज्ञान में लेते समय संविधान के अन्य उपबंधों को, खासतौर पर केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं संबंधित अन्य अनूसूचियों को भी संज्ञान में रखना चाहिए।
- चुनाव सुधार या चुनाव संबंधी उपबंधों में परिवर्तन का अधिकार अनु. 327 में संसद एवं अनु. 328 में राज्य सरकारों की विधायिका के पास होता हैं।
- आचार संहिता के माध्यम से चुनाव आयोग स्थितियों को ‘नियंत्रित एवं निर्देशित’ करने का अधिकार रखता है।
- चुनाव सुधार एवं कालाधन एक दूसरे के पूरक मुद्दे हैं। पार्टी फंडिग पर रोक लगाकर यह धन चुनाव आयोग को मिलना चाहिए एवं इसका आवंटन चुनाव आयोग द्वारा पार्टियों को होना चाहिए।
- धन और बल के माध्यम से चुनावों को जीतने का इतिहास पुराना रहा है। बल पर नियंत्रण करने में तो चुनाव आयोग कामयाब रहा है किंतु धन पर नियंत्रण के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है।
अब एक बात तो साफ है कि तकनीक का फायदा होता है किंतु तकनीक का दुरूपयोग पहले होता है। जितने होशियार व्यक्ति व्यवस्था में हैं उससे ज्यादा होशियार बाहर बैठे हैं।
-कंवरदीप सिंह
(लेखक एक बड़े मीडिया संस्थान में कार्यरत हैं)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
सोशल मीडिया बना रहा है बड़ा माहौल
एक आंकड़े के अनुसार 2.5 प्रतिशत का अंतर चुनाव परिणाम को प्रभावित कर देता है। सोशल मीडिया के द्वारा 6-8 प्रतिशत का स्विंग देखा जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया के राजनैतिक दोहन में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता है। विभिन्न राजनैतिक दलों के आईटी सेल कमर कस चुके हैं। आईटी विशेषज्ञों की टीमें नियुक्त करके उन्हें सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया को विशेष तरजीह दी थी। एक अध्ययन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का बीस फीसदी के करीब प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था। अब लोकसभा 2019 चुनावों में हर राजनीतिक दल और उसके नेता इस मंच का अधिकाधिक लाभ लेने की होड़ में शामिल हो चुके हैं। नए-पुराने नेताओं के फेसबुक खातों में हुई वृद्धि और उनके मार्फत सोशल मीडिया में बढ़ी सक्रियता भी इसी बात को तसदीक करती है कि सोशल मीडिया इस बार के चुनावों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। वर्ष 2014 एवं उसके बाद हुये चुनावों के परिणामों ने सोशल मीडिया के महत्व को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार डिजिटल क्षेत्र में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है। सरकार की उपलब्धियों व खामियों का आंकलन सोशल मीडिया के मंच पर होना प्रारंभ हो गया है।
अब नेता किसी चैनल के मोहताज नहीं हैं। वह फेसबुक लाइव से अपने फॉलोअर्स को सीधे संबोधित करते हैं। व्हाट्सऐप तथा फेसबुक पर किसी भी सूचना को बड़ी आसानी से वायरल किया जा सकता है। कुछ ही सेकेंडों में लाखों लोगों तक अपने दल की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता से साझा किया जा सकता है। युवाओं को रिझाने के लिए सोशल मीडिया असरदार एवं मुख्य हथियार है। राजनीतिक पंडितों को अब इसकी उपयोगिता समझ आ चुकी है। यही कारण है कि अभी से सोशल मीडिया का बाजार गर्म है। चुनावी रैलियों का आयोजन, भाषणों, वालपेपरों व स्लाइडों द्वारा प्रचार चुनावों में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया का एक नकारात्मक पक्ष भी है। खूबियों के बावजूद सोशल मीडिया की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जो राजनीतिक दलों और मतदाता दोनों को ही सतर्कता और संयम बरतने के लिए आगाह करती हैं। सोशल मीडिया सेंसरशिप से पूरी तरह से मुक्त है। इसमें जो भी व्यक्ति या दल अपना विचार जैसे चाहे, वैसे ही साझा कर सकता है और यहीं से असल संकट भी शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर कई बार अफवाहों के बाजार गरम हो जाते हैं और हालात बेकाबू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की संभावना हर कहीं बनी रहती है। युवाओं का हर पल स्मार्ट फोन की धुन पर गुजरता है, वहीं कर्मचारी व गृहिणियों के हाथों में भी स्मार्ट फोन पहुंच चुका है। स्मार्ट फोन में इंटरनेट का संचार जीयो जैसी सस्ती व बेहतर सेवा ने और भी तेज कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया किस पक्ष को ज्यादा लाभ दिला पाएगा यह तो वक्त ही बताएगा, पर जो दल तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल सुव्यवस्थित व नियमित ढंग से करेगा उसको सोशल मीडिया से लाभ तो जरूर मिलेगा।
शिवम यादव
(लेखक सोशल मीडिया के जानकार पत्रकार हैं। )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों की हमारी डिमांड इतनी कमज़ोर क्यों है?
हमारा लोकतंत्र कितनी दयनीय हालत में है, जनता अपने दायित्वों के प्रति कितनी अधिक लापरवाह या कितनी कम जागरूक है और राजनीतिक दल इसका किस कदर नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको फेसबुक वॉल पर किए गए दो छोटे-छोटे सर्वेक्षण नतीजों से लग जाएगा।
पहले सर्वेक्षण में हमने पूछा था- ‘चुनाव में आप क्या देखकर वोट देंगे? पार्टी या उम्मीदवार?’ 59 प्रतिशत लोगों ने कहा- पार्टी। 41 प्रतिशत लोगों ने कहा- उम्मीदवार। यानी हमारी पसंदीदा राजनीतिक पार्टियां चाहे किसी चोर को टिकट दें या डकैत को या अपराधी या भ्रष्टाचारी को, हममें से 59 प्रतिशत लोग उसे बेहिचक वोट डाल देंगे।
अब दूसरा सर्वेक्षण देखिए। इसमें हमने पूछा था- ‘अगर आपकी पसंदीदा पार्टी ने आपके हिसाब से सही उम्मीदवार न दिया हो, तो आप क्या करेंगे? पार्टी को वोट दे देंगे या नोटा दबाएंगे?’ 70 प्रतिशत लोगों ने कहा- पार्टी को वोट दे देंगे। केवल 30 प्रतिशत लोगों ने कहा- नोटा दबाएंगे। यानी यहां भी स्पष्ट है कि उम्मीदवार हमें पसंद नहीं है, वह चोर हो सकता है, डकैत हो सकता है, अपराधी या भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, लेकिन हममें से 70 प्रतिशत लोग उसे वोट दे देंगे।
समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर क्यों राजनीतिक दल अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को टिकट देने से परहेज नहीं करते हैं। क्यों बिहार में एक गठबंधन ने किसी बलात्कारी की बीवी को टिकट दे दिया, तो दूसरे गठबंधन ने किसी बाहुबली की बीवी और भाई दोनों को टिकट दे दिया। यह तो परोक्ष तरीके से राजनीति में अपराधीकरण का सम्मान हुआ, लेकिन कई राजनीतिक दलों को सीधे-सीधे अपराधियों को भी टिकट देने से गुरेज नहीं है।
जाहिर है कि राजनीति में शुचिता और संसद व विधानसभाओं की स्वच्छता किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे पर नहीं हैं। सवाल है कि जब जनता की तरफ से राजनीतिक दलों पर कोई लोकतांत्रिक दबाव है ही नहीं, तो राजनीतिक दल क्यों न लोकतंत्र की छाती पर धनबल, तनबल और गनबल से तांडव खेलें?
मेरी राय में हम इस लोकतंत्र में उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं, जो कि इसे दिन-ब-दिन गर्त में ही ले जाएगी। आज हम पहले पार्टी देखते हैं, फिर उम्मीदवार देखते हैं या उम्मीदवार देखते ही नहीं हैं। जबकि किसी भी चुनाव में हमें सबसे पहले उम्मीदवार देखना चाहिए, फिर पार्टी देखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि देश की 543 लोकसभा सीटों में से आप चाहे जिस भी सीट पर मतदाता हैं, सबसे पहले उम्मीदवार देखिए। देखिए कि कौन-सा उम्मीदवार आपको सबसे अच्छा लगता है। फिर चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल के टिकट पर खड़ा है, उसे वोट दे दीजिए। और यदि आपको लगे कि किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन से कोई भी ऐसा उम्मीदवार खड़ा नहीं है, जो आपके पैमाने पर अच्छा कहा जा सके, तो आप बेहिचक नोटा दबाइए।
नोटा की ताकत को कम करके आंकने या हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका वोट किसी को जिताने में काम न भी आ सके, लेकिन आपकी अंतरात्मा पर यह बोझ तो नहीं रहेगा कि आपने भी एक गलत उम्मीदवार को चुनकर लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का पाप किया है। साथ ही, अगर आप अच्छे उम्मीदवार न दिए जाने की स्थिति में नोटा दबाना शुरू कर देंगे, तो आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों पर अच्छे उम्मीदवार देने का दबाव बनेगा।
एक बात हमेशा याद रखें कि लोगों का समूह ही किसी भी राजनीतिक दल का निर्माण करता है। इसलिए, राजनीति में अच्छे लोगों को भेजिए। उनका रास्ता मत रोकिए। उनका मखौल मत उड़ाइए। चाहे आपकी नजऱ में कोई बुरी से बुरी पार्टी क्यों न हो, अगर उसमें अच्छे लोगों की बहुलता हो जाएगी, तो वह बुरी पार्टी भी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह, चाहे कोई पार्टी आपकी नजऱ में कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसमें बुरे लोगों की बहुलता हो जाएगी, तो उसे भी बुरा बनने में वक्त नहीं लगेगा।
बड़े नामों का टिकट काटने में भाजपा नहीं कर रही परहेज
भाजपा खेमा जीत के लिए अपने सभी पत्ते फेंटने में लगा है। बड़े बड़े धुरंधरों के टिकट काटने में भाजपा पीछे नहीं है। गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी का टिकट काट दिया गया है। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी बाहर हुये हैं। आगरा से रामशंकर कथेरिया का टिकट काटा है तो शाहजहांपुर से कृषि राज्यमंत्री कृष्णाराज का। यह सब बड़े नाम हैं जिनकी नाराजगी भाजपा पर भारी भी पड़ सकती है। 2019 का चुनावी युद्ध अब अपने उरूज़ पर है। मतदान की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब पार्टियों का पूरा फोकस टिकट वितरण पर लगा हुआ है। सभी राजनीतिक दलों में इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। खासकर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन होने के बाद सभी दलों के लिए टिकट तय करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनता दिख रहा है। विपक्षी एकजुटता के सामने भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक नई रणनीति पर विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा के 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों के टिकट कटने की उम्मीद है। मौजूदा 5 सांसदों सहित एक केंद्रीय मंत्री का टिकट काटा जा चुका है।
अभी आगे और भी टिकट काटे जाने की सम्भावना है। दिलचस्प बात इसके पीछे की बड़ी वजह है। भाजपा ने कई सर्वे कराए हैं, जिनमें यह बात सामने आई है कि मोदी लहर में जीते ज्यादातर सांसदों के खिलाफ जनता में काफी विरोध है। यानी लोग अपने सांसद को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर लगभग यह सहमति बन गई है कि जिस सांसद का कामकाज संतोषजनक नहीं रहा है या फिर जो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है, उसे दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सांसद ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसमें आरक्षित सीटों के सांसद ज़्यादा हैं। शाहजहांपुर से केंद्रीय कृषिराज्य मंत्री कृष्णाराज, हरदोई से अंशुल वर्मा, मिश्रिख से अंजुबाला सहित चार लोगों के सुरक्षित सीट से टिकट काटे जा चुके हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के सर्वे कराए हैं। नमो ऐप पर कराए गए सर्वे के अलावा आरएसएस ने अपनी तरफ से सर्वे किए हैं। जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास भी ज्यादातर सांसदों के फीडबैक अलग से भेजे गए हैं। इसके अलावा कुछ एजेंसियों ने भी बीजेपी के लिए सर्वे किए हैं।
अनिल मिश्र
(लेखक पत्रकार हैं )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
कांग्रेस के अपमान का बदला लेने को प्रियंका ने झौंकी ताकत
उत्तर प्रदेश में भाजपा का रथ रोकने के लिए जब सपा बसपा एक हुये तो उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल न करके एक तरह से अपमानित किया। 2017 में कांग्रेस और सपा गठबंधन के फ्लॉप होने के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अछूत मानने लगे थे। कांग्रेस से गठबंधन न करने में मायावती का अडिय़ल रुख ज़्यादा बड़ा बना हुआ था पर जब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे किया, प्रियंका ने मंदिर दर्शन प्रारम्भ किए तो गुजरात चुनाव के दौरान राहुल के मंदिर दर्शन का परिदृश्य सामने आ गया। यदि थोड़ा पीछे लौटें तो 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की चमत्कारी सफलता से मात्र 47 व 18 सीट जीत सके मुख्य राजनैतिक दल सपा-बसपा को यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि अलग अलग लड़कर भाजपा को हराना बेहद मुश्किल है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो से पुरानी कड़वी यादों को भूलते हुए भाजपा को हराने के लिए साथ आने का प्रस्ताव दिया। दो लगातार चुनावों में पराजय से पार्टी के अस्तित्व पर रूबरू हो रही मायावती ने पुरानी कड़वी यादों को भूलकर सपा के साथ आने में ही भलाई समझ इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी। इस गठबंधन ने एक बार फिर साबित किया कि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता है। जाति व मजहबी बेडिय़ों में जकड़े भारत के सबसे बड़े सूबे के दो प्रमुख धुर विरोधी दलों का गठबंधन सामाजिक रूप से बेहद सशक्त था। 2014 में सपा बसपा ने 22 व 20 प्रतिशत के लगभग वोट पाया था। उपचुनाव को इसके लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था। इस लिटमस टेस्ट में गठबंधन पास हुआ और उसने सारे उपचुनाव जीत लिए।
इसी दिशा में बढ़ते हुए गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीट को 37, 37, 3 करके आपस में बांट लिया। कांग्रेस का वोट बैंक प्रदेश में लगभग 7 प्रतिशत है और वह मुख्यत: सामान्य वर्ग का है। गठबंधन से असंतुष्ट लोग विकल्पहीनता की दिशा में भाजपा को वोट न कर सके इसलिए कांग्रेस को रणनीति के तहत गठबंधन से अलग रखा गया। यहां तक प्रकरण सही दिख रहा था। इसके बाद जो हुआ वह ज़्यादा रोचक था। क्षेत्रीय दलों द्वारा उचित सीटें न दिये जाने से अपमानित महसूस कर रही कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारकर प्रदेश में खोई हुई कांग्रेस की जमीन वापिस पाने व अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए अपना संपर्क अभियान प्रारम्भ कर दिया। प्रियंका गठबंधन के साथ ही भाजपा के हिन्दुत्व के एजेंडे पर प्रहार करने लगी। जिससे अब कांग्रेस के प्रति वोटर का रुझान दिखने लगा है। जबकि एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस की मजबूती गठबंधन के लिये हानिकारक रहेगी। इसके साथ ही सपा की पारिवारिक कलह की वजह से अलग दल बनाने पर मजबूर हुए शिवपाल यादव ने कम समय में प्रदेश में संगठन खड़ा किया। पीस पार्टी से गठबंधन कर मजबूती से चुनावी समर में उतरने का संदेश दिया तो वह भी सपा के परंपरागत वोट बैंक को काफी नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो के अस्थिर चरित्र व टिकट वितरण में प्रचलित तरीका अपनाये जाने से एवं जिन जिलों में सपा के प्रत्याशी नहीं है वहां पर शिवपाल की सक्रियता गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेरती दिख रही है। यह चुनाव अखिलेश यादव व उनकी सपा के राजनीतिक भविष्य के लिये बेहद महत्वपूर्ण है साथ ही यह चुनाव अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता के साथ ही तय करेगा कि क्या प्रदेश में अजीत सिंह की रालोद की तरह अखिलेश यादव की सपा कि भी दुर्गति होने वाली है?
नितिन कुमार
(लेखक उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकार हैं। )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
गांधी परिवार की डिस्कवरी ऑफ इंडिया
चौथी पीढ़ी आ गयी लेकिन नेहरु गांधी वंश का डिस्कवरी ऑफ इंडिया खत्म नहीं हो रहा। आप यह भी कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत का सबसे लंबा चलनेवाला पोलिटिकल सीरियल है। पीढ़ी दर पीढ़ी नेहरु गांधी वंश इंडिया को डिस्कवर करने में लगा है। पहले नेहरु जी ने इंडिया की खोज की, फिर इंदिरा गांधी ने, फिर राजीव गांधी ने और अब भाई बहन भारत की खोज पर निकले हैं। इंदिरा गांधी को छोड़ दें तो राजीव गांधी और अब उनके दोनों वारिस डिस्कवरी भी नहीं कर रहे, एडवेन्चर टूरिज्म कर रहे हैं। सालों साल राजभवन के गुप्त कमरों में पलने-बढऩे वाले राजकुमार और राजकुमारी प्रजा के सामने उतना ही दिखते हैं जितना दरबारी निर्धारित करते हैं। उतना ही पब्लिक लाइफ जीते हैं जितने से प्रजा को राजा की अहमियत का अंदाजा रहे। प्रजा ज्यादा करीब आने लगती है तो अचानक पर्दे से ओझल कर दिये जाते हैं। फिर तब प्रकट होते हैं जब दरबार को जरूरत महसूस होती है।
एडवेन्चर टूरिज्म की शुरुआत राजकुमार ने की। करीब पंद्रह साल के एडवेन्चर टूरिज्म के बाद भी राजकुमार को ये समझ नहीं आया है कि आलू पेड़ पर उगता है या जमीन के नीचे। राजकुमार के एडवेन्चर टूरिज्म के बीच कभी कभी राजकुमारी भी एडवेन्चर टूरिज्म पर निकलती हैं। वैसे तो उनका एडवेन्चर टूरिज्म अभी तक रायबरेली और अमेठी तक ही रहा है लेकिन इस बार दायरा बढ़ाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कर दिया गया है। संभवत: राजकुमारी अमेठी रायबरेली के तालाब, नदी, सड़क देखकर बोर हो गयी थीं इसलिए इस बार आमचुनाव से पहले वोट के लिए बोट से गंगा दर्शन कराने का निर्णय लिया गया। राजकुमारी ने इस एडवेन्चर के दौरान कुछ जगहों पर प्रजा से किसी विदेशी सैलानी के अंदाज में संवाद भी किया और प्रजा से उनके देश के बारे में जानकारी भी इक_ा की।
सुना है प्रजा को राजकुमारी ने कुछ दिव्य ज्ञान भी दिया है कि कोई देश है जो खतरे में आ गया है इसलिए उन्हें घर से निकलना पड़ा है, वरना दिल्ली की आलीशान कोठियों, फार्महाउसों और एसपीजी सुरक्षा के बीच वो सुकून से जिन्दगी गुजार रही थीं। निश्चित रूप से दरबारियों की छोटी मालकिन के घर से निकलनेवाले ‘महान त्याग’ को वंशवादी राजनीति के काले इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। भगवान जाने अभी कितनी पीढ़ी तक नेहरू गांधी वंश का यह एडवेन्चर टूरिज्म चलता रहेगा।