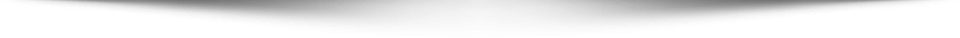न्यायिक व्यवस्था
दरकता विश्वास
क पुरानी प्रचलित कहानी है। दो महिलाएं एक राजा के दरबार में आती हैं। उनके साथ एक छोटा बच्चा होता है। दोनों इस बात पर झगड़ रही हैं कि बच्चे की माँ कौन है? काफी देर तक दोनों अपने तर्क देती रहीं और झगड़ा बढ़ता गया। जब काफी समय बीत गया तो राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा कि बच्चे के दो टुकड़े कर दो और दोनों के बीच में बाँट दो। तब उनमे से एक महिला जोर से चिल्लाई कि ‘ऐसा मत करो। बच्चे को दूसरी महिला को ही दे दो। कम से कम मेरा बच्चा जिदा तो रहेगाÓ। तुरंत न्याय हो गया और साथ ही साथ इस बात का फैसला भी कि बच्चे पर हक किसका होना चाहिए ?
अब इस केस को भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था के अनुरूप देखते हैं। पहले ये केस सेशन कोर्ट में चलेगा। दोनों पीडि़त पक्ष एक-एक वकील करेंगे। कागजात जमा होंगे। शपथ पत्र लिए जाएंगे। इसके बाद महीनों के अंतर पर तारीखे पड़ेंगी। जब तक फैसला होगा वो बच्चा युवा हो जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट मे अपील हो जाएगी। दशकों मुकदमा चलेगा और अब उस बच्चे के भी बच्चे हो जाएंगे और केस चलता रहेगा। फिर फैसला होगा और अब सुप्रीम कोर्ट मे अपील का विकल्प खुल जाएगा। फिर केस वर्षों चलेगा। उस बच्चे के बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे तब कहीं जाकर ये फैसला हो पाएगा कि वो बच्चा किसका बच्चा है। जब केस उच्च न्यायालय मे विचाराधीन होगा उस समय तक दोनों महिलाएं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होंगी। न्यायालय में केस सिर्फ इसलिए आगे चल रहा होता है कि वारिसान संपत्ति कौन होगा। यानि कि फैसला आने तक केस का मोटिव ही बदल चुका होता है। यही अंतर है न्याय और फैसले के बीच।
इसलिए कहा जाता है कि भारत मे विधि का शासन है न्याय का नहीं। उस घटना को अपराध माना जाता है जिसको विधि मे अपराध माना गया है। घटनाओं पर सबूत और तर्कों के आधार पर फैसले होते हैं। फैसले के द्वारा न्याय भी हुआ है या नहीं ? इस पर भारतीय विधि आज तक मौन है? संविधान की व्याख्या न्यायाधीश अपने अपने विवेक से करते हैं। विवेक में अपनी अपनी विचारधारा छुपी होती है। विवेक एवं विचारधाराओं का टकराव ही मूल समस्या की जड़ है। एक अन्य बिन्दु है कि लचर न्यायिक व्यवस्था में न्याय मिलने में देरी राष्ट्रवाद की भावना को कुचल देती है। महत्वपूर्ण केसों में फैसलों की देरी जनमानस और न्यायालय के बीच की दूरी को बढ़ा देती है। कुछ मिसाल देखते हैं। नञ्चसलवाद के विषय में आज महत्वपूर्ण एवं विचारणीय तथ्य यह है कि इस समस्या के मूल तत्व को विकास से जोड़कर देखा जाना चाहिए या कानून एवं व्यवस्था से। पूर्व मे भोपाल कांड हुआ था। फैसला आने मे 26 साल लगे किन्तु इतने बड़े कांड मे गुनहगार को सजा 26 माह की भी नहीं हुई। मुख्य आरोपी एंडरसन एक दिन भी जेल मे नहीं रहा। फिल्म अभिनेता सलमान खान पर फैसला आया। सलमान को पाँच साल की सजा हुई किन्तु उसी दिन दो दिन के लिये अन्तरिम जमानत एवं इसके बाद उच्च न्यायालय से नियमित जमानत भी मिल गयी। भारत मे भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। आय से अधिक संपत्ति के मामले मे स्व0 जयाललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। इसके पहले निचली अदालत से जयललिता को चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत से सजा पाने की प्रक्रिया पूरा होने मे 18 साल लगे और उच्च न्यायालय से सजा खत्म होने में सिर्फ आठ माह का समय लगा। फैसले और न्याय मे अंतर को दर्शाने के लिए अरुणा शानबाग केस का जिक्र बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अपराधी को सात साल की सजा मिली। बलात्कार पीडि़ता अरुणा शानबाग 42 साल कोमा में रही। मानवता को झकझोरने वाला यह वीभत्स कांड हम सबको लज्जित कर गया था। निर्भया कांड का मुख्य आरोपी नाबालिग होने के कारण बड़ी सजा से बच गया। क्या हम अरुणा शानबाग एवं निर्भया को न्याय दे पाये ?
यदि तकनीकी पक्ष देखेंगे तो न्यायिक फैसले गलत नहीं कहे जा सकते हैं किन्तु इनके द्वारा संदेश सही नहीं जा पाया। न्यायपालिका के फैसले अगर नजीर बनते हैं तो समाज पर इसका प्रभाव व्यापक होता है। प्राचीन काल में हत्या, बलात्कार, चोरी आदि करने पर तत्कालीन न्याय व्यवस्था त्वरित एवं कठोर निर्णय लेती थी। कोड़े मारे जाते थे। सार्वजनिक सजाएँ होती थी। इससे अपराधी के मन में डर पैदा होता था। अन्य लोगों को मिसाल मिलती थी कि अपराध करने का क्या परिणाम झेलना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं है। आज सजा पाये अपराधियों के लिये मानवाधिकार नाम का झुनझुना इतना बजाया जाता है कि पीडि़त परेशान हो जाता है। अपराधी झुनझुने की तान पर मस्त नाचता रहता है। इन सबके बावजूद आज भी भारत का आम नागरिक अदालत को न्याय का मंदिर मानता है। हर तरफ से उसकी आस जब टूटती है तब वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। चारों न्यायाधीशों की प्रेस कान्फ्रेंस ने आम आदमी की उस आस को भीतर तक झकझोर दिया है।
चार न्यायाधीश द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस प्रकरण
जिस तरह से देश की शीर्ष अदालत के चार बड़े न्यायाधीशों ने सार्वजनिक रूप से अपनी बात कही। वह न्यायपालिका के लिए एक काला दिन रहा। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तीनों अभिकरण कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका में सिर्फ न्यायपालिका ही एक ऐसा अभिकरण है जिस पर तमाम आरोपों के बावजूद आज भी जनता का विश्वास बरकरार है। इस प्रकरण से जनता में यह संदेश गया है कि उच्चतम न्यायालय में कोई बड़ी गड़बड़ी मौजूद है। अब जनता उच्चतम न्यायालय के हर फैसले को संदेह की निगाह से देखेगी। न्यायालय की यह गिरी गरिमा को संभालने में न्यायालय कामयाब हो जाएगा ऐसा भी फिलहाल नहीं दिखता है।
इस कान्फ्रेंस के परिदृश्य में देखें तो इसके तार लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े दिखते हैं। मेडिकल कालेज बनाने का अर्थ होता है कि कम से कम तीन चार सौ करोड़ का निवेश। इन चार न्यायाधीशों का आरोप है कि मुख्य न्यायाधीश ने इस मसले सहित अन्य महत्वपूर्ण वाद अपनी मनपसंद पीठों को दिये। चूंकि, मुख्य न्यायाधीश के पास विशेषाधिकार होता है कि वह कोई भी वाद किसी भी पीठ को भेज सकता है इसलिए किसी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। चारों न्यायाधीशों का मानना था कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश सिर्फ बराबरी वालों में पहले हैं इसलिए वह रोस्टर के अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। रोस्टर एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी वाद को किसी पीठ के पास भेजने का विशेषाधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। इसके साथ ही न्यायालय से जुड़ा व्यक्ति इस बात को समझता है कि न्यायालय में एक स्थापित परंपरा यह भी है कि एक जैसी प्रकृति के विषय उस पीठ को भेजे जाते हैं जो उस तरह के वादों का निपटारा करती रही होती है।
अब यह चारों न्यायाधीश क्यों उन मसलों में अपने हस्तक्षेप चाहते थे जो मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें नहीं दिये इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। इन चारों न्यायाधीशों द्वारा दिसंबर 2014 में जस्टिस लोया की मौत का प्रकरण भी उठाया गया। जस्टिस लोया गुजरात के सोहराबूद्दीन मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी एक आरोपी थे। उनकी मौत के समय उनका उनके साथी न्यायाधीशों के मौजूदगी में उपचार हुआ था किन्तु उनकी मृत्यु हो गयी थी। उनका पोस्टमोर्टम भी हुआ था किन्तु उस समय उनकी मौत पर कोई राजनैतिक विवाद नहीं बना। अभी कुछ माह पहले गुजरात में हुये चुनावों के दौरान एक शिगूफा छोड़ा गया कि जस्टिस लोया की मृत्यु संदिग्ध थी। अमित शाह का नाम जुड़ा होने के कारण यह विषय तूल पकड़ गया। जस्टिस लोया के बेटे ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुये संदिग्ध थियरी को नकार दिया। इसके बावजूद खबरों के आधार पर 09 जनवरी 2018 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में जस्टिस लोया की मौत पर एक याचिका डाल दी गयी। वहाँ सुनवाई शुरू हो गयी है। इसके बाद एक याचिका उच्चतम न्यायालय में भी डाली गयी। जिस दिन चारों न्यायाधीश प्रेस कान्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन इस याचिका पर भी सुनवाई चल रही थी और उन्होने इस प्रकरण को भी उठाया।
न्यायपालिका प्रकरण से लोकतन्त्र को कोई खतरा नहीं:
जब चारों न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्हानें न सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के रोस्टर के विशेषाधिकार को चुनौती दी बल्कि इसे लोकतन्त्र के लिए खतरा भी बताया। ये न्यायाधीश न्यायिक सक्रियता के माध्यम से होने वाले निर्णयों पर टिप्पणी दे रहे थे। जनहित याचिकाओं के निर्णय इनके निशाने पर थे। पर तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जब एक तरफ यह न्यायाधीश यह मान रहे हैं कि सभी न्यायाधीश बराबर हैं और मुख्य न्यायाधीश सिर्फ बराबरी वालों में पहले हैं। तो जिन न्यायाधीशों के द्वारा फैसले दिये गए हैं वह कैसे इन न्यायाधीशों से जूनियर माने जा सकते हैं। क्या फैसलों पर सवाल उठाना उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है? सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण एवं मलाईदार केसों के आवंटित होने की प्रक्रिया से लोकतन्त्र कैसे खतरे में आ सकता है?
न्यायिक भ्रष्टाचार को लोकतन्त्र से जोड़ कर देखना शायद उचित नहीं है। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की अनदेखी तो उच्चतम न्यायालय ने 1993 में कालेजियम व्यवस्था के द्वारा ही कर दी थी। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनु0-124 एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनु0-217 के अंतर्गत किए जाने का प्रावधान था। इस व्यवस्था में नियुक्ति में सरकार का भी हस्तक्षेप रहता था। 1993 में यह व्यवस्था बदल दी गयी। न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के हाथ में चली गईं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कुछ सौ परिवारों के इर्द गिर्द ही न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सिमट गयी। न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पारदर्शिता खत्म हो गयी। 2014 में जब सरकार ने इस व्यवस्था को भंग करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा नियुक्ति का कानून बनाया तो उच्चतम न्यायालय ने खुद उस कानून के खिलाफ निर्णय देकर कानून को निरस्त कर दिया। यह पहला ऐसा मसला था जिसमे उच्चतम न्यायालय स्वयं एक पार्टी भी था और फैसला भी दे रहा था। हालांकि, इस फैसले के द्वारा न्यायालय ने कालेजियम व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया था। बावजूद इसके प्रक्रियागत व्यवधान आते चले गए। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होती चली गयी। अभी तक कोई सर्वमान्य निर्णय नियुक्ति प्रक्रिया पर नहीं लिया जा सका है।
कालेजियम प्रक्रिया में तो इतनी खामियां हैं कि कई वरिष्ठ जिला न्यायाधीशों को दरकिनार करके उनसे जूनियर को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता है। इससे न्याय की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि निचली अदालतों में मजिस्ट्रेट बनने के लिए पीसीएस-जे एवं अपर न्यायाधीश बनने के लिए एचजेएस की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है किन्तु उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी परीक्षा को पास करने की आवश्यकता नहीं है। कालेजियम के द्वारा नियुक्तियाँ कर दी जाती हैं जिस पर भाई भतीजावाद का आरोप लगते रहते हैं। 1975 में चयन के लिए एक केंद्रीयकृत व्यवस्था भारतीय न्यायिक सेवा के द्वारा चयन का प्रावधान किया गया था किन्तु आज तक ऐसा करना संभव नहीं हो पाया है।
अब इन चारों न्यायाधीशों के उस बयान को देखते हैं जिसमें वह लोकतन्त्र को खतरा बता रहे थे। यह चारों न्यायाधीश उसी कालेजियम व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसके द्वारा नियुक्तियाँ होती हैं। इस कालेजियम व्यवस्था में जब विधायिका का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है तो कैसे लोकतन्त्र खतरे में आ सकता है? अगर न्यायाधीशों के बीच आपसी मतभेद हैं तो इसको लोकतन्त्र से जोड़ कर क्यों दिखाया जा रहा है? जब न्यायाधीश किसी भी विषय का मीडिया ट्राइल होने पर नाक भौ सिकोड़ते हैं तो क्यों उच्चतम न्यायालय के अंदरुनी मामलों को मीडिया के सामने ला रहे थे। क्या ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हैं? जब न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर उनके विशेषाधिकारों में किसी बाहरी का हस्तक्षेप ही नहीं हैं तो इन चारों को अंदरुनी मतभेद घर के भीतर ही सुलझाने चाहिए थे। पहले यह न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश पर उंगली उठाएँ और फिर उसके बाद यह भी चाहें कि मुख्य न्यायाधीश ही उनकी समस्या सुलझाएँ? दोनों ही बातों में जबरदस्त विरोधाभास दिखता है। इसके बावजूद मुख्य न्यायाधीश और इन चारों न्यायाधीशों के मध्य बातचीत की प्रक्रिया हुयी। रोस्टर सिस्टम पर चर्चा हुयी और रोस्टर व्यवस्था पर इन चारों न्यायाधीशों एवं अन्य सुझावों पर मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लिया। यह समस्या समाधान का निर्णायक कदम था क्योंकि इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस मसले में न जनता हस्तक्षेप कर सकती है न मीडिया और न ही सरकार। आरोप भी न्यायपालिका के अंदर से आए थे। और समाधान भी भीतर से होना था।
प्रकरण में राजनैतिक हस्तक्षेप रहा दुर्भाग्यपूर्ण
कभी भी कहीं भी कोई भी मसला हो। राजनैतिक लोग अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आते हैं। राजनैतिक हस्तक्षेप के बाद गंभीर एवं विचारणीय प्रश्न हल्के बन जाते हैं। इस प्रकरण को पहला राजनैतिक रंग तब मिला जब प्रेस कान्फ्रेंस के ठीक बाद भाकपा नेता डी राजा ने जस्टिस चेलमेश्वर से मुलाकात की। जस्टिस चेलमेश्वर इस प्रेस कान्फ्रेंस के मुख्य कर्ताधर्ता थे। उनके आवास पर एक कम्युनिस्ट नेता का आना कई सवाल खड़े कर गया। प्रधानमंत्री मोदी एवं भाजपा के द्वारा इस प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। क्षेत्रीय दलों द्वारा सांकेतिक विरोध किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा उसी दिन शाम को एक प्रेस कान्फ्रेंस कर दी गयी। हालांकि, चार न्यायाधीशों की बात पर राहुल गांधी की चिंता को वाजिब माना भी जा सकता है किन्तु उन्होंने जस्टिस लोया के मुद्दे को भी उठा दिया। उस मुद्दे को जिस पर पहले से उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। जिस प्रकरण को स्वयं जस्टिस लोया के बेटे संदिग्ध मानने से मना कर चुके थे। जस्टिस लोया के मामले की याचिका कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला ने दायर कर रखी है इसलिए इस विषय पर राहुल गांधी की भूमिका समझ आती है। क्या गैर जरूरी टिप्पणी करके राहुल गांधी ने सिर्फ अनावश्यक राजनीति नहीं की? बेहतर होता कि वह न्यायालय के इस विवाद पर न्यायालय को अंदर सुलझाने की बात कहकर अपनी परिपञ्चवता का परिचय देते।
सिर्फ नैतिकता की अपेक्षा है समस्या का समाधान
न्यायालय पर किसी का दवाब नहीं है। महाभियोग के द्वारा आज तक किसी न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सका है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसकी जटिलता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। 1993 में जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया संसद में पूरी हुयी किन्तु तब कांग्रेस ने महाभियोग के विरोध में अपना मत देकर उन्हें बचा लिया। 2008 में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सौमित्र सेन पर महाभियोग की सिफारिश की गयी। उन्होने महाभियोग के पहले ही इस्तीफा दे दिया। 2008 में गाजियाबाद जिला न्यायाधीश रमा जैन ने 82 लोगों के खिलाफ गाजियाबाद कोषागार से गैर कानूनी रकम निकालने के आरोप में एफआईआर करने का आदेश दिया। जब जांच आगे बढ़ी तब मालूम हुआ कि इस रकम से 36 जज लाभान्वित हुये थे जिसमे से एक उच्चतम न्यायालय से, ग्यारह इलाहाबाद एवं उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं 24 उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिला न्यायालयों से संबन्धित थे। इस मामले में पहली बार देश के मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई को इजाजत दी कि वह आरोपी न्यायाधीशों से पूछताछ कर सके। ये कुछ मामले ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि क्यों न्यायाधीश सर्व शक्तिशाली होते हैं और उनको भ्रष्टाचार की किसी कार्यवाही का डर नहीं होता है।
ऐसे में समाधान का रास्ता बचता है नैतिक मूल्य। उच्चतम न्यायालय द्वारा परंपरागत नैतिक मूल्यों के अनुसार न्यायाधीशों की मीडिया से बात करने पर पाबंदी है। ये कोई बाध्यकारी कानून नहीं है पर सर्व स्वीकृति से स्वीकार्य नियम है। 07 मई 1997 को उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने न्यायाधीशों के लिए नैतिक मूल्य (रिइन्सटेंटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडीशियल लाइफ) स्वीकार किए थे। इसके बाद 1999 में मुख्य न्यायाधीश कान्फ्रेंस में इसे पूरी न्यायपालिका के लिए स्वीकृत किया गया। इसमे सौलह बिन्दु हैं। इसमें नवें बिन्दु में यह कहा गया है कि न्यायाधीश अपने फैसलों के जरिये बोलेंगे एवं मीडिया को कोई साक्षात्कार नहीं देंगे। यह कोई कानूनी रोक नहीं थी सिर्फ स्व नियंत्रण की गाइड लाइन थी। चारों न्यायाधीशों ने इसलिए किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं किया किन्तु नैतिकता की एक स्थापित परंपरा तोड़ दी। अब चूंकि, न्यायाधीशों पर न तो महाभियोग की प्रक्रिया आसान है और न ही भ्रष्टाचार रोकथाम का कोई कारगर विकल्प। इसलिए सिर्फ नैतिकता ही एक मात्र माध्यम बचता है जिससे हम न्यायाधीशों से अपेक्षा करें कि वह ठीक से कार्य करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी पद पर स्थापित व्यक्ति की शोभा उसके पद से नहीं बल्कि उस पद पर रहते हुये उसके द्वारा किये गये कार्यों से होती है। पद सुख का माध्यम नही होता है। एक उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व में सिर्फ अधिकारों का इस्तेमाल ही नही, कर्तव्यों का निर्वहन भी शामिल होता है। उत्तरदायित्व, कर्तव्य और अधिकारों का घालमेल इतना जटिल बन जाता है कि नैतिकता इसमें कहीं उलझ कर रह जाती है। नैतिकता की सिर्फ अपेक्षा ही रह जाती है और समाधान अंधेरे में खो जाता है।
क्या भारतीयता आधारित न्याय व्यवस्था पर काम नहीं कर सकते हम ?
हालांकि, प्रश्न हायपोथेटिकल है? किन्तु बेहद आवश्यक है। क्या आज भी हमें मैकाले के कानूनों से देश चलाने की आवश्यकता है ? क्या भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गये तत्व भारतीयता को सही ढंग से परिभाषित कर रहे हैं ? क्या 1872 में बनी भारतीय दंड संहिता हमारी न्याय व्यवस्था पर खरी उतर रही है ? भारतीय दंड संहिता में 25 रुपये की मुर्गी चुराने पर सजा का प्रावधान है किन्तु 25 हजार करोड़ के घोटाले का कोई जिक्र नहीं है। इसकी वजह यह है कि तत्कालीन व्यवस्था में बड़े घोटाले गोरे अंग्रेज करते थे और उस धन को इंग्लैंड ले जाते थे। आज वह घोटाले काले अंग्रेज करते हैं और उस धन को स्विस बैंक में ले जाते हैं। तत्कालीन व्यवस्था में 25 रुपये की मुर्गी भारतीय चुराते थे और उनको सजा का डर दिखाया जाता था। आज भी वही कानून और व्यवस्था लागू है। आज इसमे भारतीयता का समावेश आवश्यक है। समस्या के समाधान को दो शब्दों के अंतर से समझा जा सकता है।
अँग्रेजी में दो शब्द हैं। आर्गुमेंट (तर्क) एवं डिस्कशन(चर्चा)। कुछ लोगों के मध्य किसी बिन्दु पर होने वाली बहस मे ‘तर्कÓ के द्वारा साबित किया जाता है कि कौन सही है ? चर्चा मे हासिल किया जाता है कि क्या सही है ? ये कौन और क्या का अंतर ही समस्याओं का हल खोजने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान व्यवस्था में अदालत की कार्यवाही तर्कों पर आधारित होती हैं। वहाँ ये तय होता है कि दो पक्षों में से किसका पक्ष सही है। वहाँ क्या सही है इस पर बात नहीं होती। भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में प्राचीन काल से ही चर्चा और विमर्श का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। बड़े बड़े मुद्दों पर बुद्धिजीवी शास्त्रार्थ किया करते थे। ग्रामीण स्तर पर भी किसी पेड़ की छाया में चौपालें लगा करती थी। गर्मी की तपती दोपहरी मे समय काटने के लिए लगी ऐसी चौपालों में बड़ी-बड़ी समस्याओं के हल निकाल लिए जाते थे। जमीन से जुड़े दीवानी मुकदमे जो आज पचास साल में भी नहीं सुलझ पाते हैं उस व्यवस्था में दो घंटे में सुलझ जाते थे। गाँव के बुजुर्ग ऐसे विषयों में अघोषित रूप से न्यायाधीश की भूमिका मे आ जाते थे। अनुभवों की कसौटी पर कसे उनके निर्णय स्वत: ही स्वीकार्य हो जाया करते थे। भारत में आवश्यकता है अब ऐसी न्याय प्रणाली की जिसमें आर्गुमेंट के द्वारा आरोप प्रत्यारोप न हों। डिस्कसन के द्वारा समाधान निकले।