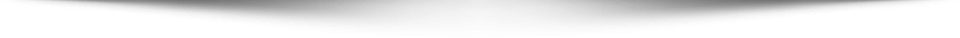दूध का धुला कौन?
पंकज कुमार झा
पनी बात शुरू करूं इससे पहले यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अपने लिए न तो चेलमेश्वर समूह कोई भगवान हैं, और न ही दीपक मिश्रा को ही कोई क्लीन चिट देने का अपना कोई इरादा है। सच कहें तो इस लेख का आशय चार जजों द्वारा उठाये गए मूल प्रकरण पर बात करने से है भी नहीं। हम तो इस अप्रत्याशित घटना के बाद फेसबुक पर छा गए समर्थन-विरोध और उसके तरीके के प्रति बात करना चाह रहे हैं।
हर मुद्दे की तरह इस मामले में भी प्रेस वार्ता होने के पांच मिनट के भीतर-भीतर भाई लोगों ने जिस तरह अपना-अपना पक्ष तय कर अपनी सारी शब्द क्षमताओं को झोंक दिया, वह हंसाता तो है ही लेकिन, उससे ज्यादा सिहरन पैदा करता है कि हम आखिर कैसे समाज का हिस्सा हैं। हर विषय को व्यक्ति विशेष के पक्ष या विरोध का मामला बना देना, और अपने-अपने काल्पनिक पक्ष के लिए ‘मर मिटनाÓ एक ऐसी विडंबना है जिस पर बात किया जाना चाहिए। खैर। अगर आप इस भेड़चाल का हिस्सा नहीं हैं तो जरा गौर कीजिये। देश में कोई भी न्यायिक मामला किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आता है, तो एक सब-इन्स्पेक्टर तय कर लेता है कि आप आरोपी हैं, फिर आप दोषी हैं या नहीं, यह फैसला होने में दशक भर का समय कम से कम लग जाता है लेकिन, यहां जब सुप्रीम कोर्ट के चार-चार कार्यरत जज अपने एक सहयोगी (बॉस नहीं) पर कोई आरोप लगाते हैं, तो कुछ क्षण के भीतर ही हर फेसबुक सेनानी अपनी-अपनी पोजीशन लेकर अपना-अपना हथियार निकाल लेती है, आभासीय दुनिया में ‘युद्धÓ शुरू हो जाता है। कहीं से कोई कथित राष्ट्रवाद का एक सिरा पकड़ कर शुरू हो जाता है तो अन्य वामी गिरोह अपनी डफली से अपना राग निकालना शुरू कर देता है।
यह बड़े शोध का विषय है कि मात्र पांच-दस मिनट में कौन इतने बढ़े समूह को ब्रीफ कर जाता है कि फलाने घटना में फलाना व्यक्ति कथित राष्ट्रवादी है और ढिमकाना व्यक्ति दुसरे पक्ष का! सोशल मीडिया (खास कर फेसबुक) पर चुकी ‘दूसरा पक्षÓ जरा कम प्रभावी है फिर भी, उनके यहां भी यही प्रकिया दुहराते हुए हर घटना पर फेसबुकिया कुरुक्षेत्र सज जाता है। आखिर कौन झटके में यह तय कर लेता है व्यक्ति विशेष की आइडियोलॉजी ञ्चया है, इसे समझना टेड़ी खीर ही है। जरा खुल कर ही कहें तो इसमें जिन पर आरोप लगाया गया है वे दीपक मिश्रा कथित तौर पर राष्ट्रवादी कहे जा रहे हैं और दूसरा पक्ष जाहिर है अन्य वादी। जबकि मूल मामला यह है कि ‘फस्र्ट एमोंग इक्वलÓ मुख्य जज पर आरोप यह है कि वे केस बांटने के अपने अधिकार का दुरूपयोग कर रहे हैं। इस मामले में किसी विचारधारा का कोई लेना-देना हो, ऐसा तो नहीं ही लगता है। आरोप लगाने वाले पक्ष ने प्रेस वार्ता में मोटे तौर पर उड़ीसा के एक मामले का उदाहरण दिया है, जहां से ‘आरोपीÓ मुख्य जज खुद हैं। खैर!
सवाल यह है कि इस विषय पर बात होने के बजाय इसमें कोई राजनीतिक वाद कहां से आ गया? अव्वल तो किसी जज के द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर ‘वादÓ तय कर देना ही शर्मनाक है। यह बात तो सीधे तौर पर समूची न्याय व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करती है। अंतत: इससे यह आशंका मजबूत होती है कि सभी जज अपनी निष्ठा या विचारधारा के आधार पर ही फैसला देते हैं। अगर ऐसा है तो भयावह ही कहा जाएगा इसे। तब तो यह मान लिया जाय कि अब उम्मीद की कोई किरण शेष नहीं है। अंतत: जिसकी लाठी होगी भैंस उसे ही दिला देंगे कथित माय लार्ड लोग भी। ईश्वर करे ऐसा न हो। इतना गलीज नहीं हो गया हो अपना तंत्र, ईश्वर से यही प्रार्थना। फिर भी अगर किसी जज का आचरण आप उसके दिए फैसले से निर्धारित करेंगे, तो कुछ सामने आये तथ्यों पर गौर कीजिये। हालिया ‘विद्रोहÓ के अगुआ जज चेलमेश्वर जिन्हें खलनायक माना जा रहा है, वे अनेक जजों के बीच अकेले ऐसे जज थे जिन्होंने जजों को नियुक्त करने वाली कोलेजियम व्यवस्था का खुल कर विरोध किया था और वे इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाए जाने के पक्षधर हैं। इस मामले में चेलमेश्वर का विरोध इतना तगड़ा है कि वे इससे संबंधित बैठकों का भी बहिष्कार करते रहे हैं।
अगर न्यायिक खबरों पर आपकी नजर रहती हो तो जरूर आप जानते होंगे कि कोलेजियम व्यवस्था ही सरकार और कोर्ट के बीच सबसे बड़ा विवाद है। सरकार इसे पारदर्शी और समावेशी बनाना चाहती है, वर्तमान भाजपा सरकार तो लोकसेवा आयोग की तर्ज पर ‘न्यायिक सेवा आयोगÓ बनाकर उसमें सभी को अवसर देने के पक्ष में है, कोई भी लोकतान्त्रिक व्यक्ति ऐसे आयोग का समर्थन करना चाहेगा। लेकिन सरकार के इस विचार का मुख्य जज समेत ज्यादातर जज विरोध करते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि जस्टिस चेलमेश्वर का रुख इसके उलट है।
तो सवाल उठता है कि सरकार के रुख से इस मामले में सहमति रखने वाले जज अगर अन्य मामले में अलग रुख रखते भी हों तो वे अन्य ‘वादीÓ कैसे मान लिए गए? संदर्भवश यह भी जिक्र करना उचित होगा कि यह चेलमेश्वर ही थे जिन्होंने कपिल सिब्बल की गुंडागर्दी को निरस्त करते हुए आईटी एक्ट की धारा 66-्र को रद्द किया था। अगर वह धारा आज अस्तित्व में होता तो हम में से ज्यादातर फेसबुकिये आज जेल में होते। तब भाजपा के लिए यह एक बड़ा मुद्दा था जिसके पक्ष में इस बागी जज का फैसला आया था। अब आखिर किसने यह तय कर लिया कि ये जज राष्ट्रवाद के खिलाफ हो गए? इसी तरह चार में से अन्य जजों की बात करें। आज केंद्र सरकार का एक बड़ा विषय ‘तीन तलाकÓ का मामला है। इस मामले का राजनीतिक महत्त्व भी कितना ज्यादा है, यह बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बेहतर जानते हैं लेकिन, क्या यह भी जानते हैं आप कि इन्हीं चारों जजों में से एक कुरियन जोसेफ थे जिन्होंने तीन तलाक के खिलाफ फैसला दिया था। (हालांकि जोसेफ ने ही सरकार की किरकिरी भी कराई थी जब किसी इसी पर्व पर केंद्र द्वारा बुलाई बैठक में जाने से मना कर दिया था, वह तब बड़ा मुद्दा बन गया था)।
इन्हीं में से एक जज रंजन गोगोई तो सुप्रीम कोर्ट के ही (विक्षिप्त हो गए) जज रहे मार्कंडेय काटजू को नाक रगडऩे पर विवश किया था। सशरीर एक अपराधी के रूप में जज रहे काटजू को कोर्ट में पेश करने का वाकया शायद ही आप भूले हों। यह संयोग नहीं होगा कि उसके बाद ही मार्कंडेय की बोलती जरा बंद है अभी तक। जाहिर है काटजू सबसे ज्यादा भाजपा को ही काटते थे भों-भों कर। नब्बे प्रतिशत भारतीय को मूर्ख कह कर ‘राष्ट्रवादÓ को भी उसने कमजोर तो किया ही था। । । कहने का आशय बार-बार सिर्फ इतना है कि किसी जज के दिए किसी एक-दो फैसले से आप उनका पक्ष न तौलें और न ही ऐसे मामलों में कूद कर नतीजे पर पहुंच जायें। साथ ही देश के हर मामले को राजनीति या विचारधारा के चश्मे से देखने की कवायद हमारे लिए और तंत्र के लिए भी अंतत: बूमरैंग ही साबित होनी है। और भी गम हैं जमाने में राजनीति के सिवा मेरे भाई। बहरहाल।
मुख्य जज दीपक मिश्रा के साथ जज अरुण मिश्रा आये, प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्रा ने संकट दूर करने की कोशिश की, बार काउन्सिल अध्यक्ष मनन मिश्रा ने विवाद खत्म होने का दावा किया ही। इस तरह अपनी ‘मिश्रितÓ न्यायव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। । । लौटेगी भी। इतने बड़े देश में ऐसे नए-नए और अनोखे संकट आते रहेंगे। राष्ट्र उसका स्वाभाविक समाधान तलाशते रहेगा। तलाश कर ही रहेगा। लेकिन, हम कोशिश करें कि हर मामले में निष्कर्ष तक झट से पहुंच जाने की आतुरता से बचें। हर मामले का विशेषज्ञ भी नहीं बनें। किसी के इशारे पर (या इशारे के बिना भी) दो मिनट में कूद कर हर व्यक्ति के ‘वादÓ का निर्धारण करने नहीं लग जायें, कुछ चीजों के लिए इंतजार भी करना सीखें।
और हां, जन अदालत में जा कर जजों ने सही किया या गलत, यह तो इतिहास भी शायद ही तय करे, पर एक बात जजों के पक्ष में जरूर जाती है कि जब यहां कूएं में ही भांग घुल गयी है, हर बड़े से बड़ा व्यक्ति जब मर्यादा की तिलांजलि कैसे दी जाय इस कवायद में लगा है, तो इसी साल सेवानिवृत्त होने जा रहे इन जजों (एक शायद मुख्य जज बन जायें) पर ही मर्यादा का सारा बोझ क्यूं कर लादें भला? चलने दीजिये चीटें, निकलने दीजिये वादों-मवादों को। पारदर्शिता से मजबूत ही होगा अपना तंत्र, यह उम्मीद करें। हालांकि इस प्रकरण में इन चार जजों को इतना तो श्रेय दे ही सकते हैं कि अंतत: इन्होंने जनता की अदालत को उच्चतम न्यायालय से भी श्रेष्ठ समझा है। फिलहाल इतना भी कम नहीं है।
लेखनी को विराम देने से पहले एक पुरानी कहानी का जिक्र करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। आप भी सुन लीजिये प्लीज। कहानी यूनान की है। वहां के सबसे बड़े जज को रिश्वतखोरी के इल्जाम में मौत की सजा मिली थी। तब शासन की तरह न्याय व्यवस्था भी वंशानुगत ही था (कोलेजियम प्रथा भी कुछ-कुछ वैसी ही है), तो मृत जज के बेटे को ही फिर जज बनाया गया। राजा ने बेटे जज की कुर्सी को बाप जज की मोटी खाल से ही मढ़वाया और नए जज को उसपर बैठाते हुए उसे ताकीद की कि हमेशा याद रखना कि इस कुर्सी को किस तरह सुसज्जित किया गया
है।