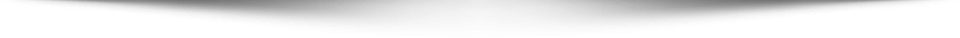नई दिल्ली पुस्तक मेला-2018
मुखर हुआ राष्टï्रवादी विमर्श
द्य सोनाली मिश्रा
हते हैं रंग बदलता है, किताबों का, मेलों का और रंग बदलता है हवाओं का, विमर्शों का। क्योंकि हर रंग सत्ता को समेटे होता है। वह रंग कुछ भी हो सकता है, वह धारा कोई भी हो सकती है, कभी इधर के चेहरे चमक सकते हैं, तो कभी उधर के। नई दिल्ली में जनवरी में जब पुस्तकों का सबसे बड़ा बाजार सजा, तो राष्ट्रवादी स्वरों की थोड़ी फुसफुसाहट थी। दरअसल यह फुसफुसाहट पिछले वर्ष के पुस्तक मेले में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए विमर्शों के आधार पर हो रही फुसफुसाहट थी। इस सरकार के आने के बाद से ही ऐसे विमर्शों के तेज होने की अपेक्षा थी, पर ऐसा न होने से लोग निराश हो रहे थे। पर जनवरी 2018 में आयोजित पुस्तक मेला राष्ट्रवादी वैचारिक मंथन के प्रेमियों के लिए सुखद आश्चर्य के साथ आया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस वर्ष पुस्तक मेले में राष्ट्रीय साहित्य संगम के तले शब्द उत्सव नाम से विविध विषयों पर पांच राष्ट्रवादी विमर्शों का आयोजन किया।
लेखन में विचार, धार और धारा
विचारों के इस महोत्सव का आरम्भ दिनाक 7 जनवरी 2018 को पुस्तक मेले के दूसरे दिन, लेखन में विचार, धार और धारा विषय पर चर्चा के साथ आरम्भ हुआ। इस चर्चा का आयोजन दिल्ली पत्रकार संघ एवं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने संयुक्त रूप से किया था। इस चर्चा का संचालन दिल्ली पत्रकार संघ के सचिव श्री प्रमोद सैनी ने किया और इस आयोजन में मुख्य वक्ता रहे हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति श्री कुलदीप चन्द्र अग्निहोत्री, पांचजन्य एवं ऑर्गनाइजर के समूह सम्पादक श्री जगदीश उपासने, आईआई एमसी के महानिदेशक श्री केजी सुरेश। इस चर्चा में मूल रूप से चर्चा लेखन और विचार धारा के आसपास रही। इस विषय पर कि क्या विचार के बगैर लेखन किया जा सकता है, श्री जगदीश उपासने जी का स्पष्ट मानना था कि हालांकि निजी विचार आपके काम में परिलक्षित नहीं होने चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। निजी चैनल अपने विचारधारा के अनुसार ही खबरों को संशोधित कर दिखलाते हैं। जो कुछ उनके मन में चलता है, उसे ही वे खबरों का रूप दे देते हैं। उन्होंने विचारधारा के अनुसार खबरों के रूप में भारत में नरेंद्र मोदी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलाए गए अभियान का उदाहरण दिया। सच ही है, कुछ मामलों में मीडिया खबर और विचार में इतना उलझ जाता है कि उसकी विश्वसनीयता पर ही संकट उत्पन्न हो जाता है। आज मीडिया विचार के आधार पर साख और पहचान के संकट से गुजर रहा है। इसी के साथ उनका कहना यह भी रहा कि पत्रकारों ने चूंकि अब विचारों के अनुसार खबरों को प्रस्तुत करना आरम्भ कर दिया है, तो लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया से विचलन होने लगा है। जगदीश उपासनेय का यह कहना कहीं न कहीं पूरी तरह सत्य ही है कि चूंकि अब एजेंडा के साथ खबरें दिखाई जाती हैं, तो लोग अब उस एजेंडे को समझने लगे हैं, वे झांसे में आने के लिए तैयार नहीं होते।
विचारधारा और समाचार पर चर्चा को आगे बढाते हुए श्री केजी सुरेश ने भी आज की पत्रकारिता के आन्दोलनकारी स्वरुप पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज पत्रकार कम आन्दोलनकारी या कार्यकर्ता अधिक हो गए हैं। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि मीडिया को व्यवस्था विरोधी होना चाहिए, उन्होंने कहा कि मीडिया को जन सापेक्ष होना चाहिए। चर्चा में जब यह प्रश्न उठा कि आज पत्रकार उग्रता की भाषा में बात करते हैं तो श्री अग्निहोत्री जी का यह कहना था कि पहले तो पत्रकार को उग्र होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही वह उग्र होता है, वैसे ही पच्चीस प्रतिशत तो वह गलती कर ही देता है। आज समाचारों के नाम पर व्यक्तिगत एजेंडे का ही निर्वाह किया जा रहा है, क्योंकि आज पत्रकारिता पैशन से नहीं टार्गेट से होती है।
टार्गेट को ही इस बार राष्ट्रवादी खेमे ने संज्ञान में रखकर राष्ट्रीय साहित्य संगम के बैनर तले पूरे देश से लगभग 12 के करीब प्रकाशकों ने राष्ट्रवादी साहित्य की पुस्तकों का खजाना पाठकों के सामने खोल दिया था और अंतिम ही दिन पता चल पाया था कि उस पिटारे से निकली हुई किताबों ने व्यावसायिक स्तर पर सफलता के शिखर को छू लिया था।
इस चर्चा में श्रोताओं से भी सवाल का दौर था। सवालों के दौर में डायलॉग इंडिया पत्रिका के समूह सम्पादक श्री अनुज अग्रवाल ने इस प्रश्न को उठाया कि जब एजेंडे से चलने वाली पत्रकारिता हो रही है तो ऐसे में प्रेस काउंसिल क्या कर रही है? या जब सरकार का नियंत्रण मीडिया को नहीं चाहिए तो ऐसे में एजेंडे और पत्रकारिता के घालमेल को किस प्रकार रोका जा सकेगा?
जबाव केजी सुरेश जी ने दिया कि आपके सवाल में ही आपका जबाव है कि प्रेस काउंसिल को और पावर दी जाए। इसी के साथ यह भी बात उठी कि नए पत्रकार कैसे शुरुआत करें।
विमर्श के संग भीड़ ञ्जाी बढ़ रही थी। दिन ढलने लगा था, और अगला दिन नई घटनाओं के साथ प्रतीक्षारत था। हालांकि दिल्ली की जनता पुस्तक मेले के खुमार में थी, मगर एजेंडा से संचालित होने वाली मीडिया एजेंडे को धार देती हुई एक नवोदित नेता को दिल्ली में स्थापित करने के प्रयास में लगी हुई थी। नौ जनवरी को उस नेता ने श्री नरेंद्र मोदी से जबाव मांगने जाना था, मगर उसे यह नहीं पता था कि उसे ही दिल्ली की जनता जबाव देने वाली है।
मेले में आने वाले लोग नौ की आशंका से चिंतित लगे, मगर यह दिल्ली है, जौक की दिल्ली, गालिब की दिल्ली, हर तरह की जिजीविषा से भरी हुई।
इतिहास में मिथक और यथार्थ
शब्द उत्सव में साहित्य-इतिहास में मिथक और यथार्थ पर चर्चा?का आयोजन किया गया था। हालांकि इस वर्ष प्रगति मैदान में चल रहे निर्माण कार्य के कारण स्थान कम रहा और उसके कारण अव्यवस्थाएं भी काफी रहीं, मगर इससे पुस्तक प्रेमियों और विमर्श प्रेमियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। पूरे नौ दिन इस मेले को दिल्ली की जनता का प्यार मिला। शब्द उत्सव में अगले दिन विमर्श में जब साहित्य और मिथक पर चर्चा हुई तब भी श्रोताओं की कमी नहीं थी। दरअसल साहित्य और मिथक हैं ही ऐसे विषय, जिन पर जितनी चर्चा हो उतनी कम। साहित्य जहां जन सापेक्ष के स्थान पर आजकल किसी एजेंडे का वाहक बन गया है और साहित्य एवं मिथक में साहित्य के इसी संकट पर बात की गयी। इस चर्चा का मुख्य हिस्सा रहे प्रो। कपिल कुमार, रजनीश शुक्ल एवं माखन लाल जी। इस सत्र का संचालन करते हुए श्री सौरभ मालवीय ने प्रश्न उठाए कि यदि जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण है, उसी प्रकार इतिहास भी समाज का दर्पण है। इतिहास में कल्पना नहीं होती, जबकि साहित्य कल्पना की जमीन पर रचा जाता है। पर इतने वर्षों से जिस साहित्य का सृजन हो रहा है क्या वह भारत के सन्दर्भ में वाकई दर्पण है? या वह ऐसा दर्पण है जिसमें एक भारतीय समाज अपना चेहरा नहीं देख सकता है? ऐसे कई प्रश्न कई वर्षों से भारतीय जन मानस को उद्वेलित कर रहे हैं। प्रो। कपिल ने कहा कि साहित्य को यदि उसके दर्पण होने पद से अलग किया, तो किसने किया? भारत पर आक्रमण जितना बाहरी हुए, उतना ही उसकी आत्मा पर बौद्धिक आक्रमण भी हुए। विभाजित करने वाली तकनीक को माञ्चर्सवाद ने बढाया। जहां भारतीय दर्शन सर्व धर्म समभाव की भावना को आत्मसात किए हुए हैं, वहीं लेनिन का मानना ही है कि साहित्यकारों का यह फर्ज है कि वे अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्गसंघर्ष को बढाएं, जिससे शोषक और सर्वहारा में यह दुनिया बंटें एवं उसके बाद साम्यवादी राज्य स्थापित हो। भारत के साथ तो यह उस पर आर्यों के बाहरी होने के सिद्धांत के साथ अन्याय आरम्भ हो गया था। इस चर्चा से यह बात निकल कर आई कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रवादी विचारों की तरफ से भी वैकल्पिक लेखन आरम्भ हो। शायद यही कारण है कि उस दिन दो पुस्तकों का विमोचन भी मंच से हुआ, जिसमें एक थी युवा लेखक लोकेन्द्र सिंह की हम असहिष्णु लोग। जिसमें असहिष्णुता के कथित खतरे की साजिश पर विचार हैं।
दिन के समाप्त होते होते, फिर से दिल्ली में कल क्या होगा की आहट हो रही थी। क्या फिर से एक आन्दोलन होगा? पुणे और मुम्बई से उठता काला धुंआ कहीं दिल्ली को अपने आगोश में तो नहीं ले लेगा? मगर यह आशंक निर्मूल हुई। दिल्ली में नौ जनवरी को दिल्ली वालों ने कथित क्रांति का स्थान देने के स्थान पर किताबों की शरण में आना मुनासिब समझा। दिल्ली वालों ने अपनी राह चुन ली थी, कि उन्हें पुस्तकें चाहिए, फिर चाहे उसके लिए कितना भी पैदल न चलना पड़े और उन्हें मीडिया की वह चमक नहीं चाहिए, जो अराजकता की तरफ जाए,शायद तभी पुस्तकों को व्यक्ति का सबसे बड़ा दोस्त कहा गया है।
संदीप देव की पुस्तक राज-योगी का लोकार्पण
कहानी कम्युनिस्टों की नामक किताब से लोकप्रिय हुए लेखक संदीप देव की एक और पुस्तक राज-योगी का भी लोकार्पण इस पुस्तक मेले में हुआ। इस पुस्तक वार्ता में आउटलुक के पूर्व संपादक श्री आलोक मेहता, साध्वी जया भारती और भाजपा के प्रवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय मुख्य अतिथि थे। इसका हिंदी और अंगरेजी लेखन हालांकि एक साथ हुआ है, मगर हिंदी में योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक सफर और राजनीतिक सफर की बात है तो वहीं अंग्रेजी में उन राजनीतिक कुचक्रों की तरफ इशारा है, जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुनियोजित तरीके से चला। इस चर्चा में धर्म को राजनीति से अलग मानने वालों की आलोचना की गयी, क्योंकि भारतीय परम्परा में धर्म राजनीति से अलग हो ही नहीं सकता है। भारत में तो राज दरबार में भी ऋषि मुनियों को स्थान देने की परम्परा थी। और चूंकि योगी के पास अपना कुछ नहीं होता, तो वह एक ऐसा शासन जनता को दे सकता है जो निष्पक्ष है और जो कानून के अनुसार है। लेखक संदीप देव के अनुसार यह किताब योगी जी और नाथ सम्प्रदाय पर है। योगी राज की सफलता पर प्रकाशक ब्लूम्स बेरी भी आश्चर्यचकित थे।
साहित्य और पत्रकारिता, कितने दूर कितने पास
हिंदी साहित्य संगम का अगला कार्यक्रम मेले में दिनांक 12 जनवरी को हुआ। इस चर्चा का साहित्य और पत्रकारिता, कितने दूर कितने पास। साहित्य की समझ एक पत्रकार को संवेदनशील बनाती है और उस वर्ग के प्रति संवेदना की समान भूमि पर लाती है, जिसके लिए वह उत्तरदायी है। प्रेमचंद का रचा हुआ समाज आज भी है, मगर जहां आज कुछ पत्रकारों को धान और गेंहू में अंतर नहीं पता है, वे अपनी रिपोर्ट में धान को बार बार गेंहू कहते हैं, तो ऐसे पत्रकार उस तबके लिए कहाँ से संवेदनशील हो पाएंगे जहां वाकई धान और गेंहू में अंतर होता है। यह सवाल आज लेखन की दो विधाओं के सामने हैं, कि उन्हें आपस में एक दूसरे से कितना लेना है और कितना छोड़ देना है। इस चर्चा में आलोक पौराणिक ने बहुत ही खास बात की कि आज पूरे भारत में तीन प्रकार के भारत हैं, 5 करोड़ लोग अमेरिका हैं, 40 करोड़ लोग मलेशिया और बाकी के 80 करोड़ लोग बांग्लादेश हैं। उन्होनें कहा कि जो अर्थशास्त्र समझते हैं, वे इस वर्गीकरण को समझ जाएंगे। दरअसल आज मीडिया केवल और केवल बाजार और टार्गेट से ही संचालित हो रही है, उनका काम अपना लाभ अधिक से अधिक करना है। जब पौराणिक जी मीडिया के लाभ की चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे में यह सवाल उठना भी उतना ही लाजमी था कि लाभ को ही अपना अंतिम लक्ष्य बनाने वाली मीडिया जब अपने पत्रकार सिद्धांतों के साथ ही सरोकार नहीं रख पा रही है तो वह साहित्य को कहाँ और कैसे स्थान देगी। और इसी बात की पुष्टि जैसे चर्चा में बाद में श्रोतादीर्घा में बैठे दिलीप मंडल ने कर दी। उन्होंने कहा कि जब साहित्य अपने आप में बिकाऊ हो जाएगा तब उसकी चर्चा भी पुस्तकों में होने लगेगी। यदि किसी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उसके लिए तो पत्रिका के तीन क्या चार पन्ने भी दे दिए जाएं, मगर जिसकी केवल तीन या चार सौ प्रतियां भी न बिक पाएं तो ऐसी रचना के लिए पन्ने क्या देना। उन्होनें साहित्य को पूरी तरह से बाजार से ही जोड़ दिया। इसी चर्चा में बस्तर के तमाम मुद्दों पर लिखने वाले लेखक राजीव रंजन भी उपस्थित थे। उन्होंने मीडिया की बेहद चुनिन्दा भूमिका पर बोलते हुए कहा कि आदिवासियों की समस्या की तरफ किसी भी मीडिया का ध्यान नहीं है, वहां पर आदिवासी व्यवस्था और नक्सल दोनों के बीच पिस रहा है। मगर ये खबरें केवल स्थानीय स्तर पर ही रह जाती हैं, दिल्ली तक नहीं आ पातीं।
शायद दिल्ली तक आने के लिए जिस आधार या बाजार की जरूरत होती है। वह बस्तर के आदिवासियों के बस की बाहर की बात ही होगी। मीडिया जब अपने एजेंडे पर चलती है, तब वह दर्द और तकलीफें भी एजेंडे के दायरे में देखती है, और तभी साहित्य से मीडिया का बैर है क्योंकि साहित्य सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, साहित्य लोक की बात करता है और लोक जेब को गर्म करने को तैयार नहीं है।
वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक अनंत विजय ने भाषा पर बात करते हुए कहा कि आज लेखक भाषा को लेकर असावधान है, वह शब्दों के चयन के प्रति गंभीर नहीं है।
अनंत विजय शायद नई वाली हिंदी की बात कर रहे थे। नई वाली हिंदी, अर्थात ऐसी हिंदी जिसमें हिंदी भी है और अंग्रेजी भी। वह हिंदी जिसमें आज के कूल ड्यूड की भाषा है। मगर क्या ऐसी हिंदी अधिक समय तक चल पाएगी? और यह नई वाली हिंदी ही ऐसी हिंदी है जिसमें लिखी गयी किताबें जागरण के बेस्ट सेलर में रहती हैं। क्या अब हमें प्रेमचंद की संवेदनशीलता के स्थान पर आने वाले समय में दिल्ली आदि में इस्तेमाल हो रही या गंदी बात जैसी हिंदी की किताबें पढने को मिलेंगी? प्रश्न यह भी है कि इस प्रकार बेस्ट सेलर की सूचियों को लाकर कहीं जागरण भी तो ऐसी हिंदी को प्रोत्साहित नहीं कर रहा? सवाल यह भी है कि इस नई हिंदी की मंशा आखिर क्या है? क्या नई हिंदी भी तो किसी एजेंडे के तहत स्थापित नहीं की जा रही है? इस सवाल का जबाव सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली से महेश भारद्वाज हंस कर देते हैं कि ऐसी चर्चाएँ आज पहली बार तो नहीं हो रही हैं, दरअसल ऐसी चर्चाएँ हमेशा होती रही हैं और होती रहेंगी। आत भी लोग अच्छा साहित्य पढऩा चाहते हैं, अच्छी और मर्यादित भाषा पढऩा चाहते हैं। आज भी प्रेमचंद बिक रहे हैं, आज भी नरेंद्र कोहली बिक रहे हैं। चित्रा मुद्गल की किताबें आज भी उतना ही बिक रही हैं, जितना पहले बिकती थीं, बल्कि आज तो और और भी ज्यादा बिक रही हैं। उन्होंने कहा कि यह दौर भी जल्द खत्म हो जाएगा। और उनके इसी विश्वास की पुष्टि वे बड़े बड़े थैले कर रहे थे, जो लोग राजकमल और वाणी प्रकाशन से विद्यार्थी या कहें युवा लेकर निकल रहे थे। वहीं नई वाली हिंदी का परचम लहराने वाले हिन्द युग्म के स्टाल पर भी लेखक और प्रकाशक अपनी हिंदी के साथ हमेशा रहे।
इस नई वाली हिंदी ने हिंदी को मठों की बेडिय़ों से निकाला है और इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदी को न जाने कब तक केवल अकादमी की ही भाषा बना दिया गया। और वही हिंदी जब तक पुस्तक मेले में हावी रही, तब तक हिंदी पाठकों से दूर रही। धीरे धीरे आम बोलचाल वाली हिंदी को अकादमिक हिंदी से भिड़ा कर हिंदी को क्लिष्टता की ऐसी चोटी पर पहुंचा दिया था कि लोग हिंदी को केवल सरकारी भाषा मानने लगे थे। ऐसे में हिंदी इज कूल का नारा देकर नई हिंदी के लेखक ऐसी ताजी हवा के झोंकों की तरह आए, जिन्होनें हिंदी के प्रति आम जनता के मन में प्यार जगाया। मगर इस नई वाली हिंदी ने भाषा को सरल करने के साथ फार्मूला लेखन की बहस को भी जन्म दे दिया। कई लोगों का मानना है कि ये उपन्यास वन सिटिंग में बैठकर पढने वाले उपन्यास हैं और आप इन्हें हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते है। ऐसे में नए प्रकाशक इस विषय में बहुत ही भ्रामक से दिखे कि उन्हें आखिर में साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी है या फार्मूला लेखन करवाना है। नई दिल्ली के यश प्रकाशन से राहुल भारद्वाज का कहना था कि आज न केवल लेखन शैली बदली है, बल्कि बाजार भी बदला है, तो सवाल यही है कि हम गुणवत्ता को बनाए रखकर किस तरह से अच्छी पुस्तकें जनता तक पहुंचा सकते हैं। हमने हमेशा ऐसा किया है और हम ऐसा ही करेंगे। लेखन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। नई दिल्ली से ही आए सस्ता साहित्य मंडल पर भी उपन्यास, बाल साहित्य आदि सभी विधाओं की पुस्तकों पर पाठकों की अच्छी खासी संख्या दिखी।
लोक को नकारे तो कैसा साहित्य
मेला धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रहा था। मेले में अंतिम दिन भी राष्ट्रीय साहित्य संगम के बैनर के तले चर्चा का आयोजन किया गया था। यह चर्चा लोक और साहित्य के परस्पर सम्बन्धों पर आधारित थी। लोक को नकारे तो कैसा साहित्य, में प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव श्री सच्चिदानंद जोशी, आकाशवाणी दिल्ली के निदेशक श्री सोमदत्त शर्मा और इतिहासकार और साहित्यकार डॉ। प्रमोद दुबे एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ। अवनिजेश अवस्थी मुख्य वक्ता के रूप में थे। चर्चा का संचालन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश चतुर्वेदी ने लोक और साहित्य पर बात करते हुए कहा कि एक तरफ तुलसीदास थे जिन्होनें राम को अवधी भाषा अर्थात लोकभाषा में रचकर समाज को एक ऐसी कृति दी है, जिसकी तुलना विश्व के किसी भी साहित्य में कहीं नहीं दिखती है। लोक से ही पीढिय़ाँ ग्रहण करती हैं, मगर कहीं न कहीं आज लोक पीछे है, फार्मूला लेखन आगे है। श्री सोमदत्त शर्मा ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जो साहित्य पहले लोक की पहचान हुआ करता था, वह आज इस तरह फार्मूला लेखन की तरफ क्यों मुड़ गया? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गलत हुआ है? कोई भी साहित्य लोक को नकार कर नहीं लिखा जा सकता है। लोक में रंग है, हर रंग है। लोक में हमारी परम्पराएं हैं। मगर कुछ समय से एक ऐसा साहित्य रचा गया और उससे हटकर कुछ भी लिखने वालों को हेय द्रष्टि से देखा गया, उसने लोक साहित्य का बहुत नुकसान किया है। उन्होंने साहित्यिक छुआछूत का उदाहरण देते हुए कहा कि रामविलास शर्मा ने जब सरस्वती और वेदों पर काम किया तो उन्हें वामपंथियों ने साइडलाइन कर दिया। त्रिलोचन शास्त्री ने चूंकि तुलसीदास को आदर्श माना तो उन्हें वामपंथियों ने कवि माना ही नहीं।
त्रिलोचन को नकारने वाले दरअसल उस लोक को नकारते हुए प्रतीत होते हैं, जो उनके कहे में नहीं चलता। वह लोक जो अभी भी आस्था से भरा है। कबीर और तुलसी दोनों के राम अलग हैं, मगर भारत का लोक दोनों ही राम को अपनी आस्था का विषय बना लेता है और यही इस लोक की खासियत है।
डॉ. अवस्थी ने तुलसी और कबीर की व्यर्थ की तुलना पर अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। कबीर कबीर हैं, तुलसी तुलसी। ऐसे में कैसे कोई किसी से श्रेष्ठ हो सकता है। कबीर को प्रतिष्ठित कर तुलसी को नीचा दिखाने के सुनियोजित प्रयास किए गए, जो अभी तक चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज रचना उत्पाद बन गयी है, वह लोक से अलग होकर केवल दिमाग का विषय बन गयी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय होने के लिए स्थानीय होना सबसे अधिक जरूरी है। इसी चर्चा में आगे इसी विषय पर डॉ। प्रमोद कुमार ने कहा कि कबीर और तुलसी में कोई अंतर है ही नहीं। यह भ्रमित करने का प्रयास है। लोक और वेद दोनों को उन्होंने बिम्ब और प्रतिबिम्ब बताया। उन्होंने कहा कि लोकाचार तो बदल सकता है, वेदाचार नहीं। मालिनी अवस्थी ने लोक को साहित्य का अनिवार्य हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जो भी आसपास घटित हो रहा है वह सब लोक है। लोक से यदि आप नहीं कुछ ले रहे हैं, तो यह लोक की नहीं आपकी दरिद्रता है। राम साधारण होकर असाधारण हैं, यही लोक है। मगर भारत में लोक को नीची द्रष्टि से देखने का जो द्रष्टिकोण विकसित हुआ, उसने साहित्य को लोक से दूर कर दिया और यह वैचारिक निधर्नता अरूंधती राय के उस कथन से दिखती है जिसमें उन्होनें मां और शिक्षक की डांट को इस्लामी आतंकवादियों से भी भयानक बता दिया। यह तुलना लोक से जुदा हुआ व्यञ्चित ही कर सकता है। यही बात श्री सच्चिदानंद शास्त्री ने आगे बढ़ाई कि हमारे पर्व धार्मिक कम लोक के अधिक हैं। दरअसल जब से यह प्रवृत्ति विकसित हुई कि कलावा बाँधना भी है मगर उसे बाहर नहीं दिखाना, तब से साहित्य में एक दुराव उत्पन्न हुआ। यह बहुत ही दुखद है। हमें समग्र होना होगा, लोक के साथ चलना होगा।
ऌउक्वमीद है कि आने वाले समय में इस मंच के तले इन विमर्शों का दायरा बढ़ेगा। ठ्ठ