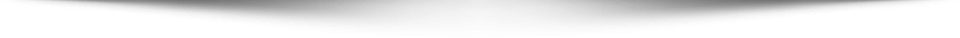उत्तर प्रदेश के फूलपुर एवं गोरखपुर उपचुनाव में हार ने एक तरफ भाजपा की अंदरूनी कलह, अहंकार को सतह पर ला दिया वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के राजनैतिक महत्व को फिर से एक परिदृश्य दे दिया है। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भी भाजपा को शिकस्त मिली है। हिन्दी भाषी प्रदेशों की हार से नवंबर माह में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा के चुनाव कराये जाने की जो रूपरेखा बन रही थी उसे इन चुनाव परिणामों के द्वारा विराम लगता दिख रहा है। पूर्वोत्तर में भाजपा के मजबूत होने से वामदल एवं कांग्रेस का जनाधार अब समाप्ति की ओर खिसकने लगा है। त्रिपुरा एवं मेघालय में भाजपा की सरकार बनने और नागालैंड में सरकार का सहयोगी बनने से भाजपा उत्साहित है। मोदी-शाह-योगी का कारवां अब कर्नाटक फतेह की तरफ बढ़ गया है। योगी के आने से कर्नाटक में हिन्दुत्व चुनावी मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी का मंदिर दर्शन कार्यक्रम फिर शुरू हो गया है। लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा राज्य की कांग्रेस सरकार ने दे दिया है और अब इस पर गेंद केंद्र के पाले में है। बजट में किसान और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़ोर दिया जाना इस बात का इशारा है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों के चुनावी मोड में आ चुकी है। एक ओर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के चौकीदार नरेन्द्र मोदी को रोटोमैक, पीएनबी घोटाले जैसे प्रकरण संदेह के घेरे में ला रहे हैं तो दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। ट्रम्प से दोस्ती, चीन को डोकलाम में कड़ा संदेश, दावोस, आबुधाबी एवं इस्राइल-फ्लिस्तीन का संयुक्त समर्थन मजबूत विदेश नीति का पर्याय बन कर उभरा है। आर्थिक मोर्चे पर 7.2 प्रतिशत की विकास दर के ताज़े आंकड़े ने नोटबंदी और जीएसटी विरोधियों को चुप कर दिया है। सरकार को अब खतरा सिर्फ अपने लोगों से है। शिवसेना, टीडीपी, अकाली एवं अन्य क्षेत्रीय दलों की नाराजगी अब एनडीए को कमजोर कर रही है। भाजपा के अंदर मोदी विरोधी खेमा चुनाव नजदीक आने पर मुंह उठाने में लगा है। इन सबसे पार पाने के लिए भाजपा को अपने कोर मुद्दों की तरफ लौटना पड़ेगा। गौ-हत्या पर केन्द्रीय कानून न बनाने के कारण भाजपा सरकार पर सवालिया निशान है। राम मंदिर एवं 370 पर कुछ उल्लेखनीय सरकार नहीं कर पायी है। कश्मीर में पत्थरबाज़ रिहा कर दिये गए हैं। इन सबके बीच कमजोर विपक्ष में एकता की कमी और चुनावी अभियान में महारत रखने वाली भाजपा के लिये आगामी लोकसभा चुनावों से ज़्यादा विधानसभा चुनाव मुश्किल होने जा रहे हैं। पूरे राजनैतिक परिदृश्य का खाका खींचता एक आलेख ।
अमित त्यागी
र्वोत्तर में जीत की एक बड़ी वजह मोदी के द्वारा पूर्वोत्तर पर दिया जाने वाला विशेष ध्यान रहा है। एक ओर प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के लिए सरकारी खजाने खोल दिये वहीं दूसरी तरफ संगठन और संघ ने पूर्वोत्तर को राजनीति और कर्मक्षेत्र के रूप में अपना लिया। वर्षों से विकास से अवरुद्ध पूर्वोत्तर को मोदी की विकास लहर ने प्रभावित किया और वहां के क्षेत्रीय दल भाजपा से हाथ मिलाने को आतुर होने लगे। पूर्वोत्तर के सात राज्य हमेशा से संघ के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। अब छह राज्यों में भाजपा की सरकारें बन चुकी हैं। सातवें राज्य मिज़ोरम में भी इस वर्ष चुनाव होने हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया गया। वहां विकास की योजनाएं शुरू की गईं। सरकार द्वारा पूर्वोत्तर को अपनी ‘एक्ट एशिया नीति’ की धुरी बनाया गया। पूर्वोत्तर के लिए एक अलग विकास परिषद का गठन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत एवं अमित शाह ने ताबड़तोड़ दौरे किए। संघ से भाजपा में भेजे गए राम माधव को पूर्वोत्तर की कमान दी गयी। जम्मू एवं कश्मीर के बाद राम माधव के लिए यह दूसरी बड़ी परीक्षा थी। सुनील देवधर को त्रिपुरा प्रभार दिया गया।
पूर्वोत्तर के एक अहम जनाधार वाले प्रदेश असम में जीत के बाद भाजपा की रणनीतिक धार और तेज़ हो गयी थी। एक ओर असम और त्रिपुरा में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बड़ी समस्या थी वहीं अन्य राज्यों में आदिवासियों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराना राजनैतिक संरक्षण में प्रमुखता से होता था। चीन से मिल रहीं चुनौतियां और वामपंथियों का गठजोड़ तोडऩा भाजपा एवं संघ के लिए एक बड़ी चुनौती था। सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर का महत्व अखंड भारत की परिकल्पना का अभिन्न विषय रहा है। असम में जीत के बाद भाजपा का पूर्वोत्तर एजेंडा खुल कर सामने आ गया। असम में चुनाव से पहले कांग्रेसी दिग्गज हेमंत बिस्वा शर्मा का भाजपा खेमे में आना असम जीत का आधार बना। इसके बाद इन्हीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने त्रिपुरा में इंडीजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफ़टी) से भाजपा का गठबंधन कराया। भाजपा आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा में अच्छा इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से ताउल्लुक रखते हैं वह त्रिपुरा की कुल आबादी का एक तिहाई है। संघ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधा। भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं पर हमले हुये। जाने गईं। इसके बाद जब टीएमसी के विधायक भाजपा के खेमे में आए तब पूर्वोत्तर में भगवा फहराने का सपना सच होता दिखने लगा।
पूर्वोत्तर जो हमेशा से कांग्रेस और वाम दलों का गढ़ रहा है उसके संदर्भ में भाजपा के कांग्रेसमुक्त भारत के नारे में वाम मुक्त भारत का नारा भी अंतर्निहित माना जा सकता है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में चुनाव उपरांत भाजपा के द्वारा सरकार बनाने से लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा की दावेदारी काफी मजबूत हुयी है। पूर्वोत्तर में जीत का एक बड़ा महत्व है। इस जीत से न सिर्फ पूर्वोत्तर के प्रदेश मुख्यधारा की राजनीति में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं बल्कि वहां की जनता में पिछली सरकारों के प्रति गुस्सा भी दिखा रहे हैं। त्रिपुरा में पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा को सिर्फ 1.5 प्रतिशत मत मिला था। वाम दलों का गढ़ होने के कारण यहां मुख्य राजनैतिक लड़ाई कांग्रेस और वाम दलों में रही है। पिछले दो दशकों से लगातार वाम सरकार होने के कारण उसका विरोध दिख रहा था। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता ने त्रिपुरा में विकल्प कांग्रेस को न चुनकर भाजपा को चुना। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का जनाधार सिमट कर 2 प्रतिशत रह गया। त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य नागालैंड में भी कांग्रेस सिमट गयी। मेघालय में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद भी कांग्रेस बहुमत से दूर रही फिर भी सरकार भाजपा के समर्थन से बनी। त्रिपुरा में हार और केरल में गिरते जनाधार से भारत में वाम दलों के सिमटने की शुरुआत हो चुकी है।
पूर्वोत्तर में जीत के राजनैतिक मायने
पूर्वोत्तर के तीन चुनावों के बाद बनी सरकारों के साथ ही भाजपा एवं उसके सहयोगी संगठनों का देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी पर शासन हो गया है। क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद की राजनीति में किसी राष्ट्रीय दल के लिए यह उत्साहित करने वाला आंकड़ा है। राष्ट्रीय दल कांग्रेस अब सिर्फ तीन चार राज्यों में सिमट गयी है। आगामी चुनावों में कर्नाटक भी उसके हाथ से जाता दिख रहा है। वाम दल अब सिर्फ केरल में सरकार में हैं। पश्चिम बंगाल एक समय वामपंथियों का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। वहां ममता बनर्जी ने वामपंथियों को बहुत बड़ी चोट दी है। उनका अस्तित्व लगभग खत्म सा कर दिया है। बंगाल में ममता और भाजपा राजनैतिक कुश्ती करके वामपंथियों को चिढ़ाते रहते हैं। त्रिपुरा भी वामपंथियों का एक ऐसा ही अभेद किला था जिसे गिराने की सोचना बेमानी लगता था। सरकार की नीतियों एवं बेहतर सांगठनिक तालमेल से यह संभव हो गया। पूर्वोत्तर की जीत के मायने बड़े हैं। भाजपा पर धनबल, सांप्रदायिकता एवं अन्य आरोप लगाकर इसको हल्का नहीं किया जा सकता है। यह जीतें वहां की जनता में सत्ता विरोधी रुझान का प्रतीक हैं। कांग्रेस और वामपंथियों से छुटकारा पाने की निशानी हैं।
विपक्षी दलों को अब एकता के लिए जनता का मनोविज्ञान समझना होगा। मोदी के व्यक्तित्व एवं जनता के गुस्से का अर्थ समझना होगा। क्योंकि जैसे जैसे वाम दल कमजोर होते जा रहे हैं। विपक्षी एकता की संभावना कम होती जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व को क्षेत्रीय दल स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वाम पंथियों के पास भी कोई ऐसा स्वीकार्य नेता नहीं बचा है जिसे राष्ट्रीय परिदृश्य में स्वीकार्यता मिली हुयी हो। मोदी विरोध में विपक्ष किसी बड़े कद्दावर नेता को खड़ा नहीं कर पा रहा है। दूसरे मोर्चे को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी स्वीकार नहीं हैं। ऐसे में तीसरे मोर्चे के बनने की संभावना बढ़ रही हैं। ममता बनर्जी एवं चन्द्रशेखर राव की मुलाकात से इसका खाका खिंचने लगा है। ओवैसी इसमें शामिल हो सकते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि मोदी विरोधी वह सभी दल जो राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करते हैं वह तीसरे मोर्चे में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धुर विरोधी माया-मुलायम का एक साथ आना तीसरे मोर्चे के अंदर की सुगबुगाहट दिखा रहा है। सपा ने 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया था और उसका हश्र सबने देखा था इसलिए राहुल गांधी से दूर रहने में ही भलाई दिख रही है। अब विपक्षी एकता दूसरे और तीसरे मोर्चे में बंटने जा रही है। तीसरा मोर्चा दूसरे से ज़्यादा मारक होगा यह तो तय है।
लगातार सफलता की सीढिय़ां चढ़ रही भाजपा के अंदर अहंकार भी दिखने लगा है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी एवं विपक्षी एकता के द्वारा उपचुनावों में लगातार भाजपा की हार भी हो रही हैं। 2019 में हिन्दी भाषी प्रदेशों में भाजपा की सीटें कम होंगी और उसकी भरपाई शायद पूर्वोत्तर के राज्यों से हो सकती है। भाजपा के लिए इस वजह से पूर्वोत्तर की जीत महत्वपूर्ण हो जाती है।
उत्तर प्रदेश उपचुनाव : अधिनायकवाद की हार
उत्तर प्रदेश में फूलपुर एवं गोरखपुर उपचुनाव में हार के बड़े मायने हैं। एक साल पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। सपा और बसपा दोनों का लगभग सफाया हो गया था। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। सत्ता के गलियारों में जैसी चर्चा सुनने में मिलती हैं उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बनाए गए। ज़्यादातर फैसले दिल्ली में बैठे भाजपाई आका लेते रहे। योगी जी ने अपने प्रारम्भिक दिनो में अवैध बूचडख़ाने, एंटी रोमियो स्क्वाड, धड़ाधड़ एंकाउंटर के द्वारा जनता में अपनी मजबूत पैठ बनानी शुरू कर दी थी। उनकी लोकप्रियता इतनी तेज़ी के साथ बढऩे लगी कि दिल्ली को उनकी लोकप्रियता खटकने लगी। योगी जी पर लगाम लगा दी गयी। फैसले लेने के क्रम में योगी जी कमजोर कर दिये गए। ज़्यादातर फैसले दिल्ली से अमित शाह एवं उत्तर प्रदेश में उनके संगठन मंत्री सुनील बंसल के द्वारा लिए जाने लगे। पार्टी को कॉर्पोरेट की तरह चलाया जाने लगा। जिस तरह के नफा नुकसान कॉर्पोरेट कल्चर में होते हैं वह होने लगे। जिस तरह के ऐब कॉर्पोरेट कल्चर में होते हैं वह पनपने लगे। भाजपा कार्यकर्ता हाशिये पर जाने लगा। जो भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी के जीतने पर खुशियां मना कर अभी थकान भी दूर नहीं कर पाया था उसको अपनी पार्टी की जीत पराई लगने लगी।
इसको समझने के लिए थोड़ा पीछा लौटते हैं। 2014 में भाजपा की जीत के समय राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थी। कांग्रेस विरोधी लहर एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे देश ने ब्रांड मोदी को वोट दिया। मोदी कद्दावर नेता बन कर उभरे। इसके बाद मोदी के शपथ ग्रहण के बाद राजनाथ सिंह सरकार में आ गए तो अमित शाह संगठन को संभालने लगे। इसके बाद हुये विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत मिलती गयी। ब्रांड मोदी के नाम पर लगातार मिल रही इन जीतों का श्रेय अमित शाह के चुनावी प्रबंधन को दिया जाने लगा। वह राजनीति के चाणक्य कहलाए जाने लगे। अमित शाह के कुशल प्रबंधन को नकारा भी नहीं जा सकता है किन्तु एक तथ्य यह भी है कि जिन प्रदेशों में ईमानदार और लोकप्रिय चेहरा मोदी के सामने आया वहां भाजपा की हार हुयी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और नितीश कुमार ने बिहार में अपने साफ चेहरे के दम पर मोदी की भाजपा को हरा दिया। इस बात को कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि जिस विजय को हम चुनावी प्रबंधन और रणनीतिक कौशल से जोड़ कर देख रहे हैं वास्तव में वह मोदी के साफ चेहरे का भी परिणाम था।
इसके बाद चुनावी प्रबंधन और जातीय गणित के नाम पर अन्य दलों के नेताओं को भाजपा में भरा जाने लगा। 2014 के लोकसभा और 2017 के उत्तर प्रदेश चुनावों तक तो कार्यकर्ता इस खुशी में झूमता रहा कि कैसे भी हो दशकों बाद किसी तरह भाजपा की सरकार बन जाये। अगर उम्मीदवार बाहरी भी था तो भी कार्यकर्ता उसे मनोयोग से लड़ाता रहा। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव हुये तो भाजपा कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि भाजपा लहर में अब कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेंगे। पर भाजपा प्रबंधन ने ऐसा किया। इस बार भी बाहरियों को टिकट दिये गए। चूंकि उत्तर प्रदेश में बदलाव की एक लहर चल चुकी थी इसलिए जनता ने इस बार भी मेयर की सीटों पर भाजपा को जिता दिया। नगर निगम एवं नगर पंचायतों के चुनावों में बसपा और सपा की उपस्थिती भी दजऱ् हुयी। एक तरफ भाजपा का कार्यकर्ता निराश होने लगा था वहीं दूसरी तरफ सपा और बसपा को नगर निकायों के चुनावों ने एक संजीवनी प्रदान कर दी। भाजपा का संगठन लगातार कार्यकर्ताओं को निराश करता रहा। कार्यकर्ता का कोई काम उनकी अपनी ही सरकार में नहीं हुआ। ठगा सा महसूस करता भाजपा कार्यकर्ता हताश होकर घर बैठ गया। केंद्र और राज्य दोनों स्थानों पर भाजपा की सरकार होने के कारण भाजपा कार्यकर्ता किसी भी सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था।
अहंकार में डूबा भाजपा नेतृत्व
फिर योगी आदित्यनाथ एवं केशव मौर्य के विधान परिषद में जाने के कारण फूलपुर और गोरखपुर में उपचुनाव हुये। इन दोनों सीटों पर इन दोनों कद्दावरों के पसंद के लोगों को टिकट नहीं दिये गए। फूलपुर में एक बाहरी व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया जो केशव मौर्य की पसंद नहीं थे। गोरखपुर में पिछले आठ बार से गौरक्ष पीठ के मठ का व्यक्ति सांसद रहा है। योगी आदित्यनाथ इस बार भी मठ से जुड़े व्यक्ति को लोकसभा का टिकट चाहते थे। दिल्ली के आलाकमान ने इन दोनों सीटों पर दोनों कद्दावरों को नजऱ अंदाज़ किया। प्रदेश के संगठन के लोग भी इसी मुगालते में रहे कि जनता इस बार भी मोदी और कमल को वोट देगी। इस बीच राज्यसभा चुनावों के समीकरण के चलते मायावती और अखिलेश में इन चुनावों के लिए समझौता हो गया। उपचुनावों से परहेज़ रखने वाली बसपा ने सपा को समर्थन दे दिया। पहले से ही अपने अहंकार में डूबा भाजपा नेतृत्व इस गठबंधन का तोड़ नहीं निकाल पाया। चूंकि भाजपा का कार्यकर्ता पहले से ही निराश और हताश बैठा था इसलिए उसने इन चुनावों में कोई रुचि ही नहीं ली। सपा-बसपा के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को अहम की लड़ाई बना कर प्रयास किया और जीत हासिल की।
इन चुनावों में कम वोट प्रतिशत इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जनता ने इन चुनावों में कोई रुचि नहीं दिखाई। वह न तो मोदी के कार्यों से खुश दिखी और न ही मोदी विरोध की कोई लहर ही बनी। बस मतदाता उदासीन हो गया। सपा और बसपा के एक होने के बावजूद जीत का अंतर काफी कम रहा। यह इस बात को दर्शाता है कि सपा और बसपा का पूरा वोट बैंक ट्रान्सफर नहीं हुआ है। इस गठबंधन को जनता की मान्यता अभी नहीं मिली है। भाजपा के कार्यकर्ता में अगर थोड़ा सा जोश बढ़ जाता तो यह चुनाव सपा के लिए आसान नहीं होते। योगी और मौर्य के पसंद के उम्मीदवार न होने के संकेत भी कार्यकर्ताओं की हताशा को बढ़ाने वाले रहे। भाजपा की इस हार में एक और तथ्य अवश्य विचारणीय है। हालांकि भाजपा की केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है किन्तु भाजपा की राज्य सरकारें दूध की धुली नहीं हैं। संगठन को कॉर्पोरेट की तरह चलाने के कारण दिल्ली और लखनऊ के नेता पैसों के लेनदेन में सामंजस्य बनाए रखते हैं। जमीनी कार्यकर्ता जो संगठन में न तो सम्मान पा रहा था और न ही उसे कुछ आर्थिक लाभ हो पा रहा था वह शायद स्वयं भाजपा को झटका लगने की प्रतीक्षा कर रहा था। नरेश अग्रवाल के आने से भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इस तरह से जो यह पूरा राजनैतिक कोलाज बन रहा था उसमें भाजपा की हार कार्यकर्ताओं को अपनी जीत की तरह महसूस हुयी।
राजस्थान और मध्य प्रदेश की डगर है कठिन
लोकलुभावन बजट देकर मोदी सरकार ने एक संकेत दिया था कि वह समय पूर्व लोकसभा चुनाव करा सकती है। लोकसभा चुनाव नवंबर में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के साथ हो सकते हैं। राजस्थान में गत माह तीन स्थानों अलवर, अजमेर में लोकसभा एवं मांडलगढ़ में विधानसभा चुनाव हुये थे। इन तीनों चुनावों में कांग्रेस की जीत हुयी और भाजपा हार गयी। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होने के बाद भी हार के कई कारण निकल कर आये। अजमेर और अलवर में भाजपा के कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल दिखा। जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर भाजपा में जान फूंकी थी उनकी अनदेखी हुयी। वसुंधरा सरकार में कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिली। केंद्र की भाजपा ने पहले के चुनावों में आयातित प्रत्याशियों पर दांव लगाया था। उस समय कार्यकर्ताओं ने उन्हें जी जान से लड़वाया और जिता दिया। बाद में स्थानीय कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के बदले कुछ नहीं दिया गया। वह हताश होने लगे। इन चुनावों में उन्होंने अपने दल से भीतरघात किया और भाजपा हार गयी। एक अन्य वजह यह रही कि वसुंधरा का विरोध राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। उनसे न आम जनता खुश है न भाजपा कार्यकर्ता। वसुंधरा को कमजोर करने के लिये भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही अपने प्रत्याशियों को हरवा दिया। सूबे की मुखिया होने के कारण वसुंधरा की किरकिरी हुयी। उनका कद घटा और भाजपा के नए चेहरे के रूप में राज्यवर्धन राठौड़ का नाम और चमक गया। इसके साथ ही थावर चन्द्र गहलौत एवं ओम माथुर को भी वसुंधरा के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में दो सीटों पर उपचुनाव हुये हैं। इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस विजयी रहीं। बिहार के अररिया में लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की हार नितीश और भाजपा की दोस्ती का भविष्य तय करने वाली है।
हालांकि, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी परिणामों में एक अंतर है। राजस्थान में जो सीटें भाजपा हारी है वह भाजपा के ही पास थीं जबकि राजस्थान में जो सीटें भाजपा जीत नहीं पायीं उस पर पहले से ही कांग्रेस का कब्जा था। उपचुनावों की इन हारों ने विपक्ष को संयुक्त होने का एक विकल्प दे दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत कांग्रेस की मजबूती का प्रतीक नहीं है। उपचुनावों में उतनी गंभीरता न जनता दिखाती है न ही सरकार। उपचुनावों में मोमेंटम का प्रभाव भी कम दिखता है। हालांकि, कांग्रेस का जीतना उसे मजबूती प्रदान कर रहा है। पहले गुजरात में मजबूत हुयी कांग्रेस को राजस्थान में जीत ने राहुल गांधी की पप्पू छवि को धूमिल करने का काम किया है। राहुल अब नेता के रूप में कुछ निखरे दिख रहे हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल को उनकी लोकप्रियता का एहसास कराया गया। नवजोत सिद्धू ने राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़े। एक समय मनमोहन सिंह को पानी पी पीकर कोसने वाले सिद्धू ने अब मनमोहन सिंह के मौन को उनकी शक्ति बताया है। सिद्धू ने मनमोहन सिंह के पैर छूए जो यह दिखाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अब कभी किसी दिन ताज़े ताज़े भाजपाई नरेश अग्रवाल भी राम की तारीफ करते नजऱ आने वाले हैं।
वापस राजस्थान की तरफ देखें तो एक ओर भाजपा में वसुंधरा के स्थान पर राज्यवर्धन का नाम उछाला जा रहा है तो वहीं कांग्रेस में सचिन पाइलट एवं अशोक गहलौत में आपसी कशमकश जारी है। अशोक गहलौत के कार्यक्रम में जब दिग्गज कांग्रेसी पहुंचे थे तो सचिन पाइलट वहां से नदारद थे। इन सबके बावजूद कांग्रेस राजस्थान में मजबूत दिखने लगी है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की विजय संभव है। इसके इतर अगर लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ ही हो जाते हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी मैजिक का फायदा विधानसभा चुनावों में भी मिल जाएगा और भाजपा प्रदेश में फिर से जीत सकती है। मध्य प्रदेश में भी लगातार तीन कार्यकाल के बाद शिवराज सरकार के प्रति किसानों में नाराजगी है। विधानसभा चुनावों में यह नाराजगी कांग्रेस को मजबूत बना रही है। पर राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी रुझान का फायदा कांग्रेस को तब मिलेगा जब केंद्र में भी कांग्रेस एवं सहयोगी दल मजबूत हो। उपचुनावों की लगातार हार ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो दे ही दिया है।
अधिवेशन के बावजूद लाचार कांग्रेस, हताश विपक्षी एकता
कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी खूब गरज़े। सोनिया गांधी ने सक्रिय भाग लिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कसीदे पढ़े। राहुल गांधी ने मोदी और संघ को जी भर कर कोसा। मनमोहन सिंह एवं सिद्धू में राजनैतिक तल्खियां कम दिखीं। सिद्धू मनमोहन सिंह के सामने नतमस्तक हो गए। दिग्गज कांग्रेसी इस पूरे ड्रामे का आनंद लेते रहे। वर्तमान में जितनी कांग्रेस एक लाचार दल के रूप में बनी हुयी है उतनी ही विपक्षी एकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मोदी विरोध के कारण एक जुट होने में प्रयासरत विपक्ष के पास एकजुट होने का कोई बहाना नहीं बन पा रहा है। अभी तक भारतीय राजनीति का यह इतिहास रहा है कि सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए कई दल एक साथ एक मंच पर आ जाते हैं और गठबंधन सरकार में सबकी हिस्सेदारी हो जाती है। मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चन्द्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी एवं मनमोहन सिंह की सरकारें गठबंधन सरकारें ही रही हैं। 2014 में मोदी के प्रचंड बहुमत ने विपक्ष को ऐसे उड़ा दिया कि इस बार संयुक्त विपक्ष को सत्ता भी मिलती नहीं दिख रही है। कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी संयुक्त विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा नहीं बन पा रहे हैं। लालू यादव जेल में हैं। ऐसे में शरद पवार ने अलग अलग स्वभाव के कई दलों के गठबंधन की कवायद शुरू की है।
शरद यादव महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में एक समय बड़ा कद होने के बावजूद जबसे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है वह एक क्षेत्रीय नेता बन कर रह गए हैं। वह स्वयं को संयुक्त विपक्ष का नेता मान कर चलना शुरू हुये ही थे कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि संयुक्त विपक्ष का नेता वह हो जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो और उसे प्रशासनिक अनुभव हो। इसके द्वारा ममता ने साफ कर दिया कि राहुल और शरद पवार का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं है क्योंकि ये दोनों उनके दोनों मापदण्डों पर खरा नहीं उतरते हैं। इसके बावजूद जब संयुक्त विपक्ष की बैठक यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुरू हुयी तब कांग्रेस में राहुल के समर्थक नाराज़ हो गए। उनका मानना है कि जब राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में संयुक्त विपक्ष की बैठक का क्या औचित्य है। राहुल गांधी के अतिरिक्त किसी अन्य का संयुक्त विपक्ष का चेहरा बनना इन कांग्रेसियों को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस के अस्तित्व के हिसाब से यह बात ठीक भी है। कांग्रेस को 2014 के चुनाव में एक बड़ी हार के बावजूद ग्यारह करोड़ वोट मिले थे।
पिछले चार सालों में विपक्ष ने इस बात की लगातार कोशिश की है कि मोदी सरकार को पूंजीपतियों की सरकार साबित कर दें। समय समय पर मोदी और अडानी-अंबानी सम्बन्धों को प्रचार किया गया। सरकार द्वारा उज्जवला योजना के द्वारा एक बार जो गरीब जनता का विश्वास जीता गया वह आज तक बरकरार है। संयुक्त विपक्ष हमलों से कमजोर होता चला गया और मोदी सरकार लगातार मजबूत होती चली गयी। इस मजबूती के बीच जब इस वर्ष के बजट में गरीबों के लिए योजनाओं की बारिश हुयी तो संयुक्त विपक्ष की एकता की एक कोशिश नाकाम हो गयी। सत्ता हाथ में आते न देख विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद जो एक अच्छे नेता की छवि बनाई थी वह तब धूमिल हो गयी जब गुजरात नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ा। बहरीन में दिये गए राहुल के भाषण ने भारत में उनकी किरकिरी कराई। चूंकि तमाम प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी से युवा नहीं जुड़ पा रहा है इसलिए कांग्रेस की दावेदारी सर उठाने से पहले ही खत्म हो जाती है।
ऐसे में विपक्षी एकता का झुनझुना बजने के पहले ही बंद हो गया दिखता है। विपक्ष को अगर संयुक्त विपक्ष बनना है तो अब उसे अपना एक राष्ट्रीय चिंतन बनाना होगा। वह चिंतन जो भाजपा के चिंतन का वैकल्पिक चिंतन का रूप ले सके। जिसमें मोदी विरोध से ज़्यादा मोदी सरकार की असफलताओं पर ध्यान केन्द्रित हो। जिसमें तुष्टीकरण के स्थान पर मोदी का वैकल्पिक राष्ट्रीय चिंतन हो। पर विपक्ष इस पर एक राय नहीं बना पा रहा है। अलग अलग प्रदेशों के क्षेत्रीय समीकरण कांग्रेस के संयुक्त विपक्ष के प्रस्ताव को ठप्प कर देते हैं। बिहार में लालू जेल में है तो उनका दल अभी कमजोर है। उनके बच्चों में लालू जैसी राजनैतिक चपलता नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का दल स्वयं को कांग्रेस से बड़ा दल मानता है। कांग्रेस के साथ गठबंधन का नुकसान वे 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उठा चुका है। बंगाल में ममता स्वयं संयुक्त गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। ऐसा ही हाल अन्य प्रदेशों का भी है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, झारखंड में जेएमएम, तमिलनाडु में दृमुक कांग्रेस के पाले में सिर्फ पेंडुलम की तरह झूलते दिखते हैं। पूरी तरह टिकते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रीय दल जो भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं वह कांग्रेस के साथ भी फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। अगर क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं बैठता है तो आगामी लोकसभा चुनावों में वोटों के विभाजन के कारण भाजपा को किसी से भी टक्कर की कोई संभावना नहीं है। समय पूर्व चुनाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय दलों का कमजोर होना भी तय है।
एक साथ चुनाव से कमजोर होंगे क्षेत्रीय दल
सत्ता के गलियारों में समय पूर्व लोकसभा चुनावों की आहट सुनाई देती रहती है। एक साथ चुनाव की स्थिति में राष्ट्रीय दल फायदे में रहते हैं। क्षेत्रीय दलों की राजनीति क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़्यादा केन्द्रित रहती है। एक साथ चुनाव होने पर मतदाता एक ही राजनैतिक दल को वोट देगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे मतदाता लगभग 77 प्रतिशत होंगे। चूंकि आज का मतदाता जागरूक है इसलिए उसका वोट केंद्र की राजनीति के हिसाब से होगा। ऐसे में प्रदेश की सत्ता भी उसी दल के हाथ में आएगी जिसकी केंद्र में सरकार होगी। केंद्र और राज्य में बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
अब तस्वीर का दूसरा पक्ष भी देखना महत्वपूर्ण है। भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य महत्वपूर्ण कारक हैं। राज्य के चुनाव राज्य के विषयों पर होते हैं और केंद्र के चुनाव राष्ट्र की नीति के हिसाब से। इस तरह संघवाद की अवधारणा पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी लाज़मी है। इसके साथ ही इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि विधानसभा एवं लोकसभा दोनों पूरे पांच साल चले। अल्पकाल की एक सरकार होने के बाद यह प्रक्रिया फिर से ध्वस्त हो जाएगी। यदि चुनाव एक साथ करवाने के क्रम में यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो यह संविधान की मूल भावना का खिलवाड़ होगा। यदि लोकसभा चुनाव समय पूर्व करने की स्थिति में किसी राज्य की विधानसभा को समय पूर्व बर्खास्त किया जाता है तो जनादेश का अपमान होगा। अनु.-356 के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। इतिहास में ऐसा हो भी चुका है। आपातकाल के दौरान पहले इन्दिरा गांधी ने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग किया, इसके बाद 1977 में जनता पार्टी सरकार ने कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। पूर्व में रही कांग्रेस की सरकारों ने भी इस तरह का दुरुपयोग किया था। स्वार्थ सिद्धि के लिए किए जाने वाले यह फैसले लोकतन्त्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने लगते हैं।
ऐसा ही कुछ अविश्वास प्रस्ताव के साथ होता है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जि़क्र नहीं है। ‘लोकसभा के नियम और आचरण’ की पुस्तक में इसका जि़क्र है जो नियम 198 के तहत वर्णित है। इसके अनुसार जब पचास या इससे ज़्यादा सदस्य एक साथ आ जाते हैं तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना होगा। भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर अगर अन्य दल गठजोड़ करके नयी सरकार का गठन नहीं कर पाते हैं तो एक साथ चुनाव की परिकल्पना सिर्फ एक कल्पना बन कर रह जाएगी। फिर कैसे समाधान की तरफ बढ़ा जाये। चुनावी खर्च को कैसे कम किया जाये? इसका भी एक समाधान 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट में दिया गया था। जर्मनी के संविधान में एक प्रावधान है। वहां चांसलर सत्ता का सर्वोच्च होता है जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है। इस प्रावधान के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में किसी अन्य सदस्य के प्रति विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है। मौजूदा चांसलर के प्रति अविश्वास एवं किसी नए सदस्य के प्रति विश्वास पारित होने की स्थिति में वैकल्पिक राजनैतिक विकल्प मिल जाता है। मध्य चुनाव से बचा जा सकता है। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो संसद में नकारात्मक राजनीति ज़्यादा होने लगती है। किसी वैकल्पिक विश्वास की परिकल्पना तो अच्छी दिखती है किन्तु इसकी संभावना बेहद कम दिख रही है।
सहयोगियों के साथ रिश्ते संभाले भाजपा
समय पूर्व चुनाव से ही भाजपा की सत्ता में वापसी हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ बेहतर नीतियां एवं विकास भी अहम नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है अपने सहयोगियों को अपने साथ रखना। किसी भी सहयोगी दल के अलग होने की स्थिति में कभी भी समीकरण बदल सकते हैं। 2004 में हुये चुनाव के दौरान भाजपा से उसके सहयोगी डीएमके एवं राम विलास पासवान नाराज़ हो गए थे। तत्कालीन भाजपा ने इस नाराजगी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी और भाजपा के नेतृत्व वाला राजग चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गया। पुरानी भूलों से भाजपा नेतृत्व को समय रहते सबक लेना चाहिए। इस बार चन्द्रबाबू नायडू भाजपा से नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने बाहर का रास्ता अपना लिया है। उनकी नाराजगी इतनी ज़्यादा नहीं है कि सुलह न हो सके। पंजाब में अकाली दल और भाजपा में खटपट है। महाराष्ट्र में भाजपा का बढ़ता जनाधार शिवसेना को रास नहीं आ रहा है और वह भाजपा से दूरी बनाना चाह रही है। हालांकि, भाजपा ने एनसीपी के साथ करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। नितीश कुमार के साथ बिहार में भाजपा की साझेदारी है किन्तु रिश्ते मधुर न होकर सामान्य हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा कब अलग हो जाएं कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में सहयोगियों का असंतुष्ट होना एवं कार्यकर्ताओं की अनदेखी भारी पड़ सकती है।
यदि 2019 और 2004 के चुनावी परिदृश्य की तुलना करें तो 2004 के चुनाव और आज की परिस्थिति में एक अंतर है। उस समय हिन्दू एक वोटबैंक के रूप में नहीं था। जातियों में बंटे हिन्दू समाज और मुस्लिम तुष्टीकरण के द्वारा दलों ने अपने वोट बैंक तैयार किए हुये थे। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जैसे तैसे भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया था। 2014 में परिदृश्य बदला। जातियों में बंटे हिन्दुओं ने एकजुट होकर वोट किया। हिन्दू वोट बैंक निर्णायक साबित हुआ। वर्तमान में अभी यह भाजपा का स्थायी वोट बैंक नहीं बना है। एक समय काल में लगातार साथ रहने के बाद ही उसे स्थायी वोट बैंक माना जा सकता है। वोट बैंक की गणित को समझने के लिए हमें आज़ादी के बाद की राजनीति को समझना होगा।
1947 में देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक थे। दलित पिछड़े हुये थे। मुसलमानों और दलितों को संरक्षण देने के नाम पर कांग्रेस ने इनको पोषित किया। धीरे धीरे कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के कारण यह वर्ग कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक बन गया। आज़ादी की दुहाई देकर कांग्रेस ने दलितों को अपने साथ जोड़े रखा। नेहरू के प्रारम्भिक काल में यह गठजोड़ खूब देखा गया। इसके बाद इन्दिरा गांधी के आने के बाद महिलाओं का रुझान इन्दिरा की तरफ था और महिलाओं का वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक बन गया। गरीबी हटाओ नारे के साथ गरीबों का वोट इन्दिरा कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो गया। इन्दिरा और नेहरू की छवि से बना वोट बैंक धीरे धीरे कांग्रेस का वोट बैंक बनता चला गया। अब अगर वर्तमान में भाजपा के स्थायी वोट बैंक की बात करें तो अभी दलित भाजपा से स्थायी रूप से नहीं जुड़ पाया है। उसने अपना भरोसा तो भाजपा पर जताया है किन्तु उस भरोसे को बरकरार रखने के लिए भाजपा को निरंतर प्रयास करने होंगे। हालांकि, भाजपा के द्वारा ऐसे प्रयास हुये भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द दलित वर्ग से। जिस जाति विशेष का नेता सत्ता में होता है उस वर्ग का वोट स्वत: उसके साथ हो जाता है। ऐसा भारत का राजनैतिक इतिहास रहा है।
यदि स्थायी वोट बैंक की चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भाजपा के स्थायी वोट बैंक में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहने वाला वर्ग शामिल है। रोजगार के नए अवसर तलाश रहा युवा शामिल है। सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहीं महिलाएं इसमें शामिल हैं। यह एक नए तरह का वर्ग है जो स्थायी वोट बैंक का स्थान ले रहा है। तीन तलाक से मुक्ति पायी मुस्लिम महिलाएं इसमें शामिल हैं। कांग्रेस राज में रोज़ रोज़ नए घोटाले सुनकर अपना सर नोचने वाले वर्ग इसमें शामिल हैं। रोजगार प्राप्ति की आस लगाए युवा इसमें शामिल हैं। ये जातियों और धर्मों से अलग वर्ग है। यह परंपरागत राजनीति से अलग तरह की राजनीति है। इसमें मोदी से अपेक्षाओं के पूरे न होने का दर्द तो है किन्तु मोदी की विश्वसनीयता से आस अभी भी बनी हुयी है। मोदी के कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। अभी हाल फिलहाल में पीएनबी और रोटोमक घोटाले जरूर भाजपा के गले की फांस बनते दिख रहे हैं। इनमें एक बात जो खुल कर आ रही है कि इन दोनों घोटालों के तार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों से जुड़े दिख रहे हैं। ऐसा होने की स्थिति में भाजपा और मोदी की विश्वसनीयता कम होने नहीं जा रही है। 2019 में जीत के लिए सहयोगियों को मनाने एवं चुनावी गड्ढों को भरते समय भाजपा के संगठन को इस बात को समझना है कि उन्हें जनता ने वोट राम मंदिर, अनु.-370, गौ हत्या पर केन्द्रीय कानून, कश्मीर समस्या का समाधान एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए दिये थे। क्या भाजपा ने इन मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति की है? शायद अभी तक तो नहीं? भाजपा के थिंक टैंक को इस ओर समय रहते ध्यान देना होगा। वरना 2004 की पुनरावृत्ति होने की संभावना बरकरार रहेगी। ठ्ठ
भाजपा क्यों हारी?
कहते हैं गोरखपुर में बीजेपी की हार की आधी स्क्रिप्ट तो उसी दिन लिख दी गई थी, जब वहां से उपेंद्र दत्त शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया था। उपेंद्र शुक्ला अगर जीतते तो ये बीजेपी, मोदी और योगी की जीत से ज्यादा गोरखपुर के मठ की हार होती। गोरखपुर में बीजेपी की इस हार में कहीं न कहीं मठ की अपनी जीत भी छिपी है।
गोरखपुर की सियासत को करीब से जानने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यहां की सियासत ब्राह्मण बनाम ठाकुर की चलती आ रही है। ये लड़ाई आज की नहीं है। दशकों पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। बताया जाता है कि उस वक्त गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ हुआ करते थे। गोरखपुर के ब्राह्मणों के बीच पं. सुरतिनारायण त्रिपाठी बहुत प्रतिष्ठित थे। किसी वजह से दिग्जिवज नाथ ने सुरतिनारायण त्रिपाठी का अपमान किया था। वहीं से क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण का गणित शुरू हो गया। इसके बाद उस वक्त के युवा नेता हरिशंकर तिवारी ने दिग्विजय नाथ के खिलाफ आवाज उठाई। आगे चलकर ठाकुरों का नेतृत्व वीरेंद्र शाही के हाथ आया, लेकिन हरिशंकर तिवारी का ‘हाता’ और अवैद्यनाथ के ‘मठ’ के बीच गोरखपुर में वर्चस्व की लड़ाई चलती रही।
90 के दशक में योगी आदित्यनाथ के हाथ मठ की कमान आई। योगी ने ‘मठ’ की ताकत बढ़ाई। उनकी हिंदू युवा वाहिनी आसपास के कई जिलों में सक्रिय हुई। इसी बीच साल 1998 में माफिया डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसे ब्राह्मण क्षत्रप कहा जाता था। गोरखपुर में ब्राह्मणों और राजपूतों के बराबर वोट हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की ताकत लगातार बढ़ी, ब्राह्मण नेतृत्व कमजोर होता गया। इसके साथ ही ‘हाता’ का असर कम होता गया। उस वक्त शिवप्रताप शुक्ला ब्राह्मणों के सर्वमान्य और ताकतवर नेता थे। लेकिन योगी की बढ़ती ताकत के साथ ही उनका राजनीतिक पतन होता चला गया। हालत तो ये हुई कि कुछ वर्षों के लिए शिवप्रताप शुक्ला राजनीतिक पटल से ही ओझल हो गए। इस बीच राज्य से लेकर केंद्र तक योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता रहा।
मोदी-शाह युग से पहले आलम ये था कि पूर्वांचल में एक वक्त में मामला योगी बनाम बीजेपी हो गया था। वह जिसे चाहते उसे टिकट मिलता, जिसे नहीं चाहते वह टिकट पाकर भी हार जाता। मजबूरन बीजेपी को उनके आगे घुटने टेकने पड़ते। उनकी हर बात माननी पड़ती। योगी की बनाई हिन्दू युवा वाहिनी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।
साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। मुख्यमंत्री के लिए कई नाम सामने आए। मनोज सिन्हा का नाम फाइनल तक हो गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आरएसएस के समर्थन से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। उनके मुख्यमंत्री बनते ही यूपी में सबसे ज्यादा नाराजगी ब्राह्मणों में थी। यह बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची। इसके बाद मोदी और शाह ने डैमेज कंट्रोल के लिए कई कोशिशें की, जिसमें महेंद्र पांडेय को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाना भी शामिल है। बीजेपी नेतृत्व पूर्वांचल में ठाकुर बनाम ब्राह्मण से भली भांति परिचित हो चुका था। इसलिए योगी की सीट पर टिकट देने के लिए किसी ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी, ताकि यहां भी संतुलन बनाया जा सके।
बीजेपी संगठन और आरएसएस की राय से गोरखपुर उपचुनाव के लिए उपेंद्र दत्त शुक्ल मोदी और अमित शाह की पहली पसंद बने। लेकिन सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ कतई नहीं चाहते थे कि गोरखपुर का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में जाए। योगी के सामने अपनी सीट बचाने से ज्यादा अहम था गोरखपुर में अपने ‘मठ’ की ताकत को बचाना। इसके बावजूद उपेंद्र दत्त शुक्ल को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। चूंकि आदेश अमित शाह का था, तो इसके सीधे विरोध में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन अंदरखाने साजिशों और दुरभिसंधियों का दौर शुरू हो गया। बतौर सीएम योगी ने जमकर प्रचार किया, लेकिन योगी के लोग निष्क्रिय हो गए।
सभी जानते हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी का मतलब योगी और योगी का मतलब संगठन है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार के लिए उनकी मर्जी के बिना जीत हासिल करना टेढ़ी खीर है। इस बार तो आलम ये रहा कि बूथ पर बीजेपी के एजेंट तक मौजूद नहीं थे। इसके उलट सपा और बसपा के समर्थक जोश से लगे हुए थे, जिसका परिणाम सबके सामने है।
कर्नाटक : कांग्रेस के अस्तित्व की आखरी जंग
दक्षिण भारत कांग्रेस और वाम दलों का गढ़ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल को मिलाकर दक्षिण भारत राज्यों का कोरम पूरा होता है। वर्तमान में सिर्फ कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। कुछ समय बाद कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं। जिस तरह की स्थिति का आभास यहां हो रहा है उसके हिसाब से दक्षिण भारत के इस गढ़ से कांग्रेस खत्म होने जा रही है। राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अगर उनकी सबसे बड़ी कोई परीक्षा है तो वह कर्नाटक है। कर्नाटक में जीत राहुल गांधी को विपक्ष के संयुक्त नेता के रूप में स्वीकार्यता प्रदान करेगी तो कर्नाटक की हार राहुल गांधी का राजनैतिक भविष्य सीमित करेगी। कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ के चुनावी अभियान में कूदने से हिन्दुत्व चुनावी मुद्दा बन गया है। इससे निपटने के लिए राहुल गांधी मंदिर दर्शन का क्रम शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही वह चर्च में भी जा रहे हैं ताकि भाजपा को सांप्रदायिक एवं स्वयम को सेकुलर साबित कर सकें। श्रेंगेरी मठ, उडुपी के नारायण मंदिर, दक्षिण कन्नड़, चिकमंगलूर और हासन जिलों के मंदिरों एवं चर्चों में राहुल गांधी के दौरे कांग्रेस के छदम हिन्दुत्व का नया रूप है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को पांडव एवं भाजपा को कौरव की संज्ञा दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देकर हिन्दू वोट बैंक को कमजोर करने का जाल फेंक दिया है। लिंगायत हिन्दू धर्म की ही एक विचारधारा है जो वर्षों से अलग धर्म की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महापुरुषों के रास्ते पर है। वह क्रोध नहीं फैलाते हैं। राहुल के अनुसार मोदी जी जब कहते हैं कि 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ है तब वह आपके दादा दादी, माता-पिता का अपमान करते हैं। राहुल गांधी अपने इन भाषणों से जनता को मोदी से अपमानित होता दिखा कर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं।
दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस सरकार के विरोध और क्षेत्रवार नीति के आधार पर कर्नाटक की तैयारी कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्र भाजपा के लिए बहुत मजबूत नहीं रहा है। 2008 में जब पहली बार भाजपा सरकार बनी थी तो भाजपा को 19 में से दस सीटें मिली थीं। 2013 में हुये विधानसभा चुनावों में भाजपा तीन सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन उसके एक साल बाद ही जब 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर चला तब भाजपा ने 17 सीटों पर बढ़त हासिल की। भाजपा का ध्यान अब उस लहर को वापस प्राप्त करने का है। कुछ मोदी के नाम पर तो कुछ योगी के नाम पर, भाजपा को आस की किरण दिखने लगी है। पूर्व में तटीय कर्नाटक में भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं पर हमले हुये हैं। केरल की सीमा से लगे क्षेत्रों में भी संघ पर हमले होते रहे हैं। इन विषयों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए भाजपा के द्वारा सुरक्षा यात्रा निकाली जा रही है। योगी आदित्यनाथ का इस यात्रा के समापन कार्यक्रम में रहना प्रस्तावित है। कर्नाटक का चुनाव हिन्दुत्व के मुद्दे पर होता दिखने लगा है जिसमें योगी का प्रभाव साफ दिखाई देने लगा है।
कर्नाटक के चुनाव परिणाम देश की राजनीति की दिशा तय करने जा रहे हैं। जिस तरह से त्रिपुरा में भाजपा की जीत ने वाम दलों का गढ़ ध्वस्त किया है वैसे ही कर्नाटक में भाजपा की जीत कांग्रेस का किला तोडऩे जा रही है। वर्तमान में मिज़ोरम, पंजाब, पांडिचेरी एवं कर्नाटक में ही कांग्रेस की सरकार बची है। कर्नाटक की हार के साथ ही राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति से बाहर होने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में विपक्षी एकता का सपना, सपना ही बनने वाला है।
उत्तर प्रदेश का विचित्र त्रिकोण
उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले एक डेढ़ वर्ष में नया त्रिकोण पैदा हो गया है। दलगत वफ़ादारियों से ज्यादा स्वार्थी गठजोड़ रूप ले चुके हैं।
पहला गठजोड़ हिंदुत्ववादी मोदी-अमित शाह-योगी आदित्यनाथ और संघ का एक धड़ा व सपा का अखिलेश-रामगोपाल गुट। सपा में तोडफ़ोड़ के कारण ही यह गुट उत्तर प्रदेश में अपार बहुमत से जीता। पुरुस्कार स्वरूप अखिलेश के घोटालों पर चुप्पी साधी गयी है।
दूसरा गठजोड़ अवसरवादी राजनाथ (ठाकुर)- जेटली (ब्राह्मण), संघ का मोदी को नियंत्रण में लगा एक धड़ा व मुलायम-शिवपाल गुट। जो उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व पुन: बनाना चाहते हैं। पुराने खिलाडिय़ों का यह धड़ा नौकरशाही के एक तबके पर गहरी पकड़ रखता है।
तीसरा गठजोड़ मायावती बनाने में लगी है जिसमें सपा के दोनों धड़े व कांग्रेस को शामिल किए जाने की कोशिश है। अगर सही समीकरण बने व भाजपा में गुटबाजी बढ़ी तो सपा के दोनों धड़े माया के साथ पूर्ण गठजोड़ बना सकते हैं।
ऐसे में सपा- बसपा के घोटालों की जो जांच धीमे चल रही हैं, अंजाम तक पहुंचने लगेंगी। वहीं राजनाथ-जेटली धड़े की गोरखपुर में हार के बाद मोदी-शाह-योगी को लोकसभा चुनावों में फ्री होल्ड मिल गया है व लोकसभा चुनावों में मोदी-शाह आसानी से पत्ते फेट सकेंगे। प्रदेश की राजनीति में हिंदूवादी उफान आना अब तय है।
– अनुज अग्रवाल
नरम हिंदुत्व बनाम प्रखर हिंदुत्व
यूपी में हालिया हार का दोष मोदी व अमित शाह की जोड़ी का अधिक है जो सुनील बंसल को सुपर सीएम बनाकर योगी जी की मुश्के कसे हुए है और गोरखपुर की ब्राह्मण लॉबी को हवा दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि यूपी में योगी के पास 25 प्रतिशत अधिकार भी नहीं। सारा खेल अमित शाह,मोदी, जेटली की तिकड़ी खेल रही है। सभी निर्णय दिल्ली से लिये जाते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर वोटरों को रिझाने के लिए ही योगी का इस्तेमाल किया जाता है और समय समय पर औकात भी बता दी जाती है।
दूसरा बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा अमित शाह की टीम द्वारा दिया जा रहा है। योगी सपाइयों व बसपाइयों सहित नौकरशाही के आकंठ भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते हैं, मगर वे लोग दिल्ली से डील कर योगी को ठेंगा दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में लाखों करोड़ की लूट हुई है जिसके विरुद्ध कार्यवाही के नाटक के नाम पर दिल्ली के नेताओं द्वारा डील की जा रही हैं।
योगी सरकार को एक वर्ष पूरा हो गया है, स्वयं भाजपा ने सपा बसपा के कई लाख करोड़ के घोटालों की पुस्तक जारी की थी सबूतों सहित। प्रदेश का कोई भी पीसीएस अधिकारी 100 करोड़ से कम का और आईएएस अधिकारी 1000 करोड़ से कम का नहीं है। योगी सरकार आने के बाद काम करने के रेट डबल हो गए हैं, मगर सब मजे ले रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं।
असली लड़ाई यही है। मोदी जी का नरम हिंदुत्व बनाम योगी जी का प्रखर हिंदुत्व। योगी जी को निबटाने में राजनाथ जी का भी बड़ा हाथ रहता है क्योंकि योगी जी ने उनके एकछत्र राजपूत नेता की स्थिति को छोटा कर दिया।