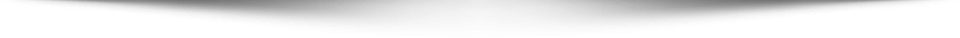[आज सुबह मन में उठ रहा एक प्रश्न यहाँ मित्रों के बीच रखा था। जिन सुधी महानुभावों ने अपनी सुविचारित टिप्पणियों से उसे और अधिक विचारास्पद बनाया उन सभी का सकृतज्ञता साधुवाद।…उसी विषय पर अब थोड़ा विस्तार से]
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
सर्वविदित है कि बसंतपंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। दो कारणों से इसका विशेष महत्व है। पहला, यह सरस्वती पूजन का पर्व है और दूसरा, इसे बसंत ऋतु का प्रवेश द्वार माना जाता है। सरस्वती विद्या, ज्ञान और समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री देवी है तथा बसंत ऋतु नव सृजन और नए संवत्सर की प्रथम ऋतु होने के कारण दोनों ही अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रसंग हैं।
प्रश्न है कि बसंतपंचमी से जुड़े इन दोनों प्रसंगों में क्या कोई पारस्परिक संबंध है?
एक और विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आता है कि भारतीय कालगणना की दृष्टि से चैत्र एवं वैशाख बसंत ऋतु के मास है। जबकि प्रकृति में बसंत ऋतु के चिह्न फाल्गुन मास में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। और यह बसंतपंचमी तो उससे भी बहुत पहले माघ मास में आ जाती है।
तो प्रश्न उठता है कि बसंतपंचमी को शिशिर ऋतु में मनाए जाने की क्या प्रासंगिकता है? शिशिर ऋतु के भी पूर्वार्ध में! माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु के महीने हैं। भारतीय परंपरा में छहों ऋतुओं का मासिकक्रम इस प्रकार है–
चैत्र–वैशाख में बसंत, जेष्ठ–आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण–भाद्रपद में वर्षा, आश्विन–कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष–पौष में हेमंत और माघ–फाल्गुन मास में शिशिर।
भारतीय वाङ्मय में इस विषय पर कोई सुस्पष्ट उत्तर नहीं मिलता कि बसंतपर्व, बसंत ऋतु से लगभग चालीस दिन पूर्व क्यों मनाया जाता है?
यह अनुमानमात्र है कि अतिप्राचीन काल में कभी माघ और फाल्गुन मासों में ही बसंत के चिह्न प्रकट होने लगे होंगे और यह पर्व उसी कालखण्ड का स्मृतिचिह्न होगा। यह भी संभव है कि बसंत आगमन के चिह्न भारतवर्ष के किसी भूभाग में चैत मास लगने के पहले ही दिखाई देने से वहां यह बसंत पर्व मनाया जाने लगा होगा, जो अद्यावधि निरंतर बना हुआ है। इधर आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता में एक समांतर कालगणना का उल्लेख भी मिलता है जिसमें फाल्गुन और चैत्र मास को बसंत ऋतु के अन्तर्गत माना गया है। इस प्रकार बसंत ऋतु वर्तमान कालगणना से एक महीने पूर्व खिसक आती है।
यों भी हमारे चतुर्दिक् पसरी प्रकृति में हम देखते हैं कि बसंत किसी एक दिन, एकाएक नहीं आ धमकता। पतझड़ और पल्लवन का क्रम मास, दो मास तक साथ चलता रहता है। बसंत ऋतु अपने यौवन पर भले ही चैत्र मास में आती हो, परंतु उसका बीज तो माघ मास की पंचमी को ही फूट जाता है। और इस तरह बसन्तपंचमी, सरस्वती पूजन और बसंतागमन का समवेत पर्व बन जाती है।
परन्तु मूल प्रश्न इन दोनों घटनाओं के पारस्परिक संबंध का है। प्रश्न बसंतपंचमी में दोनों प्रसंगों के समाहित होने के औचित्य का है।
सरस्वती गीत, संगीत, काव्य आदि समस्त कलाओं की देवी है। दूसरी ओर बसंत ऋतु को कामनाओं को उद्दीप्त करने वाली ऋतु कहा जाता है। प्रेम, शृंगार, रतिक्रिया आदि का जितना वर्णन बसंत के साथ जुड़ा हुआ है उतना किसी अन्य ऋतु के साथ नहीं। यहां तक कि समाधिस्थ शिव में वासना जगाने के लिए कामदेव ने भी अपने मित्र बसंत का ही सहारा लिया था। ऐसी इस बसंत ऋतु का संयोजन सरस्वती पूजन के साथ होने के इस प्रश्न का उत्तर हमें भारतीय मनीषा की विलक्षण दृष्टि से साक्षात्कार कराता है। भारतीय दृष्टि के इस मूल्यवान संदेश को हमें समझना चाहिए।
जो बसंत मनुष्य की कामभावनाओं के उद्दीपन की ऋतु है, जो बसंत ऋतु सभी चेतन प्राणियों में वासना का उन्माद जगाकर प्राकृतिक जीवसृष्टि के लिए प्रेरित करती है, जो बसंत ऋतु हृदय में ठंडी पड़ी आग को दहका देती है, उसके शमन–शोधन का प्रबंधन है बसंतपंचमी पर्व।
कामनाओं की वेगवती धारा को बाढ़ में बदलने से पूर्व ही मोड़ने का बंदोबस्त कैसे किया जाए; इस प्रचण्ड प्रवाह की मूल आत्मा को बचाते हुए इसे सहज शान्त कैसे बनाया जाए; यह भारतीय परंपरा ने सिखाया है। क्योंकि यह प्रवाह निषिद्ध नहीं है, अपितु जीवसृष्टि के लिए अपरिहार्य है। आवश्यकता इसे रोकने की नहीं साधने की है।
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है,
“कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।” अर्थात् सबसे पहले रचयिता को काम का भाव आया जो कि सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। अत: सृष्टि रचना की इन आधारभूत अपरिहार्य वासनाओं को रोका नहीं जा सकता। उत्पत्ति और विकास की धाराओं को रोकना नहीं, संस्कारित करना अपेक्षित है। इन वासनाओं संस्कारित करने का कार्य साहित्य और कलाएं करती हैं। समस्त कलाएं मनुष्य की कामवासनाओं के रूपांतरण और परिष्कार से जन्मती हैं। कलाओं का अनुशीलन हमारी वासनाओं को ऊर्ध्वमुखी बनाता है। जो मनुष्य को सांसारिक कुंठाओं, क्लेशों और उपद्रवों से मुक्त कर सहज सुन्दर बनाती है।
कला–कुल की स्वामिनी सरस्वती का पर्व बसंतपंचमी, बसंत के साथ आने वाले उसके कामदेव के उद्दामवेग को शमित, संस्कारित और नियंत्रित करने की पूर्व तैयारी है।
बसंत ऋतु सृजन की ऋतु है। प्रकृति के सृजन व्यापार के समांतर मनुष्य के मन में भी सृजन व्यापार चलता रहता है। काम भी मूलत: मन की सृष्टि है। इसीलिए इसे मनसिज, मनोज आदि नाम दिए गए हैं। अर्थात् मन में जन्म लेने वाला। साहित्य और कलाएं भी पहले मन में जन्म लेती हैं फिर बाहरी रूपाकार ग्रहण करती हैं।
यह कितनी विलक्षण बात है कि मनुष्य जैविक सृजन की ऋतु के सोपान पर चढ़ने से पूर्व मानसिक सृजन की अधिष्ठात्री शक्ति की आराधना करे। गीत, संगीत, काव्य आदि समस्त कलाओं की देवी सरस्वती की वन्दना के पीछे यही रहस्य छुपा है। सरस्वती की उपासना अर्थात् साहित्य, कला, संगीत, ज्ञान की साधना। शिशिर की जड़ता जब बसंत की आँच में पिघलने लगती है तो तामस भाव राजस भाव में बदलने लगता है। सरस्वती उपासना का सात्विक भाव मनुष्य को राजसिक भावों से आक्रांत होने से बचाता है। अन्यथा कामदेव तो अपने सहचर बसंत के साथ धनुष बाण लिए तैयार बैठा है। अस्तु, यह सात्विक संतुलन स्थापित करने का पर्व है।
पुरातन के रूपांतरण का अधिष्ठान है बसंत। यह जीर्ण–शीर्ण आवरण को उतारने और नव पल्लवों को प्रस्फुटित करने की वेला है; जिसमें ध्वंस भी है, सृजन भी है। किंतु लक्ष्य है रूपांतरण का। लक्ष्य है विकास का।
रूपांतरण कुछ वस्त्र, आभूषण या मुखौटा बदलने भर का नाम नहीं है। यह रूपांतरण आत्मद्रव के बदलते जाने पर होता है। पुराने पत्ते, फूल, फल नवांकुरों–पल्लवों के लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं। किंतु जड़ और तना अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते, बल्कि कुछ और अधिक मजबूती से धरती को पकड़े रहते हैं।
शीत और ग्रीष्म के दो विपरीत बिंदुओं की संधि रेखा पर स्थित बसंत का यह प्रवेश द्वार गहरी रात के बीतने और पौ फटने का नैसर्गिक घंटाघोष है। यह जड़ता और अंधेरे से गति और प्रकाश की ओर चल पड़ने का संकल्प है।
यह पुरातन के ध्वंस और नव–प्रसव का उत्सव ही नहीं, वरन् धरती के शृंगार का पर्व भी है। ऐसा लगता है मानो सद्य:प्रसूता धरती, गोटा–पत्ती की पीली ओढ़नी और लाख का चूड़ा पहन कर मेहंदी, महावर, हल्दी, काजल, टिकी से सजी-धजी कुआं पूजन के लिए ढोलक की थाप पर मंगलगीत और जच्चा गाती हुई हँसी–ठिठोली करती स्त्रियों से घिरी बैठी हो।
कवियों ने बसंत पर अद्भुत कविताएं लिखी हैं। “पद्मावत” के बसंत–खंड में जायसी बसंत ऋतु का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण करते हैं कि इस ऋतु में सब कुछ नया-नया देखकर उल्लास होता है। और वातावरण ऐसा की देर तक न धूप सुहाती न छाॅंह। खास बात यह है कि वे बसंतपंचमी को “श्री पंचमी” कहते हैं। जैसा कि भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी इसी नाम से जाना जाता है।
“दैऊ देउ कै सो ऋतु गँवाई । सिरी-पंचमी पहुँची आई॥ भएउ हुलास नवल ऋतु माहाँ । खिन न सोहाइ धूप औ छाहाँ॥” (पद्मावत)
भारतेंदु हरिश्चंद्र बसंत को ऋतुओं का कंत (पति) कहकर वातावरण का मनोरम चित्रण करते हैं।
“कंतसखि आयो बसंत रितून को कंत,
चहूँ दिसि फूलि रही सरसों।
बर शीतल मंद सुगंध समीर
सतावन हार भयो गर सों।।
अब सुंदर सांवरो नंद किसोर
कहै ‘हरिचंद’ गयो घर सों।
परसों को बिताय दियो बरसों
तरसों कब पाँय पिया परसों।।”
हिंदी का शायद ही कोई बड़ा कवि होगा जिसने बसंत पर अपनी कलम न चलाई हो। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति, पद्माकर, सेनापति, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी, बच्चन आदि के द्वारा ऋतुराज बसंत पर लिखी इन कविताओं में खिलते फूल, चटकती कलियां, नए चिकने पल्लव, आम की मंजारियां, सुगंधित पवन, उड़ते परागकण, झूमती सरसों, पंचम स्वर में कूॅंजती कोकिल, गुंजार करते भौंरे, रंग–बिरंगी तितलियां के रूप में मुखरित प्रकृति हमारे सामने हंसती–खिलखिलाती–झूमती नजर आती है। कहीं प्रणय व्यापार, कहीं प्रकृति के रंग–गंध, कहीं चेतना का उल्लास हमारी हृदयतन्त्री को झंकृत कर देती है। पाठक का चित्त मधुर मादक काव्यरस से सराबोर हो जाता है। साहित्य में यह वैविध्यभरा बसंत चित्रण अत्यंत मनोरम और हृदयावर्जक है। कुछ कवियों ने बसंतपंचमी को लक्ष्य कर सरस्वती वंदना के रूप में अद्भुत रचनाएं हिंदी साहित्य को दी हैं।
निराला की “वीणावादिनी वर दे” कविता बसंत आगमन के पहले ही, बसंत का बीज फूटने के प्रथम क्षण में हमारे चित्त में सात्विक सृजन का रोमांच भर देती है। कवि जब कहता है कि
“काट अंध-उर के बंधन-स्तर
बहा जननि, ज्योतिर्मय निर्झर;
कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर
जगमग जग कर दे!….
पढ़कर हमारे मन में ज्योति का झरना बहने लगता है। रोम रोम एक नई चेतना से आप्लावित हो उठता है। और तभी नव–नव की दशदिक् आवृत्तियां तन–मन में एक आनन्दमय ऊर्जा का संचार करने लगती हैं।
नव गति, नव लय, ताल-छंद नव
नवल कंठ, नव जलद-मन्द्ररव;
नव नभ के नव विहग-वृंद को
नव पर, नव स्वर दे!
नए आकाश में, नए–नए पक्षियों को नई उड़ान और नए स्वर की कामना ही सरस्वती की आराधना है। यही नव सृजन की आधारभूमि है। पुरातन का उन्मोक और नवीन का संधान ही संस्कृति की चिरनवीनता का रहस्य है।
महाकवि तुलसीदास मानस के प्रारंभ में, मंगलाचरण में सर्वप्रथम देवी सरस्वती को ही नमन करते हैं। “वन्दे वाणीविनायकौ” कहते हुए वे सरस्वती के उपरान्त गणेश का स्मरण करते हैं।
महर्षि वेदव्यास भी सरस्वती को नमन करते हुए महाभारत की रचना आरंभ करते हैं। वे लिखते हैं, “नत्वा सरस्वतीदेवीं ततो जयमुदिरयेत्” अर्थात् सरस्वती देवी को प्रणाम करके जय नामक महाकाव्य को प्रारंभ करें।
दुर्गा सप्तशती के “प्राधानिक रहस्य” में वर्णन है कि भगवती महालक्ष्मी के तमोगुण से महाकाली और सत्वगुण से सरस्वती प्रकट होती हैं।
“तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी: स्वरूपमपरं नृप।
सत्वाख्येनाति शुद्धेन गुणेनेंदु प्रभं दधौ।
अक्षमालांकुशधरा वीणापुस्तकधारिणी।।
सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ।
महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती।
आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी।।
(श्लोक सं.14–16 प्राधानिकं रहस्यम्, श्री दुर्गासप्तशती)
अर्थात् महाकाली को प्रकट करने के उपरांत महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण का था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे इस प्रकार नाम प्रदान किए– महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, देवगर्भा, और धीश्वरी।।
वस्तुत: महादेवी की तीन शक्तियां हैं, जो स्वतंत्ररूप से पूजी जाती हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और काली। लक्ष्मी की एकनिष्ठ उपासना मनुष्य को भौतिक समृद्धि की ओर ले जाती है, जिसकी चकाचौंध में वह मंगल–मूल्यों के पथ से विरत हो जाता है। काली की एकनिष्ठ उपासना मनुष्य को वीरभाव और विजीगीषु वृत्ति की ओर ले जाती है, जिसके वशीभूत मनुष्य निरंतर संघर्ष में रहता है। एक में राजस का अतिरेक है, दूसरे में तामस का। सरस्वती की उपासना मनुष्य को ज्ञान–विज्ञान की ओर ले जाती है, यह सहजता और शमन का पथ है जो सात्विक भावों का संवर्धन करता है।
कहना न होगा कि स्वस्थ, समृद्ध और मंगलकारी जीवन के लिए सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों भावों का सामंजस्य और संतुलन आवश्यक है।
**************************************
इंदुशेखर तत्पुरुष