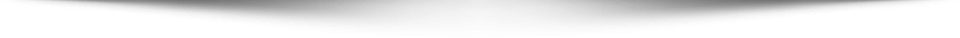एक वकील के घर मिलन के अवसर पर लोकमान्य तिलक द्वारा गुलामी को राजनीतिक समस्या बताने की प्रतिक्रया में स्वामी विवेकानंद ने कहा था – ”परतंत्रता राजनीतिक समस्या नहीं है। यह भारतीयों के चारित्रिक पतन का परिणाम है।” बापू को लिखी एक चिट्ठी के जरिए लाॅर्ड माउंटबेटन ने भी चेताया था – ”मिस्टर गांधी क्या आप समझते हैं कि आजादी मिल जाने के बाद भारत.. भारतीयों द्वारा चलाया जायेगा। नहीं ! बाद में भी दुनिया गोरों द्वारा ही चलाई जायेगी” यही बात बहुत पहले अपनी आजादी के लिए अकबर की शंहशाही फौजों से नंगी तलवार लेकर जंग करने वाली चांदबीबी की शौर्यगाथा का गवाह बने अहमदनगर फोर्ट में कैद ब्रितानी हुकूमत के एक बंदी ने एक पुस्तक में लिखी थी।
‘ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री’ के जरिए पंडित जवाहरलाल नेहरु ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक साम्राज्यवाद का खुलासा करते हुए 1933 में लिखा था – ”सबसे नये किस्म का यह साम्राज्य जमीन पर कब्जा नहीं करता; यह तो दूसरे देश की दौलत या दौलत पैदा करने वाले संसाधनों पर कब्जा करता है।…. आधुनिक ढंग का यह साम्राज्य आँखों से ओझल आर्थिक साम्राज्य है” आर्थिक साम्राज्य फैलाने वाली ऐसी ताकतें राजनैतिक रूप से आजाद देशों की सरकारों की जैसे चाहे लगाम खींच देती हैं। इसके लिए वे कमजोर, छोटे व विकासशील देशों में राजनैतिक जोङतोङ व षडयंत्र करती रहती हैं। ऐसी विघटनकारी शक्तियों से राष्ट्र की रक्षा के लिए चेताते हुए पंडित नेहरु ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का इतना उलझा हुआ जाल बताया था कि इसे सुलझाना या इसमें एक बार घुस जाने के बाद बाहर निकलना अत्यंत दुष्कर होता है। इसके लिए महाशक्तियां अपने आर्थिक फैलाव के लक्ष्य देशों की सत्तााओं की उलट-पलट में सीधी दिलचस्पी रखती हैं।
दुर्योग से कालांतर में देश ने इन दर्ज बयानों को याद नहीं रखा। आजादी बाद कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक मंडल गठन के गांधी संदेश की दूरदृष्टि को भी देश भूल गया। स्मृति विकार के ऐसे दौर में भारतीय लोकनीति, रीति और प्रकृति और संस्कार की सुरक्षा कैसे हो ? गणतन्त्रता के 68वें पङाव पार खङे भारत के समक्ष आज यह प्रश्न बङा है और बेचैनी भी बङी। ये बेचैनी अभी अलग-अलग है; कल एकजुट होगी; यह तय है। यह भी तय है कि यह एकजुटता एक दिन रंग भी लायेगी। अब आपको-हमें तय सिर्फ यह करना है कि इस रंग को आते देखते रहें या रंग लाने में अपनी भूमिका तलाश कर उसकी पूर्ति में जुट जायें। आकलन यह भी करना है कि अंधेरा क्यों हुआ ? रोशनी किधर से आयेगी ? दियासलाई…दीया कौन बनेगा, तेल कौन और बाती कौन ??
बंद गली के मुहाने पर हम
याद करने की बात है कि प्राचीन युगों में एकतंत्र गणतंत्रों को चाट जाते थे। मगघ साम्राज्य ने बहुत से गणतंत्रों का सफाया कर दिया था। यह आज का विरोधाभास ही है कि आधुनिक संचार के इस युग में भी दुनिया की महाशक्तियां दूसरे लोकतंत्रों को चाट जाने की साजिश को अंजाम देने में खूब सफल हो रही हैं। यह सही है कि यह विरोधाभास किसी एक-दो देश या राजनेता का विरोधाभास नहीं है; यह पूंजी की खुली मंडी का विरोधाभास है। जो भी तंत्र इस मंडी की गिरफ्त में है, वहां आदर्शों का मोलभाव सट्टेबाजों की बोलियोें की तरह होता है। इस तरह की पूंजी मंडी मंे उतर कर देश लोहिया के समाजवादी विचारों की हिफाजत कर पायेगा; यह दावा करना ही एक दुष्कर कार्य हो गया है।
भारत इस मंडी की गिरफ्त में आ चुका है। अक्षम्य अपराध यह है कि अद्ृश्य आर्थिक साम्राज्यवाद के दृश्य हो जाने के बावजूद हमने इसके खतरों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। खतरों को सतह पर आते देख, उनका समाधान तलाशने की बजाय, सत्ता खतरों के प्रति आगाह करने वालों को ही अप्रासंगिक बनाने में लग जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद से आज तक महात्मा गांधी का नाम लेना हम कभी नहीं भूले, लेकिन खादी के चरखे से निकले ग्राम स्वावलंबन और आत्मसंयम के गांधी निर्देश को हमने सात समंदरों की लहरों मे बहा दिया।
हमारे राजनेता भूल गये हैं कि सत्ता का व्यवहार… सत्ता के आत्मविश्वास का नाप हुआ करता है। जब कभी किसी अनुत्तरदायी सत्ता को लगता है कि यदि उसका भेद खुल गया, तो वह टिक नहीं पायेगी, तो वह दमन, षडयंत्र व आतंक का सहारा लिया करती है। आज वह समय है कि जब जनमत चाहे कुछ भी हो, लोककल्याण चाहे किसी मंे हो, सत्ता वही करेगी, जो उसे चलाने वाले आर्थिक आकाओं द्वारा निर्देशित किया जायेगा। सत्ता के कदम चाहे आगे चलकर अराजक सिद्ध हों या देश की लुट का प्रवेश द्वार… सत्ता को कोई परवाह नहीं है। विरोध होने पर वह थोङा समय ठहर चाहे जो जाये… कुछ काल बाद रूप बदलकर वह उसे फिर लागू करने की जिद् नहीं छोङती; जैसे उसने किसी को ऐसा करने का वादा कर दिया हो। भारतीय संस्कार के विपरीत यह व्यवहार आज सर्वव्यापी है। भारत की छवि आज निवेश का भूखे राष्ट्र की बनती जा रही है। भारत की वर्तमान सरकार के एजेंडे में इस भूख की पूर्ति पहली प्राथमिकता है। ऐसा लगता है कि इस बेताबी में आर्थिक साम्राज्यवाद के खतरों के प्रति सावधान होने का समय उसके पास भी नहीं है।
सत्ता-संविधान के प्रति शून्य आस्था व उदासीनता खतरनाक
बावजूद इसके सच है कि ठीकरा सिर्फ आर्थिक साम्राज्यवाद की साजिशों के सिर फोङकर नहीं बचा जा सकता। कारण और भी हैं। नरेन्द्र मोदी, सत्ता के प्रति लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, किंतु उनके विरोधाभासों के साथ-साथ यदि हम भारत के पूरे राजनैतिक परिदृश्य पर निगाह डालें, तो लोगों की निगाह में राजनीति का चरित्र अभी ही संदिग्घ ही है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक साल के बच्चे को भी दंगे को आरोपी बना सकती है। एक तरफ संविधान के रखवालों के प्रति यह अविश्वास है, तो दूसरी ओर दंगे के दागियों को सम्मानित करना सत्ता का नया चरित्र बनकर उभर रहा है। एक रुपया तनख्वाह लेने वाली मुख्यमंत्री की संपत्ति का पांच साल में बढकर 33 गुना हो जाना विश्वासघात की एक अलग मिसाल है। चित्र सिर्फ ये नहीं हैं, भारतीय राजनैतिक चित्र प्रदर्शनी ऐसे चित्रों से भरी पङी है। संविधान के प्रति दृढ आस्था का यह लोप हतप्रभ भी करता है और दुखी भी।
लोकतंत्र में नागरिकों की उम्मीदें जनसेवक व जनप्रतिनिधियों पर टिकी होती हैं। प्रधानमंत्री अपने को भले ही प्रधानसेवक कहते हों, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे जनसेवकों व जनप्रतिनिधियो ने जनजीवन से कटकर अपना एक ऐसा अलग रौबदाब व दायरा बना लिया है कि जैसे वे औरों की तरह के हांड-मास के न होकर कुछ और हों। प्रचार और विज्ञापन की नई संचार संस्कृति ने उन्हे जमीनी हकीकत व संवाद से काट दिया है। सत्ता के प्रति लोकास्था शून्य होने की यह एक बङी वजह है। एक तरह से सत्ता के प्रति जनता ”कोउ नृप होए, हमैं का हानि” के उदासीन भाव ग्रहण चुकी है। किसी भी लोकतंत्र की जीवंतता के लिए इससे अधिक खतरनाक बात कोई और नहीं हो सकती।
संस्था चाहे राजनैतिक हो या कोई और… ‘संविधान’ सत्ता के आचरण व शक्तियों के निर्धारण करने का शस्त्र हुआ करता है। जो राष्ट्र जितना प्रगतिशील होता है, उसका संविधान भी उतना ही प्रगतिशील होता है। उसका रंग-रूप भी तद्नुसार बदलता रहता है। क्या हम भारत के संविधान को प्रगतिशील की श्रेणी में रख सकते हैं ? नहीं। क्यों ? क्यों आज भी भारत को संविधान ब्रितानी हुकूमत की प्रतिच्छाया लगता है ?? हमारे संविधान की यह दुर्दशा क्यों है ? यह विचारणीय प्रश्न है।
दरअसल, भारतीय लोकतंत्र आज ऐसे विचित्र दौर से गुजर रहा है, जब यहां लगभग और हर क्षेत्र में तो विशेष शिक्षण-प्रशिक्षण-योग्यता की जरूरत होती है, राजनीति में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, विचारधारा अथवा अनुशासन की जरूरत नहीं होती। भारतीय राजनीति के पतन की इससे अधिक पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि हमारे माननीय/माननीया जिस संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं; जो विधानसभा/संसद विधान के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है, उनके विधायक/सांसद ही कभी संविधान पढने की जरूरत नहीं समझते। और तो और वे जिस पार्टी के सदस्य होते हैं, जिन आदर्शों या व्यक्तित्वों का गुणगान करते नहीं थकते, ज्यादातर उनके विचारों या लिखे-पढे से ही परिचित नहीं होते। इसीलिए हमारे राजनेता व राजनैतिक कार्यकर्ता न तो संविधान की पालना के प्रति और ना ही अपने दलों के प्रेरकों के संदेशों के अनुकरण में कोई रुचि रखते हैं। समझ सकते हैं कि क्या कारण हैं कि पार्टियां भिन्न होने के बावजूद हम कार्यकर्ताओं व राजनेताओं के चरित्र में बहुत भिन्नता नहीं पाते।
राजनैतिक अनैतिकतावाद के व्यापक दुष्प्रभाव का दौर
करीब आठ बरस पहले इतिहास ने करवट ली। जे पी की संपूर्ण क्रांति के दौर के बाद जनमानस एक बार फिर कसमसाया। वैश्विक महाशक्तियों द्वारा भारत को अपने आर्थिक साम्राज्यवाद की गिरफ्त में ले लेने की लालसा के विरुद्ध धुंआ उठा भी। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह मौका उस दौर में आया, जब बुद्धिजीवी ही नहीं, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान, पंच और गांव के आखिरी आदमी तक राजनीति के चारित्रिक गिरावट के दुष्प्रभाव की चपेट में थे। हाशिये के लोगों की बात करने वाले खुद हाशिये पर ढकेले जा रहे थे। लिहाजा, वह धुंआ न आग बन सका और न ही किसी बङे वैचारिक परिवर्तन का सबब; वह धुंआ सत्ता परिवर्तन का माध्यम बनकर रह गया।
गौर करने की बात है कि यह आचार सहिंताओं के टूटने का ही नहीं, उसके व्यापक दुष्प्रभाव का भी दौर है। जे पी ने इस बारे में कहा था – ”अज्ञात युगों से ऐसे राजनीतिज्ञ होते चले आयें हैं, जिन्होने यह प्रचारित किया है कि राजनीति में आचार नाम की कोई चीज नहीं है। पुराने युगों में यह अनैतिकवाद फिर भी राजनीति का यह खेल करने वाले एक छोटे से वर्ग से बाहर अपना दुष्प्रभाव नहीं फैला सका था। अधिसंख्य लोग राज्य के नेताओं और मंत्रियों के आचरणों से दूषित होने से बचे रहते थे। परंतु सर्वाधिकारवाद, का उदय हो जाने से यह अनैतिकतावाद विस्तार के साथ लागू होने लगा है। यह ऐसा सर्वाधिकारवाद है, जिसके भीतर नाजीवाद-फासीवाद और स्तालिनवाद सभी शामिल है। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया है।”
हालांकि भारत अभी आर्थिक विषमता और असंतुलन ऐसे चरम पर नहीं पहुंचा है कि समझ और समझौते के सभी द्वार बंद हो गये हों। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाज और सत्ता के बीच जो समझ और समझौता विकसित होता दिख रहा है, उसकी नींव भी अनैतिकता की नींव पर ही टिकी हैं – ”तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हे खैरात दूंगा।” भारत जैसे लोकतंत्र में चुनाव का मतलब बीते पांच वर्षों के कार्यों के आकलन तथा अगले पांच वर्षों के सपने को सामने रखकर निर्णय करना होना चाएि। अभी पिछले उत्त्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ने इसे युद्ध की संज्ञा देते हुए कहा – ”प्रेम और युद्ध की कोई आचार संहिता नहीं होती।’’ नजरिया सचमुच इस स्तर तक गिर गया है। जनप्रतिनिधि बनने का मतलब जनप्रतिनिधित्व नहीं, राजभोग समझ लिया गया है। जनता भी वोट का बटन दबाते वक्त यदि तमाम नैतिकताओं व उत्तरदायित्वों को ताक पर रखकर जाति, धर्म और निजी लोभ-लालच के दायरे को प्राथमिकता पर रखती है। उम्मीदवार से ज्यादा अक्सर पार्टी ही प्राथमिकता पर रहती है। इस नजरिए का ही नतीजा है कि कितनी ही भौतिक, आर्थिक व अध्यात्मिक अनैतिकताओं को आज हमने ’इतना तो चलता है’ मान लिया है। यही कारण है कि आज सत्ता अनुशासन के सारी आचार संहितायें नष्ट होती नजर आ रही हैं। यह बात कङवी जरूर है; लेकिन यदि हम अपने जेहन मंे झांककर देखे, तो आज का सच यही है।
निगाहें फिर विचार मार्ग पर
इतिहास गवाह है कि जब-जब सत्तायें गिरावट के ऐसे दौर में पहुंची हैं, हमेशा वैचारिक शक्तियों ने ही डोर संभालकर सत्ता की पतंग को अनुशासित करने का उत्तरदायित्व निभाया है। इसके लिए वह दंडित, प्रताङित व निर्वासित तक किया जाता रहा है। दलाईलामा, नेल्सन मंडेला व आंग सू ची से लेकर दुनिया के कितने ही उदाहरण अंगुलियों पर गिनाये जा सकते हैं। अतीत में सत्ता को अनुशासित करने की भूमिका में कभी गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य का गुरुभाव, कभी भीष्म का राजधर्म, कभी अयोध्या का लोकानुशासन, कभी कौटिल्य का दुर्भेद राजकवच, कभी मार्क्स-एंगेल्स का कम्युनिस्ट पार्टी घोषणापत्र…. तो कभी गांधी-विनोबा का राजनीतिक नैतिकतावाद दिखाई देता रहा है। आजाद भारत मंे यही भूमिका राममनोहर लोहिया के मुखर समाजवादी विचारों और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने निभाई।
‘राजसत्ता का अनुशासन’ नामक एक पुस्तक ने ठीक ही लिखा है कि नैतिक गिरावट के इस दौर में पुनः उत्कर्ष का रास्ता अध्यात्म और भौतिक… दोनो माध्यम से हासिल किया जा सकता है; लेकिन शर्त है कि सबसे पहले सतत् सामुदायिक संवाद के पारदर्शी मंच फिर से जीवित हों। इसके लिए नतीजे की परवाह किए बगैर वे जुटें, जिनके प्रति अभी भी लोकास्था जीवित है; जिनसे छले जाने का भय किसी को नहीं है। बगैर झंडा-बैनर के हर गांव-कस्बे में ऐसे व्यक्तित्व आज भी मौजूद है; जो लोक को आगे रखते हुए स्वयं पीछे रहकर दायित्व निर्वाह करते हैं। गङबङ वहां होती है, जहां व्यक्ति या बैनर आगे और लोक तथा लक्ष्य पीछे छूट जाता है। राष्ट्रभक्त महाजनों को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्तित्वों की तलाश कर उनके भामाशाह बन जायें।
जिस दिन ऐसे व्यक्तित्व छोटे-छोटे समुदायों को उनके भीतर की विचार और व्यवहार की नैतिकता से भर देंगे, उस दिन भारत पुनः उत्कर्ष की राह पकङ लेगा। तब तक देर न हो जाये, देश में दौलत करने वाले संसाधन व सत्ता में सुस्थिरता पैदा करने वाली लोकास्था पूरी तरह लुट न जाये, इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग की कलम व वाणी को औजार बनकर सत्याग्रह करने रहना है। ”जब तोप मुकाबिल हो, तो कलम संभालो” या कहिए कि जब तोप मुकाबिल हो, तो कलम में ढेर सारे बीज रचना के भर लो और जरूरत पङने पर सत्याग्रह की ढेर सारी बारूद। रचना और सत्याग्रह साथ-साथ चलें। यही अतीत की सीख भी है और सुंदर भविष्य की नींव भी। आइये! करें।
अरुण तिवारी