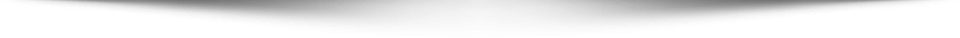पार्टिंयां चुनावों की तैयारी करती हैं। पार्टियां ही उम्मीदवार तय करती हैं। पांच साल वे क्या करेंगी; इसका घोषणापत्र भी पार्टियां ही बनाती हैं। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जायेगा; मीडिया के साथ मिलकर ये भी पार्टियां ही तय कर रही हैं। मतदान की मशीन पर चुनने के लिए छपे हुए निशान भी पािर्टंयों के ही होते हैं। मतदाता भी अपना मत, उम्मीदवार से ज्यादा, पार्टियों को ध्यान में रखकर ही देता है। यह लोकसभा के लिए लोक-प्रतिनिधि चुनने का चुनाव है कि पार्टिंयां चुनने का ? लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना है। क्या चुनाव से पूर्व कभी लोगों से पूछा जाता है, ”हां भई, आप बताइए कि किस-किस को उम्मीदवार बनाया जाए ?” सोचिए।
स्वयं से पूछिए कि इस चुनाव में चुनाव आयोग है, मतदाता है, मतदान की मशीन है; किंतु इसमें लोक कहां है ? लोक-प्रतिनिधियों का चुनाव है, तो उम्मीदवार, चुनावी प्रक्रिया, और तौर-तरीके से लेकर चुनावी एजेण्डा तक लोगों को तय करना चाहिए कि नहीं ? पार्टी-घोषणापत्र की जगह, लोक-घोषणापत्र होना चाहिए कि नहीं ? लोकसभा है, तो लोक का सभा पर नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं ? यह कहां है ? दुर्योग है कि लोकप्रतिनिधि के तौर पर चुने गये उम्मीदवार, पांच साल के दौरान जो कुछ करते हैं; हम, भारत के लोग उसमें भी अपनी कोई विशेष भूमिका अभी तक नही तलाश पाए हैं। क्या यह किसी लोकतंत्र के परिपक्व अथवा संजीदा होने के लक्षण हैं ?
यदि नहीं, तो ज़रूरत लोकतंत्र के पिरामिड को सही कोण पर खड़ा करने की है। यह संभव है। इसके पांच सूत्र हैं: लोक-उम्मीदवार, लोक-घोषणापत्र, लोक-अंकेक्षण, लोक-निगरानी और लोक-अनुशासन। इन पांच सूत्रों को व्यवहार में उतारकर लोकतंत्र को इसकी परिभाषा के अनुरूप आगे बढ़ाया जा सकता है।
लोक-उम्मीदवार
लोक-प्रतिनिधि सभाओं को दलों की दलदल से उबारने के लोकमार्ग के रूप में लोक-उम्मीदवारी को काफी अरसे से एक विकल्प के रूप में पेश किया जाता रहा है। जो तंत्र पर लोक के काबिज होने को ही बेहतरी व बदलाव का एकमेव मार्ग मानते हैं, वे भी लोक-उम्मीदवारी के विचार को उभारने के पक्षधर हैं। पार्टी उम्मीदवार, निर्दलीय व लोक उम्मीदवार में बुनियादी फर्क कई हैं। पार्टी उम्मीदवार पार्टी द्वारा तय किया जाता है। निर्दलीय उम्मीदवारी स्वेच्छा से अपनी उम्मीदवारी पेश करता है। लोक-उम्मीदवार की उम्मीदवारी उस जनता के बहुमत द्वारा तय की जाती है, जिनका उसे प्रतिनिधित्व करना है। ऐसी उम्मीदवारी के मामले में पहले से अनुबंध होता है कि लोक व उम्मीदवार दोनो एक-दूसरे के प्रति जवाबदेह होंगे। लोक-उम्मीदवार लोकप्रतिनिधि के रूप में लोक के एजेंडे को अपना एजेंडा बनायेगा। लोक के लिए किए गये कार्य की योजना, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में लोक को शामिल करेगा। लोक की उम्मीदों पर खरा न उतरने की स्थिति में लोक को हक होगा कि वह अपने द्वारा ही नामांकित-चयनित लोक-प्रतिनिधि को वापस बुला सकें।
ग्राम से लोकसभा तक इसे सच करने के रास्ते विनोबा ने भी सुझाये थे। अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रपति चुनने के तौर-तरीके को भी कोई-कोई लोक-उम्मीदवार का दर्जा दे देते हैं। आज दलों के दलदल और निर्दलीय की भी लोक के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित न होने से अजीज आ चुके मतदाताओं के एक बङे वर्ग द्वारा मतदान न किए जाने के स्थिति में लोक-उम्मीदवार का महत्व और बढ़ जाता है। दलगत व निर्दलीय उम्मीदवार उक्त चार में से एक भी शर्त को मानने को बाध्य नहीं होता। भारत में इस दिशा में कुछ प्रयोग हुए ज़रूर, लेकिन सही प्रक्रिया और पूरी ईमानदारी के अभाव में लोक-उम्मीदवार, अभी भी एक सपना ही है।
लोक-घोषणापत्र
लोक-घोषणापत्र का मतलब है, लोगों की नीतिगत तथा कार्य संबंधी जरूरत व सपने की पूर्ति के लिए स्वयं लोगों द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज। प्रत्येक ग्रामसभा / मोहल्ला समितियों को मौजूद संसाधन, सरकारी-गैरसरकारी सहयोग, आवंटित राशि तथा जनजरूरत के मुताबिक अपने इलाके के लिए अगले पांच साल के सपने का नियोजन करना चाहिए। इसे विधानसभावार, लोकसभावार व मुद्देवार तैयार करने का विकल्प खुला रखना चाहिए। इसे हर साल परिमार्जित करने का विकल्प भी खोलकर रखना अच्छा होगा। इस लोक एजेंडे या लोक नियोजन दस्तावेज को लोक-घोषणापत्र का नाम दिया जा सकता है। इस लोक-घोषणापत्र को किसी बैनर या फलेक्स पर छपवाकर अथवा सार्वजनिक मीटिंग स्थलों की दीवार पर लिखकर चुनाव प्रचार के लिए आने वाले चुनावी उम्मीदवारों के समक्ष पेश किया जा सकता है। उनसे उसकी पूर्ति के लिए संकल्पपत्र / शपथपत्र लिया जा सकता है। इससे उम्मीदवार के चयन में भी सुविधा होगी और पालन करने के लिए उम्मीदवार के सामने अगले पांच साल एक दिशा-निर्देश होगा।
लोक-अंकेक्षण
लोक-प्रतिनिधियों के बजट से क्रियान्वित होने वाली कार्यों में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए फंड का लोक अंकेक्षण यानी ‘पब्लिक-ऑडिट’ अनिवार्य हो। ऑडिट सिर्फ वित्तीय नहीं, कैग के नए विविध सूचकांकों के आधार पर होना चाहिए। इसका तरीका बहुत साधारण है। हमारे पास ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, मोहल्ला समिति, वार्ड समिति, जैसे संगठन पहले से ही मौजूद है। भिन्न-भिन्न स्तर पर उनसे नीचे के स्तर की प्रतिनिधि सभाओं द्वारा नामांकित सदस्यों की सदस्यता वाली लोक-अंकेक्षण समितियों का गठन किया जा सकता है। यह समितियां अपने लोक-प्रतिनिधि को बाध्य कर सकती हैं कि लोक-घोषणापत्र व लोक-मांग के अनुरुप बजट का आवंटन करे। वह लोक-प्रतिनिधि को कह सकती हैं कि वह प्रति तिमाही अपने खाते के बजट व कार्य का लेखा-जोखा लोक-अंकेक्षण समूह के समक्ष प्रस्तुत करे। लोक अंकेक्षण समिति के किसी भी सदस्य द्वारा मांगे जाने पर लोक-प्रतिनिधि लेखा व कार्य विवरण की रिकाॅर्ड प्रस्तुत करने को सदैव बाध्य हो।
पांच साल पूरे होने पर लोक-अंकेक्षण समूह की रिपोर्ट खुद-ब-खुद इस बात का आइना होगी कि निवर्तमान प्रत्याशी उसमें अपना चेहरा देख सके; जान सके कि वह अगली बार चुनाव लङने लायक है या नहीं। पर्टियां भी इस आधार पर अपना उम्मीदवार तय कर सकती हैं और लोग भी कि उस प्रतिनिधि को अगली बार चुना जाये या दरकिनार कर दिया जाये। पंचवर्षीय लेखा-जोखा अगले पांच वर्षीय कार्यों का नियोजन व तद्नुसार लोक-घोषणापत्र निर्माण में भी बराबर का मददगार सिद्ध होगा। यदि जनता यह जवाबदारी निभा सकी, तो तंत्र पर लोक की हकदारी स्वतः आ जायेगी। कभी यह प्रयोग करके देखना चाहिए।
लोक-निगरानी
हालांकि केन्द्र द्वारा भेजे एक सैकड़ा पैसे के नीचे तक पहुंचते-पहुंचते तीन दहाई रह जाने संबंधी राजीव गांधी के बयान की चर्चा आज भी खूब होती है, किंतु योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की कोई गंभीर कोशिश आज तक नहीं हुई। शीला दीक्षित शासनकाल में दिल्ली सरकार ने ‘जनभागीदारी’ कार्यक्रम शुरु किया था। उसकी भूमिका भी आंशिक ही थी। लोक-निगरानी इस सपने को सच करने का भी एक कारगर औजार हो सकती है और तंत्र पर नकेल कसने का भी।
योजना को ठीक से जानना-पहचाना। उसके हर पहलू पर नजर रखना। लाभार्थियों को पहले से अवगत कराना। योजना में कमी है तो टोकना। उन्हें दूर करने के लिए मजबूर करना। योजना ठीक से लागू हो; इसमें अपनी भूमिका की तलाशकर उसका निर्वाह करना। योजना के दुश्मनों को दूर करना और कर्मनिष्ठ सहायकों को मदद देना…..सम्मानित करना। समय-समय पर योजना की हकीकत को उजागर करना। ये काम अत्यंत जिम्मेदारी, सावधानी, कौशल व सातत्य की मांग करते हैं। इसके लिए लोक-निगरानी समूहों के गठन, प्रशिक्षण, कौशल विकास, संवैधानिक मान्यता व हकदारी की निर्णायक पहल समाज को स्वयं करनी चाहिए। निगरानी समूहों की आवाज सरकार में सुनी जायेगी; यह भरोसा सरकार, स्वयंसेवी जगत, पत्रकार, अदालत.. सभी को मिलकर देना चाहिए।
मैं मानता हूं कि लोक-निगरानी तंत्र जैसे-जैसे विकसित होंगे; लोकतंत्र भी विकसित होता जायेगा। अभी तंत्र आगे है, लोक पीछे। तब लोक आगे होगा; तंत्र सहायक की भूमिका में। शासन-प्रशासन जनता की सुनने को मजबूर होंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम स्वतः लग जायेगी। लोक-सहभागिता स्वतः सुनिश्चित होने लगेगी। यह आदर्श स्थिति होगी। इसकी अभी हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। हां! बीज बो सकते हैं। उसे खाद-पानी, निराई-गुडाई कर सकते हैं। बगैर चिंता किए कि क्या होगा…. शुरूआत तो करें। निश्चित जानिए कि नतीजा तो निकलेगा ही। कभी देखा यह सपना भी एक दिन सच हो ही जायेगा।
लोक-अनुशासन
व्यवस्था अपने आप में कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं होती। वह जो कुछ भी होती है, उसे बनाने व संचालित करने वालों की नीति, नीयत और क्षमता होती है। या यूं कहें कि व्यवस्था शासित या शासक के बीच का अंतर्संबंध और चालक होती है। अतः सुव्यवस्था के लिए जरूरत व्यवस्था में बदलाव की नहीं, शासित व शासक के अंतर्संबंधों में अनुशासन व एक-दूसरे के सम्मान, पोषण व रक्षण-संरक्षण की है। इस तैयारी के साथ चलने वाली कोई भी व्यवस्था सुव्यवस्था हो सकती है; फिर वह भले ही राजतांत्रिक व्यवस्था ही क्यों न हो। लोकतंत्र भी एक व्यवस्था का ही नाम है। यदि लोक की नीति, नीयत और क्षमता में दोष होगा, तो तंत्र स्वतः दोषपूर्ण हो जायेगा। यह निर्विवाद सत्य है। भारतीय लोकतंत्र में भी अब यह सत्य स्वीकारने का वक्त आ गया है।
जाहिर है कि जरूरत व्यवस्था को गाली देने की नहीं, स्वयं के सामने आइना रखकर अपने गुण-दोष निहारने की है। लोक समुदाय की मूल भारतीय संकल्पना पर निगाह डालें, तो हम पायेंगे कि यह संकल्पना भारतीय संस्कृति के दो महत्पवूर्ण पहलुओं की बुनियाद पर बुनी गई थी: सहजीवन और सहअस्तित्व। ये सांस्कृतिक पहलू जीवन विकास संबंधी डार्विन के उस वैज्ञानिक सिद्धांत को भी पुष्ट करते हैं, जो परिस्थिति के प्रतिकूल रहने पर मिट जाने और अनुकूल तथा सक्रिय रहने पर विकसित होने की बात कहता है। लाॅर्ड मेटकाफ की नजरों में समुदाय होकर ही भारत का गांव समाज सदियों तक ऐसी परिस्थितियों में भी टिका रहा, जिन परिस्थितियों में दूसरी हर वस्तु.. व्यवस्था का अस्तित्व मिट जाता है। स्पष्ट है कि यदि तंत्र व लोक को भी एक-दूसरे का अस्तित्व मिटाये बगैर एक साथ बने रहना है तो एक-दूसरे को चुनौती देने की बजाय एक दूसरे के साथ सहजीवन व सहअस्तित्व का भाव बनाना होगा। ऐसा तभी संभव है, जबकि तंत्र व उसे सर्जित व संचालित करने वाला लोकसमुदाय… दोनो स्वानुशासित हों। भारत का इतिहास इस बात को और पुख्ता तरीके से प्रमाणित करता है।
वैदिक काल में विशः ऐसी समिति थी, जो राजा तक का चुनाव करती थी। इसी समिति के माध्यम से प्रत्येक गांव में एक नेता चुना जाता था। उसे ‘ग्रामणी’ कहा जाता था। प्रत्येक गांव एक छोटा सा स्वायत्त राज्य था। स्वायत्त होने के बावजूद यह व्यवस्था अराजक नहीं थी। क्यों ? क्योंकि राजा व गांव एक-दूसरे की सत्ता को चुनौती देने की बजाय एक-दूसरे के पोषक और रक्षक की भूमिका में थे। एक मां तो दूसरा संतान। जहां राजा का पद वंशानुगत होता था; वहां भी राजा को आर्य नियमों के विरुद्ध जाने नहीं दिया जाता था। वाल्मीकि रामायण में गणराज्यों और उनके मेल से बने संघों का वर्णन है। रामायण कालीन राज्य सभा में सर्वाधिक शक्तिशाली अंग ‘पौर जनपद’ था। पौर जनपद में राजधानी के नैगम और गण्वल्लभ तथा ग्रामप्रांत के ग्रामघोष, महत्तर और समविष्ट होते थे। जनाक्षेप के आधार पर राजा राम द्वारा सीता के परित्याग का कथानक प्रमाण हैं कि गांव समितियों का हस्तक्षेप तब राज्यसभा तक था। किंतु इसके उलट राजा ने कभी ग्रामीण संस्थाओं के कार्य में अपनी ओर से हस्तक्षेप नहीं किया। बावजूद इसके लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करते थे। मौर्यकालीन व्यवस्था इसका अनुपम उदाहरण है। कालांतर में जब कभी संतान अपने कर्तव्य से च्युत हुई तो उन्हे अनुशासित करने के लिए मां ने डांट भी पिलाई। लेकिन यह तंत्र व लोक के बीच का असल व आदर्श रिश्ता मां और संतान का है; यह तथ्य निर्विवाद रहा। आज भी है।
लेखक: अरुण तिवारी