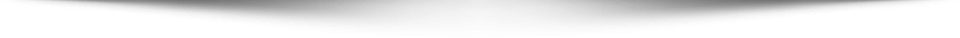सत्रहवीं लोकसभा चुनावों का विपक्ष को संकेत
सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद भारतीय राजनीति की अपनी-अपनी तरह से व्याख्या की जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के उभरने की संभावना अब और क्षीण हो गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल सेक्युलर और इंडियन नेशनल लोकदल जैसे पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों के दिन बीत रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक क्षितिज से वामपंथ की विदाई हो चुकी है। जब भी किसी खास विचारधारा और राजनीतिक दल की चुनावों में जीत होती है तो उसके बरक्स हारने वाली पार्टियों की ऐसी ही व्याख्याएं होती हैं। ऐसे विश्लेषणों का फौरी राजनीतिक संदर्भों का ज्यादा प्रभाव होता है। ऐसी व्याख्याएं करने वाले राजनीतिक पंडित भूल जाते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में राजनीति सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है राजनीतिक विचारधारा और उसके अलंबरदारों का लगातार बने रहना होता है। क्योंकि पता नहीं कब अनुभव का नया आयाम खुल जाए, जो उसके लिए बंद होती अंधेरी सुरंग में नई रोशनी की किरण दिखा दे। इस रोशनी के आलोक में विचारधारा और राजनीतिक हस्ती खुद को आइने में ईमानदारी से देख ले तो उसे नई राह सूझ सकती है। मौजूदा राजनीतिक हालात को इस सोच के आलोक में परखने की ज्यादा जरूरत है।
सबसे पहले पारिवारिक लिमिटेड पार्टियों की विदाई की अवधारणा पर विचार करते हैं। यह सच है कि बिहार के प्रथम राजनीतिक परिवार की हैसियत हासिल कर चुके लालू के कुनबे को इन चुनावों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल के उभार के बाद यह पहला मौका है, जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में उसकी नुमांइदगी करने वाला कोई नहीं रहेगा। लालू यादव की बेटी मीसा यादव पाटलिपुत्र सीट से हार चुकी हैं। संसदीय चुनाव में यह उनकी लगातार दूसरी हार है। लालू परिवार की तरह पड़ोस के उत्तर प्रदेश के प्रथम परिवार माने जाने वाले मुलायम के कुनबे की वैसी हालत नहीं हुई है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले उनके परिवार के तीन सदस्य खेत रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश ही संसद पहुंचने में कामयाब रहे हैं। हालांकि उनके तीन और साथी लोकसभा की राह पकडऩे में कामयाब रहे हैं। पंजाब में अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर भी संसद पहुंचने में कामयाब रही हैं। लेकिन दक्षिण भारत की ओर निगाह डालने पर पारिवारिक राजनीति की विदाई की अवधारणा चकनाचूर हो जाती है। आंध्र प्रदेश में नंदमुरि तारक रामाराव का परिवार, जिसकी नुमाइंदगी चंद्रबाबू नायडू करते हैं, बेशक खेत रहे। लेकिन जिन्होंने बाबू को राजनीति में किनारे लगाया है, वे जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। उनकी वाईएसआर कांग्रेस भी एक तरह से वंशवाद और परिवारवाद का ही विस्तार ही है। आंध्र के सहोदर राज्य तेलंगाना की शासक पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति भी एक तरह से पारिवारिक लिमिटेड पार्टी ही है। पिछली लोकसभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता सांसद थीं, लेकिन मौजूदा चुनावों में निजामाबाद सीट से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन तमिलनाडु में एक और पारिवारिक लिमिटेड पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम् ने भारी जीत हासिल की है। करूणानिधि परिवार ने राज्य की 23 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। कर्नाटक में बेशक पारिवारिक लिमिटेड पार्टी जनता दल सेक्युलर के अलंबरदारों को हारना पड़ा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता की पारिवारिक पार्टी को भले ही चोट पहुंची है, लेकिन उनके भतीजे जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रभावी बहुजन समाज पार्टी को कुछ महीनों पहले तक एकाधिकारवादी पार्टी माना तो जाता था, लेकिन वह पारिवारिक लिमिटेड पार्टी नहीं समझी जाती थी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर उभारना शुरू किया है, उससे साफ है कि वह भी पारिवारिक लिमिटेड पार्टी की ओर बढ़ चली है। इन चुनावों में उसे दस सीटों पर जीत मिली है।
ये मिश्रित नतीजे इस अवधारणा को झुठलाते हैं कि पारिवारिक लिमिटेड पार्टियों की विदाई का वक्त आ गया है। एक तरफ जनता ने कुछ पारिवारिक लिमिटेड राजनीतिक दलों को अंगूठा दिखाया है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दलों को भारी जीत से नवाजा है। चूंकि भारत विविधताओं वाला देश है, राष्ट्रीयता की अवधारणा को छोड़ दें तो पूरा देश एक तरह की सोच कम ही मुद्दों पर रखता है। इसलिए यह मान लेना की पारिवारिक पार्टियों की विदाई हो गई, जल्दबाजी ही कही जाएगी। पारिवारिक दलों की विदाई तब मानी जाती, जब उनका पूरे देश से खात्मा होता। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश की किस्मत का फैसला अगले पांच साल तक पारिवारिक लिमिटेड पार्टी ही करने जा रही है। विपक्षी राजनीति में डीएमके जैसी पारिवारिक पार्टी भी अहम भूमिका निभाने की तैयारी में है। बहरहाल इतना कहा जा सकता है कि जनता ने कुछ बड़बोले परिवारों को नकार कर यह संदेश जरूर दिया है कि उसके लिए जातीय और पारिवारिक सम्मान की बजाय विकास चाहिए, उसके बुनियादी मसलों को सुलझाने वाली विचारधारा वाले लोग चाहिए। जनता ने ऐसा करके यह संकेत दिया है कि पारिवारिक गौरव के नाम पर उसकी भावनाओं के साथ अब खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और उसकी संजीदगी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।
भारत में किसी भी दल की जीत हो, प्रधानमंत्री कोई रहे, लेकिन देश पर करीब 36 साल तक प्रत्यक्ष और दस साल तक परोक्ष शासन करने वाले गांधी-नेहरू परिवार को प्रथम राजनीतिक परिवार होने का गौरव हासिल है। लेकिन उसे भी भारतीय जनता ने इस बार झटका दिया है। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर ग्यारह बार से कांग्रेस लगातार प्रतिनिधित्व करती रही जिसमें नौ बार तो नुमाइंदगी गांधी-नेहरू परिवार की ही रही। लेकिन इस बार वहां की जनता ने उस परिवार के चश्म-ए-चिराग राहुल गांधी को नकार दिया। यह नकार बड़ी बाकी अस्वीकारणों में कहीं ज्यादा गंभीर है। इसलिए कि राहुल गांधी महज गांधी-नेहरू परिवार के सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से निकली देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसलिए अमेठी में उनकी हार को एक हद तक इस परिवार की विदाई के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है।
साल 2014 के आम चुनावों में बेशक कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ नहीं थी। उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। लेकिन देश राहुल गांधी को ही अगुवा मान रहा था। इस लिहाज से देखा जाए तो पिछला चुनाव परोक्ष तौर पर राहुल गांधी की अगुवाई में ही लड़ा गया। तब चुनावी राजनीति के इतिहास में कांग्रेस की सबसे बुरी हालत रही। लोकसभा में उसके 44 सांसद ही पहुंच पाए थे। 2019 का चुनाव प्रत्यक्षत: राहुल गांधी की ही अगुवाई में लड़ा गया है। उन्होंने लगातार एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले जारी रखे। कई बार उन्होंने बड़बोलापन भी दिखाया। चुनावों के आखिरी दिन यानी 19 मई को उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के निकलने-भागने के हमने सब रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन चार दिन बाद आए नतीजों ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी पहले से कहीं और ज्यादा मजबूत होकर उभरे और राहुल गांधी का ऐलान सिर्फ बड़बोलापन ही था। पिछली बार की बजाय उनकी पार्टी की सात सीटें बेशक बढ़ गईं। लेकिन उनका करिश्मा फेल नजर आया। यह तब हालत है, जब उन्होंने पिछले साल नवंबर के चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता छीन ली थी। उसके पहले कर्नाटक में राजनीतिक दांव मारकर कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की सरकार बनवा दी थी। गुजरात के विधानसभा चुनावों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भी दी। ऐसे में उनसे मौजूदा चुनावों में बेहतर नतीजों की उम्मीद थी। लेकिन देश ने उन उम्मीदों को धो दिया। इसके अपवाद केरल और पंजाब जैसे राज्य रहे।
ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब विपक्ष की राजनीति क्या होगी? इन पंक्तियों के लेखक को लगता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बीच सिरफुटौव्वल होना शुरू होगा। महागठबंधन का जितना फायदा मायावती उठाने में कामयाब रही हैं, उतना समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाया है। वैसे भी इस गठबंधन पर अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पहले ही दिन ही उठा चुके थे। अब हताश कार्यकर्ता सवाल जरूर उठाएंगे कि आखिर ऐसा बेमेल गठबंधन क्यों किया गया? इसलिए अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग अलग-अलग राय जाहिर करते नजर आएं तो हैरत नहीं होनी चाहिए। एक दौर में लालू और मुलायम के सबसे बड़े पैरवीकार वामपंथी दल हुआ करते थे। उन्हें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की कथित सांप्रदायिक राजनीति को ये ही रोक सकते हैं। इसलिए वामपंथी दलों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में इन्हीं दलों के हाथों अपने खात्मे के बावजूद इनके नेताओं को ही समर्थन दिया। लेकिन इन दलों के नेता आम जन की आकांक्षा को पूरा करने में नाकाम रहे। बिल्कुल निम्न मध्य वर्गीय परिवारों से उभर कर आने वाले इन दलों के नेता हजारों करोड़ के खुद मालिक बनते चले गये। एक दौर तक जनता इन्हें अपना रहनुमा मानती रही। लेकिन बाद में उसे समझ में आने लगा कि उसकी हैसियत वहीं की वहीं है तो उसका मोहभंग होना शुरू हो गया। इसका नतीजा सामने है। ऐसी ही सोच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर भी लोगों की होती जा रही है। बहरहाल सर्वहारा के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करने वाले वामपंथी दल भी अप्रासंगिक होते चले गए। सर्वहारा को भी लगने लगा कि भारतीय वामपंथी राजनीति विचारों से चाहे जितनी भी मजबूत हो, लेकिन वह सर्वहारा के हितैषियों की बजाय तुष्टिकरण समर्थकों के साथ है। इसलिए उसने वामपंथ को भी नकारना शुरू कर दिया। मौजूदा चुनाव नतीजों के बाद महज पांच सीटों पर सिमटना उनके लिए बड़ा संकेत है। वामपंथ को भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी अवधारणा को नकारने की भी कीमत चुकानी पड़ी है। भारतीय राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले विचारों को प्रश्रय देने का खामियाजा वह लगातार भुगत रही है। लेकिन वह अपने अंदर सुधार की राह भी नहीं देख रही। इसलिए वह इतिहास के कूड़ेदान की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए एक बात गंभीरता से स्वीकार की जा सकती है कि अगले कुछ सालों में वामपंथ बीते दिनों की बात होगी। यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। कांग्रेस को भी सोचना होगा कि वह राष्ट्रवादी सांस्कृतिक धारा के विपरीत जाएगी तो उसे ही नकार का सामना करना पड़ेगा। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने जिस तरह घर-परिवार विहीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए, वह उसे उलटा ही पड़ा। राहुल गांधी ने जिस तरह अपने वामपंथी सलाहकार की सलाह पर राष्ट्र और संस्कृति विरोधी विचारों का खुलेआम समर्थन किया, उसे भारतीय राष्ट्र राज्य की अधिसंख्य जनता ने नकारा है। चौदह राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पचास फीसद से ज्यादा वोट मिलना यही संकेत देता है। अगर कांग्रेस को भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है और अपने ऐतिहासिक गौरव को बरकरार रखना है तो उसे अपने वैचारिक आधार को लेकर मंथन करना होगा। उसे भी अब नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित जाति की नई अवधारणा गरीब को केंद्र में रखकर अपनी भावी राजनीति तय करनी होगी। अगर कांग्रेस ऐसा करने में नाकाम रहती है तो फिर वह धीरे-धीरे वामपंथ की तरह बीते दिनों की बात होती चली जाएगी।
भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में बिहार का गंभीर अवदान रहा है। लेकिन वहां जिस तरह जातिवाद की बुनियाद पर राजनीति होती रही है, उसे इस बार जनता ने नकार दिया है। पौने पांच साल नरेंद्र मोदी की सरकार में गंभीर नेता बने रहे उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर बड़बोले और अहमक हो गए थे। उन्हें सारी राजनीति अपनी कुशवाहा-कोईरी बिरादरी में ही नजर आती थी। लेकिन उनका दुर्भाग्य देखिए कि उन्हें उनकी ही जाति ने नकार दिया। अब जनता को विकास चाहिए, अपनी हालत में परिष्कार चाहिए, जाति उसके लिए अब प्राथमिक नहीं रह गई। इस वजह से अब विपक्ष को भी सोचना होगा।
इन चुनावों ने जातिवादी, परिवारवादी राजनीतिक दलों को संकेत दिया है कि सुधरो, जाति और परिवार से आगे बढ़ो, नौकरशाही पर लगाम रखो, जनता तक योजनाएं पहुंचाकर उसकी हालत सुधारो, अन्यथा व्यापक जन-नकार के लिए तैयार रहो। भारतीय जनतंत्र में अब जाति और परिवार को तवज्जो देने वालों की खैर नहीं होगी।
उमेश चतुर्वेदी