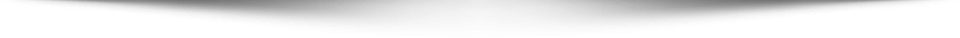कल पटना से दिल्ली की ओर बढ़े तो सोचा कि क्यों न कुछ दर्शनीय स्थानों को देखते चलें। एक-दो वरिष्ठ रिश्तेदारों और बिहार में पोस्टेड दोस्तों से सलाह ली; बिहार का नक्शा उठाया और अपने भीतर के कोलंबस को जगाकर रास्ता निर्धारित किया। योजना बनी कि पहले दिन नालंदा, पावापुरी, राजगीर, गहलौर और बोधगया को कवर किया जाए। वक़्त की कमी के चलते पावापुरी और गहलौर ठीक से नहीं देख पाए, पर बाकी तीन जगहों को ठीक से ‘जिया’।
पहला पड़ाव था- नालंदा। मेरे मन में उसकी छवि यही थी कि वह गुप्त काल में विकसित हुआ एक शानदार विश्वविद्यालय था जिसमें पढ़ने की आकांक्षा लेकर देश-विदेश के बड़े-बड़े जिज्ञासु और शोधार्थी खिंचे चले आते थे। एक बात और सुनी हुई थी कि जब बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट करने के लिये इसकी लाइब्रेरी में आग लगाई थी तो करीब 6 महीनों तक आग जलती रही थी। दंतकथाओं में अक्सर अतिशयोक्तियाँ शामिल हो जाती हैं – इस तर्क से 6 महीनों वाली बात को तथ्य न मानें तो भी इतना तो मान ही सकते हैं कि यहाँ एक अत्यंत समृद्ध पुस्तकालय रहा होगा।
खैर, हम लोग इसी कच्ची-पक्की समझ के साथ नालंदा पहुँचे। वहाँ पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने एक बोर्ड पर नालंदा से जुड़ी बुनियादी जानकारियाँ प्रकाशित की हुई हैं। उस बोर्ड को पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस पर कुछ दार्शनिकों/चिंतकों के नाम लिखे थे जिन्होंने नालंदा में रहकर अध्ययन या अध्यापन कार्य किया था। उस सूची में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु और असंग जैसे महान आचार्यों के नाम पढ़कर मन विह्वल हो गया। अज्ञेय की सिद्ध-कविता ‘असाध्यवीणा’ से एक पंक्ति उधार लेकर कहूँ तो “ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है”…
कहानी कुछ यूँ है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी हीनयान और महायान में बँट गए थे। हीनयान बुद्ध के विचारों के नज़दीक था पर अपनी कठिन मान्यताओं (जैसे निरीश्वरवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, निर्वाण की अभावात्मक धारणा और अर्हत) के कारण लोकहृदय में रस उत्पन्न करने में असमर्थ था। हिंदू परंपरा के लोग भी उसे अपनाने में बहुत सहजता महसूस नहीं करते थे क्योंकि यह उनकी परंपरागत धारणाओं से काफी दूर था। इस संकट को दूर करने के लिये बौद्ध परंपरा में महायान की शुरुआत हुई जो आसान और रसपूर्ण रास्ता तो था ही; साथ ही कई वैदिक तथा औपनिषदिक धारणाओं के समावेशन के कारण हिंदू समाज के लिये सुग्राह्य भी था। इस मुश्किल काम को जिन आचार्यों ने अंजाम दिया, लगभग वे सारे नालंदा से ही जुड़े थे। यह महत्कार्य इसी विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ था।
नागार्जुन, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे, अपने शिष्य आर्यदेव के साथ महायान की अत्यंत प्रसिद्ध शाखा माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक थे। शून्यवाद के सटीक अर्थ विनिश्चयन में बहुत वाद-विवाद हुए हैं। अब लगभग सहमति है कि ‘शून्यता’ का अर्थ ‘निषेध’ या ‘निहिलिज़्म’ नहीं बल्कि ‘अवर्णनीयता’ या ‘अनिर्वचनीयता’ है। नागार्जुन के ही शब्दों में कहूँ तो यह जगत और पारमार्थिक सत्य दोनों अलग-अलग कारणों से अनिर्वचनीय अर्थात शून्य हैं। जगत एक सामूहिक तथा विराट भ्रम है जिसका मिथ्यात्व परमार्थ का बोध होने पर ही होता है।
सच कहूँ तो नागार्जुन की वैचारिकी भारतीय अमूर्त विचारणा का चरम स्तर है; जिसे हीगेल, फिक्टे और शेलिंग की महान जर्मन परंपरा भी ठोस चुनौती नहीं दे पाती। ब्राह्मणवादी तथा वेदांत-समर्थक दार्शनिक शंकराचार्य के पक्ष में चाहे जितने भी तर्क जुटा लें, इस सच को झुठलाना संभव नहीं है कि शंकर के दर्शन का बुनियादी ढाँचा ठीक वही है जो नागार्जुन उनसे करीब 600 वर्ष पहले प्रस्तावित कर चुके थे। इसे सिर्फ संयोग कहकर टालना शुतुरमुर्गी मुद्रा है, कुछ और नहीं। सच यही है कि शंकर इस परिप्रेक्ष्य में ‘प्रच्छन्न बौद्ध’ ठहरते हैं।
महायान की दूसरी महान परंपरा ‘योगाचार विज्ञानवाद’ भी नालंदा में ही विकसित हुई। आचार्य असंग और वसुबंधु, जो आपस में अर्ध-भ्राता भी थे, एक साथ नालंदा में रहकर इस मौलिक वैचारिकी को धार दे रहे थे। उन्होंने नागार्जुन से आगे बढ़कर यह कल्पना की कि वास्तविक जगत जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हम अनुभव में सिर्फ अनुभूत-विज्ञानों को ही जानते हैं और उनके आधार पर वस्तुजगत की कपोल कल्पना कर लेते हैं। यह दर्शन लोक-अनुभवों की आसान समझ को ख़ारिज करने के कारण विश्वास का कम, कौतूहल का विषय ज़्यादा रहा है। मैं तो इसलिये इससे इतना प्रभावित हूँ कि अगर यह न होता तो हम पश्चिम के बर्कले और लाइबनिज़ जैसे प्रत्ययवादी दार्शनिकों की टक्कर में अपना कोई विचार न रख पाते। पश्चिमी दर्शन के सम्राट ‘कांट’ का ‘अज्ञेयवाद’ हो या एडमंड हुस्सर्ल का ‘संवृत्तिवाद’, हम ‘विज्ञानवाद’ के सहारे सभी को गहराई के मामले में स्पर्धा दे सकते हैं।
अब आप सोचिये कि जब मुझे पता चला होगा कि ये सारे महान आचार्य इस जगह व्याख्यान देते थे; यहाँ बैठते/घूमते थे और इस प्रस्तर-भवन में रहते थे तो मुझ पर क्या गुज़री होगी? एक बार वर्धा में एक संग्रहालय में बताया गया कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उस पर कभी महात्मा गांधी बैठते थे। इतना सुनते ही करंट सा लगा था और फिर उस पर बैठने का साहस नहीं हुआ था। यही हाल निराला, वर्ड्सवर्थ और ग़ालिब के मकानों में लिपटी उनकी यादों को महसूस करते हुए हुआ था।
इसी भाव-बिंदु पर नालंदा के मौन पत्थरों को हौले से थपथपाकर शुक्रिया कह आया हूँ…