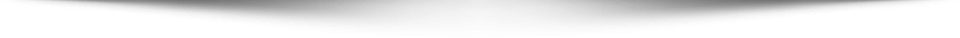-बलबीर पुंज
एक हालिया प्रेसवार्ता में पत्रकार के एक प्रश्न पर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने अपना आपा खो दिया। आपराधिक मानहानि मामले में अदालत से दो वर्षीय सज़ा मिलते ही अपनी सांसदी निरस्त होने और इसपर जारी राजनीति को लेकर राहुल से, वर्षों से कांग्रेस कवर कर रहे टीवी-पत्रकार ने प्रश्न किया— “मोदी-उपनाम पर उनकी टिप्पणी को भाजपा ‘ओबीसी का अपमान’ बता रही है।” इसपर झुंझलाकर राहुल ने कह दिया, “…आप… बीजेपी का सिंबल सीने पर लगा लीजिए, तब मैं आपको उसी के अनुसार जवाब दूंगा। पत्रकार होने का ढोंग मत कीजिए।” इसके बाद थोड़ा ठहरकर राहुल ने कहा, “हवा निकल गई”। सार्वजनिक रूप से राहुल द्वारा इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार, कोई पहला मामला नहीं है।
सुधी पाठकों को स्मरण होगा कि कैसे सितंबर 2013 में राहुल ने कांग्रेसी प्रेसवार्ता में अचानक पहुंचकर अपनी ही सरकार द्वारा पारित एक अध्यादेश को बतौर सांसद फाड़कर फेंक दिया था। इससे असहज और अपमानित तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की सरकार को वह अध्यादेश वापस लेना पड़ा। राहुल का यही बर्ताव उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। यदि राहुल तब स्वयं पर नियंत्रण रखते, अध्यादेश नहीं फाड़ते, तो शायद वे आज लोकसभा से अयोग्य घोषित नहीं होते। इसी प्रकार, तथ्यों की अवहेलना करके राहुल द्वारा अक्सर स्वातंत्र्यवीर सावरकर को गरियाना और सहयोगी शिवसेना की घुड़की से दवाब में आकर एकाएक इसपर चुप्पी साध लेना— उनकी राजनीतिक परिपक्वता और हड़बड़ाहट को भी रेखांकित करता है। आखिर राहुल गांधी ऐसे क्यों है और उन्हें बार-बार गुस्सा क्यों आता है?
नेहरू-गांधी वंश से आने के कारण राहुल गांधी, उस रुग्ण ‘विशेषाधिकार की भावना’ (Sense of Entitlement) से जकड़े हुए है, जिसमें उनका मानना है कि विचार रखने का ‘दैवीय अधिकार’ केवल उन्हीं के पास है और वे अपने अनुकूल ‘लोक’ और ‘तंत्र’ (मीडिया-न्यायालय सहित) को चला सकते है। जब ऐसा नहीं होता, तब उन्हें लोकतंत्र संकट में दिखता है। इसी चिंतन से प्रेरित होकर जिस रोब से वर्ष 2019 की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए ‘मोदी-उपनाम’ के सभी लोगों को चोर बता दिया था, ठीक उसी ठसक से राहुल ने पत्रकार का अपमान कर दिया।
यह गुस्सा कोई 9 दिन या 9 वर्ष पुराना नहीं है। मीडिया, विशेषकर अंग्रेजी मीडिया दशकों से भारतीय राजनीतिक दलों को अपनी बौद्धिकता के अनुरूप ‘सेकुलर’ (पंथनिरपेक्षी), ‘कम्युनल’ (सांप्रदायिक), ‘लेफ्ट-लिबरल’ (वाम-उदारवादी) और ‘राइट-नेशनलिस्ट’ (दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी) आदि खांचों में उतारकर वर्गीकृत कर रहा है। इसी कारण भारतीय जनसंघ (अब भारतीय जनता पार्टी) के साथ नवंबर 2019 से पहले तक शिवसेना आदि को ‘सांप्रदायिक’ कहकर संबोधित किया गया, तो कांग्रेस या कालांतर में उससे टूटकर बनी पार्टियों और कई क्षत्रपों के साथ उन वामपंथी दलों को ‘सेकुलर’ उपाधि दे दी, जिसने मजहब के नाम पर जिहादियों-ब्रितानियों की सहायता करते हुए भारत के रक्तरंजित विभाजन और पाकिस्तान के जन्म में महती भूमिका निभाई थी।
यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता पश्चात पं.नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पार्टी में शामिल करके उन नेताओं को ‘सेकुलर’ घोषित कर दिया, जो न केवल स्वतंत्रता से पहले भारत को 15 से अधिक हिस्सों में तोड़ने हेतु आंदोलित थे, अपितु अधूरे एजेंडे की पूर्ति हेतु विभाजन के बाद खंडित भारत में ही रुक गए। इसी विरोधाभास के गर्भ से एक विशेष मीडिया संस्कृति’ का जन्म हुआ, जिसका विचार-वित्तपोषण उसी स्वघोषित ‘सेकुलर’ सत्ता अधिष्ठान की ‘गोदी’ में हुआ।
टीवी मीडिया पर 1990 के दशक तक सरकारी नियंत्रण था, जबकि समाचारपत्र इससे लगभग मुक्त रहा। तब अखबारों द्वारा नीतिगत निर्णयों और मंत्रियों-जनप्रतिनिधियों के कदाचारों आदि की आलोचना होती थी। किंतु जब भी पं.नेहरू के ‘सेकुलरवाद’, वामपंथियों और जिहादियों द्वारा संकलित ‘वैचारिक अधिष्ठान’ पर प्रश्न उठता, तो इसके ‘अपराधी’ को ‘अमेरिकी पिट्ठू’, ‘पूंजीपतियों का दलाल’, ‘सांप्रदायिक’, ‘फिरकापरस्त’ आदि विशेषणों से नवाज दिया जाता। यहां तक, पाकिस्तान को बनाने वाली ‘काफिर-कुफ्र’ अवधारणा के खिलाफ लिखने/बोलने वाले को ‘युद्ध-उन्मादी’ या ‘नफरत फैलाने वाला’ बता दिया जाता।
वैचारिक-विरोधियों के प्रति असहिष्णुता कितनी गहरी थी, यह वर्ष 2002 के गुजरात दंगा मामले से स्पष्ट है। 27 फरवरी 2002 को मजहबी उन्मादी भीड़ ने अयोध्या से ट्रेन में लौट रहे 59 कारसेवकों को गोधरा स्टेशन के निकट जीवित जलाकर मार दिया था। इस नृशंस घटना की प्रतिक्रियास्वरूप गुजरात में दंगे भड़के, जिसमें दोनों पक्ष प्रभावित हुए। तब ‘सेकुलर-वाम-जिहादी गठजोड़’ (मीडिया के एक वर्ग सहित) ने गोधरा हत्याकांड को प्रोत्साहित करने वाली मानसिकता को छिपाने हेतु प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री (वर्तमान प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी को निरंतर निशाने पर लिया और हिंदू समाज का दानवीकरण कर दिया।
यह कोई पहली या आखिरी घटना नहीं थी। जब मुंबई 1993 में 12 श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों से दहल उठी, जिसमें 257 निरपराध मारे गए थे— तब महाराष्ट्र के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री शरद पवार ने इस आतंकवादी हमले को प्रेरित करने वाली मानसिकता और षड़यंत्रकर्ताओं की मजहबी पहचान से ध्यान भटकाने हेतु मीडिया की सहायता से यह झूठ गढ़ दिया कि 13वां धमाका मुस्लिम बहुल मस्जिद-बंदर के पास भी हुआ था। वस्तुत: यह तथ्यों को क्षत-विक्षत करके हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने का पहला प्रयास था। इस परिपाटी को संप्रगकाल (2004-14) में कांग्रेसी नेता पी.चिंदबरम और सुशील कुमार शिंदे ने केंद्रीय गृहमंत्री रहते हुए आगे बढ़ाया। इसमें दिग्विजय सिंह ने मुंबई के भीषण 26/11 आतंकवादी हमले का आरोप संघ पर लगाकर पाकिस्तान को ही क्लीन-चिट दे दी।
बीते नौ वर्षों से भारतीय शासन-व्यवस्था भले ही उपरोक्त रूग्ण विचारधारा से मुक्त हो, किंतु उसके रक्तबीज आज भी शैक्षणिक, बौद्धिक, साहित्यिक, नौकरशाही, आर्थिक और पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में न केवल सक्रिय है, अपितु बहुत हद तक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते है। चूंकि मई 2014 से दशकों पुराने एकतरफा वैचारिक विमर्श को चुनौती मिल रही है, देश गुलाम मानसिकता से बाहर निकल रहा है और ‘वाम-सेकुलर-जिहादी’ कुनबे द्वारा निर्धारित ‘रेखा’ को लांघकर सभी विषयों पर दूसरा पक्ष भी जनता के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, इससे राहुल गांधी को गुस्सा आना और उनके जमात का हतप्रभ होना— समझ में आता है।
लेखक वरिष्ठ स्तंभकार, पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय-उपाध्यक्ष हैं