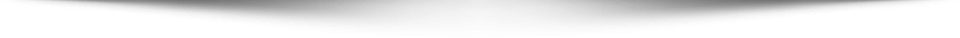भगवान महावीर: भारतीय संस्कृति का सूरज
-ललित गर्ग-
प्रत्येक वर्ष हम भगवान महावीर की जन्म-जयन्ती मनाते हैं। महावीर जयन्ती मनाने का अर्थ है महावीर के उपदेशों को जीवन में धारण करने के लिये संकल्पित होना, महावीर बनने की तैयारी करते हुए देश एवं दुनिया में अहिंसा, शांति, करूणा, प्रेम, सह-जीवन को साकार करना। शांतिपपूर्ण, उन्नत एवं संतुलित समाज निर्माण के लिए जरूरी है महावीर के बताये मार्ग पर चलना। सफल एवं सार्थक जीवन के लिये महावीर-सी गुणात्मकता को जन-जन में स्थापित करना। कोरा उपदेश तक महावीर को सीमित न बनाएं, बल्कि महावीर को जीवन का हिस्सा बनाएं, जीवन में ढालें। भगवान महावीर एक युग प्रवर्तक, कालजयी महापुरुष थे। उन्होंने एक क्रांति द्रष्टा के रूप में मानवजाति के हृदय में नवीन चेतना का संचार अपने जीवन-अनुभवों, उपदेशों, शिक्षा और सिद्धांतों के द्वारा किया। भगवान महावीर सामाजिक क्रांति के शिखर पुरुष थे, वे भारतीय संस्कृति का सूरज हैं। महावीर का दर्शन अहिंसा, शांति और समता का ही दर्शन नहीं है बल्कि क्रांति का दर्शन है। व्यक्तिगत एवं समााजिक क्रांति के संदर्भ में उनका जो अवदान है, उसे उजागर करना वर्तमान युग की बड़ी अपेक्षा है। ऐसा करके ही हम दुनिया में युद्ध, हिंसा, आतंक, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तनाव को समाप्त कर एक उन्नत, शांतिपूर्ण, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे।

महावीर जन्म से ही अतीन्द्रिय ज्ञानी थे। उन्होंने कहा तुम जो भी करते हो- अच्छा या बुरा, उसके परिणामों के तुम खुद ही जिम्मेदार हो। अपने ज्ञान से उन्होंने प्राणी मात्र में चैतन्य की धारा प्रवाहित की। अक्सर वे कहा करते थे- सुख-दुख के तुम स्वयं सर्जक हो। भाग्य तुम्हारा हस्ताक्षर है। मां को फूलों से सजते देख धीरे से बोल उठे-मां! देखो ये फूल रो रहे हैं। उन्होंने लहलहाती दूब पर चलने की मां की मनुहार को भी ठुकरा दिया। मां! इस दूर्वा की सिसकियां मेरे प्राणों में सिहरन पैदा कर रही हैं। मैं भला कैसे अपने पैरों से रौंदने का साहस करूं? क्षणिक स्पर्श सुख के लिए किसी को परितापित करना क्या उचित है मां? उनकी करुणा एवं सूक्ष्म अहिंसा के सामने मां मौन थी। मन ही मन अपने लाडले की महानता के सामने नत थी। कभी किसी निरपराध अभावग्रस्त व्यक्ति की दासता उनके कोमल दिल को कचोट जाती तो कहीं अहं और दर्प में मदहोश सत्तासीन व्यक्तियों का निर्दयतापूर्ण क्रूर व्यवहार उनके मृदु मानस को आहत कर देता। महावीर घण्टों-घण्टों तक इन समस्याओं का समाधान पाने चिंतन की डुबकियों में खो जाते। तीस वर्ष की युवावस्था में सहज रूप से प्राप्त सत्ता वैभव और परिवार को सर्प कंचुकीवत् छोड़ साधना के दुष्कर मार्ग पर सत्य की उपलब्धि के लिए दृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े। साधिक बारह वर्ष तक शरीर को भुला अधिक से अधिक चैतन्य के इर्द-गिर्द आपकी यात्र चलती रही। ध्यान की अतल गहराइयों में डुबकयिां लगाते हुए सत्य सूर्य का साक्षात्कार हुआ। वे जिस दिन सर्वज्ञ व सर्वदर्शी बन गये वह पावन दिन था वैशाख शुक्ला दशमी।
महावीर ने आकांक्षाओं के सीमाकरण की बात कही। उन्होंने कहा मूर्च्छा परिग्रह है उसका विवेक करो। आज की समस्या है- पदार्थ और उपभोक्ता के बीच आवश्यकता और उपयोगिता की समझ का अभाव। उपभोक्तावादी संस्कृति महत्वाकांक्षाओं को तेज हवा दे रही है, इसीलिए जिंदगी की भागदौड़ का एक मकसद बन गया है- संग्रह करो, भोग करो। महावीर का दर्शन था खाली रहना। इसीलिए उन्होंने जन-जन के बीच आने से पहले, अपने जीवन के अनुभवों को बांटने से पहले, कठोर तप करने से पहले, स्वयं को अकेला बनाया, खाली बनाया। तप तपा। जीवन का सच जाना। फिर उन्होंने कहा अपने भीतर कुछ भी ऐसा न आने दो जिससे भीतर का संसार प्रदूषित हो। न बुरा देखो, न बुरा न सुना, न बुरा कहो। यही खालीपन का संदेश सुख, शांति, समाधि का मार्ग है। दिन-रात संकल्पों-विकल्पों, सुख-दुख, हर्ष-विषाद से घिरे रहना, कल की चिंता में झुलसना तनाव का भार ढोना, ऐसी स्थिति में भला मन कब कैसे खाली हो सकता है? कैसे संतुलित हो सकता है? कैसे समाधिस्थ हो सकता है? जो आज को जीना सीख लेता है, समझना चाहिए उसने मनुष्य जीवन की सार्थकता को पा लिया है और ऐसे मनुष्यों से बना समाज ही संतुलित हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, समतामूलक हो सकता है।
हर युग की अपनी समस्याएं होती हैं। वर्तमान की भी अपनी समस्याएं हैं। आदमी सदा अपनी समस्या का समाधान खोजता है और खोजता रहा है। तो क्या समस्या भी वर्तमान की और समाधान भी वर्तमान का, यही पर्याप्त है या इसके सिवाय दूसरा भी कोई विकल्प हमारे सामने है? मैंने पढ़ा अमेरिका की एक पत्रिका ‘टाइम्स’ में कि अब सिंगापुर, चीन आदि में कंफ्यूशियस को फिर लाया जा रहा है। यानी कि वर्तमान समस्या का समाधान अतीत में खोजने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमें महावीर को समझना है तो शाश्वत और अशाश्वत दोनों को समझना होगा। अतीत और वर्तमान, दोनों को समझना होगा। महावीर ने सापेक्षता का दर्शन दिया। हर आदमी एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। न केवल आदमी बल्कि प्रत्येक पदार्थ एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारी विचार-तरंगें, हमारी वाणी की तरंगे, संसार की तरंगों से जुड़ी हुई हैं। सारा विश्व एक शंृखला में जुड़ा हुआ है। इसी आधार पर आचार्य उमास्वामी ने लिखा था-‘परस्परोपग्रहो जीवानाम्’, जीव का स्वभाव है एक-दूसरे का आलंबन बनना, सहारा बनना। यह ‘स्ट्रंगल फार सरवाइवल’ या ‘स्ट्रगल फॉर एक्जिसटेंस’ वाली बात अहिंसा के क्षेत्र में मान्य नहीं हो सकती। आज की यह विचारधारा बन गई है कि ‘या मैं या तुम’। दोनों साथ नहीं चल सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसीलिए हुई कि विरोधी विचारधारा वाले राष्ट्र भी एक साथ रह सकें, विकास कर सकें। डॉ. राधाकृष्णन ने भगवान महावीर के बारे में कहा था-आज यह जो पूरा लोकतंत्र जीया जा रहा है, महावीर के आधार पर जीया जा रहा है। वर्तमान की समस्या के समाधान के लिए हमारी दृष्टि वर्तमान पर ही न रहे, वह पीछे की ओर भी जाए। अतीत में भी हमारी समस्या के बहुत से समाधान छिपे हुए हैं। उनका साक्षात्कार करें। इसी से हमारा नया जन्म होगा।

भगवान महावीर हिंदुस्तान के महान सपूत थे। महावीर की अहिंसा में क्रमिक विकास के लिए अवकाश है। मुनि के लिए उन्होंने अहिंसा के महाव्रत का विधान किया। किंतु गृहस्थ के लिए अहिंसा के अणुव्रत का विधान है। लोकतंत्र की आधारभूमि अहिंसा और अनेकांत है। लोकतंत्र के नायकों में सबको विकास का समान अवसर देने व दूसरों के विचारों के प्रति न्याय करने की भावना प्रबल होने पर ही वह सफल होता है, अन्यथा नहीं। महावीर संयम-प्रधान व्यक्ति थे। वैसे तो संयम भारतीय साधना का सामान्य तत्त्व है। महावीर ने उसे अपनी साधना में मुख्य स्थान दिया था। उन्होंने अहिंसा को इसी संदर्भ में स्वीकार किया कि वस्तुतः अपना संयम करना ही अहिंसा है। महावीर का एक महत्वपूर्ण संदेश है ‘क्षमा’। भगवान महावीर ने कहा कि ‘खामेमि सव्वे जीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे, मित्ती में सव्व भूएसू, वेर मज्झं न केणई’। अर्थात् ‘मैं सभी से क्षमा याचना करता हूं। मुझे सभी क्षमा करें। मेरे लिए सभी प्राणी मित्रवत हैं। मेरा किसी से भी वैर नहीं है। यदि भगवान महावीर की इस शिक्षा को हम व्यावहारिक जीवन में उतारें तो फिर क्रोध एवं अहंकार मिश्रित जो दुर्भावना उत्पन्न होती है और जिसके कारण हम घुट-घुट कर जीते हैं, वह समाप्त हो जाएगी।
भगवान महावीर एक कालजयी और असांप्रदायिक महापुरुष थे, जिन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत को तीव्रता से जीया। वे इस महान त्रिपदी के न केवल प्रयोक्ता और प्रणेता बने बल्कि पर्याय बन गए। जहां अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत की चर्चा होती है वहां भगवान महावीर का यशस्वी नाम स्वतः ही सामने आ जाता है। महावीर के दर्शन के प्रकाश में हमें अपने आपको परखना है व अपने कर्तव्य को समझना है। तभी हम उस महापुरुष के श्रीचरणों में सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करने में सफल हो सकेंगे। महावीर के उपदेश जीवनस्पर्शी हैं जिनमें जीवन की समस्याओं का समाधान निहित है। भगवान महावीर चिन्मय दीपक हैं। यदि हमें महावीर बनना है तो पल-पल उनका चिंतन करना अपेक्षित है। यह महावीर जयंती की सार्थकता है और इसी से हम महावीर बनने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।