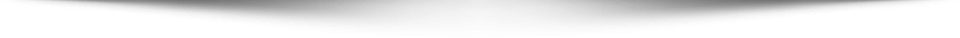स्वच्छता अभियान कहाँ अटक गया ?
*विनीत नारायण
2014 में जब देश में मोदी जी ने सत्ता में आते ही स्वच्छता के प्रति ज़ोर-शोर से एक अभियान छेड़ा था तो सभी
को लगा कि जल्द ही इसका असर ज़मीन पर भी दिखेगा। इस अभियान के विज्ञापन पर बहुत मोटी रक़म खर्च की
गयी। कुछ ही महीनों में मोदी सरकार की प्राथमिकताएं दिखनी भी शुरू हो गईं। जितनी तीव्रता से इस विचार को
सामने लाया गया उससे नई सरकार के योजनाकार भी भौचक्के रह गए। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने सफाई के काम
को छोटा सा काम बताया था। पर अब तक का अनुभव बताता है की सफाई का काम उन बड़े-बड़े कामों से कम
खर्चीला नहीं है जिनके लिए सरकारें हमेशा पैसा कि कमी का रोना रोते रहे हैं। आज आठ साल बाद भी देश की
राजधानी दिल्ली के ही पॉश इलाक़ों तक में पर्याप्त सफ़ाई नहीं दिखती। जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दिखते हैं।
प्रश्न है कि क्या इसके लिए केवल सरकार ज़िम्मेदार है? क्या स्वच्छता के प्रति हम नागरिकों का कोई दायित्व नहीं
है? सोचने वाली बात है कि अगर देश की राजधानी का यह हाल है तो देश के बाक़ी हिस्सों में क्या हाल होगा?
देश के 50 बड़े शहरों में साफ़ सफाई के लिए क्या कुछ करने कोशिश नहीं की गई? रोचक बात ये है कि 600 से
ज्यादा जिला मुख्यालयों में जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन अगर वाकई किसी मुद्दे पर आँखें चुराते हुए
दिखता है तो वह साफ सफाई का मामला ही है। उधर देश के 7 लाख गावों को इस अभियान से जोड़ने के लिए हम
न जाने कितने साल से लगे हैं। यानी कोई कहे कि इतने छोटे से काम पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया तो यह
बात ठीक नहीं होगी। महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इस सार्वभौमिक समस्या के समाधान के लिए व्यवहारिक उपाय
ढूंढने के काम पर लगा जाए तो शायद सही दिशा में अच्छे परिणाम आएँगे। इसके लिए नागरिकों और सरकार की
सहभागिता के बिना कुछ नहीं होगा।
गांधी जयन्ती पर केंद्र या राज्य सरकार के तमाम मंत्री किस तरह खुद झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई करते दिखाई
देते हैं उससे लगता है कि इस समस्या को कर्तव्यबोध बता कर निपटाने की बात सोची गई थी। यानी हम मान रहे
हैं कि नागरिक जब तक अपने आसपास का खुद ख़याल नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस खुद ख्याल रखने
की बात पर भी गौर करना ज़रूरी है।
शोधपरख तथ्य तो उपलब्ध नहीं है लेकिन सार्वभौमिक अनुभव है कि देश के मोहल्लों या गलियों में इस बात पर
झगड़े होते हैं कि ‘मेरे घर के पास कूडा क्यों फेंका’? यानी समस्या यह है कि घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके कहाँ
‘फेंका’ जाए?
निर्मला कल्याण समिति जैसी कुछ स्वयमसेवी संस्थाओं के पर्यीवेक्षण है कि उपनगरीय इलाकों में घर का कूड़ा
फेकने के लिए लोगों को आधा किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। ज़ाहिर है कि देश के 300 कस्बों में लोगों की
तलाश बसावट के बाहर कूड़ा फेंकने की है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अनुभव यह है कि हमारे
बेशकीमती जल संसाधन मसलन तालाब, कुण्ड और कुँए – कूड़ा कचरा फेंकने के खड्ड बन गए हैं। इन नए घूरों और
खड्डों की भी अपनी सीमा थी। पर अब हर जगह ये घूरे और कूड़े से पट गए हैं। आने वाले समय में नई चुनौती यह
खड़ी होने वाली है कि शहरों और कस्बों से निकले कूड़े-कचरे के पहाड़ हम कहाँ-कहाँ बनाए? उसके लिए ज़मीने
कहाँ ढूंढें? दिल्ली जैसे महानगर में भी कूड़ा इकट्ठा करने के स्थान भर चुके हैं और यहाँ भी कूड़ा इकट्ठा करने के लिए
नए स्थान खोजे जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पूर्वी दिल्ली में बने कूड़े के पहाड़ों को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई
कर रहा है।
गाँव भले ही अपनी कमज़ोर माली हालत के कारण कूड़े कचरे की मात्रा से परेशान न हों लेकिन जनसँख्या के बढते
दबाव के चलते वहां बसावट का घनत्व बढ़ गया है। गावों में तरल कचरा पहले कच्ची नालियों के ज़रिये भूमिगत
जल में मिल जाता था। अब यह समस्या है कि गावों से निकली नालियों का पानी कहाँ जाए। इसके लिए भी गावों
की सबसे बड़ी धरोहर पुराने तालाब या कुण्ड गन्दी नालियों के कचरे से पट चले हैं।
यह कहने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि बड़े शहरों और कस्बों के गंदे नाले यमुना जैसी देश की प्रमुख नदियों में
गिराए जा रहे हैं। चाहे विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हों और चाहे पर्यावरण पर काम करने वाली स्वयंसेवी
संस्थाएँ – और चाहे कितनी भी चिंतित सरकारें – ये सब गंभीर मुद्रा में ‘चिंता’ करते हुए दिखते तो हैं लेकिन
सफाई जैसी ‘बहुत छोटी’ या बहुत बड़ी समस्या पर गम्भीर कोई नहीं दिखता। अगर ऐसा होता तो ठोस कचरा
प्रबंधन, औद्योगिक कचरे के प्रबंधन, नदियों व सरोवरों या कुंडों के प्रदूषण स्वच्छता और स्वास्थ्य के सम्बन्ध जैसे
विषयों पर भी हमें बड़े अकादमिक आयोजन होते ज़रूर दिखाई देते।
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और राष्ट्रीय दिवसों पर सरकारी पैसे से कुछ सेमीनार और शोध सम्मेलन होते ज़रूर हैं।
लेकिन उनमें समस्याओं के विभिन्न पक्षों की गिनती से ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। ऐसे आयोजनों में आमंत्रित करने
के लिए विशेषज्ञों का चयन करते समय लालच यह रहता है कि सम्बंधित विशेषज्ञ संसाधनों का प्रबंध करने में भी
थोड़ा बहुत सक्षम हो। और होता यह है कि ऐसे समर्थ विशेषज्ञ पहले से चलती हुई यानी चालु योजना या
परियोजना के आगे सोच ही नहीं पाते। जबकि जटिल समस्याओं के लिए हमें नवोन्मेषी मिज़ाज के लोगों की
ज़रूरत पड़ती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों, प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थानों और चिंताशील स्वयंसेवी संस्थाओं
के समन्वित प्रयासों से, अपने-अपने प्रभुत्व के आग्रह को छोड़ कर, एक दूसरे से मदद लेकर ही स्वच्छता जैसी बड़ी
समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। पर हर समस्या को समस्या बनाकर रखने की अभ्यस्त नौकरशाही इस
समस्या को भी अपनी लालफ़ीताशाही की फ़ाइलों में क़ैद रखने में ही अपनी कामयाबी समझती है। इसलिये कोई
हल नहीं निकल पाता।
हिमाचल प्रदेश की मनोरम घाटी हों या सागर के रमणीक तट, तेज़ रफ़्तार से दौड़ती रेलगाड़ियों की खिड़की के
दोनों ओर की रेल विभाग की ज़मीने, हर ओर कूड़े का विशाल साम्राज्य देख कर कलेजा मुँह को आता है। पश्चिमी
देशों की नज़र में भारत सबसे गंदे देशों में से एक है। ये हम सबके लिये शर्म की बात है। हम सबको सोचना और
कुछ ठोस करना चाहिये।